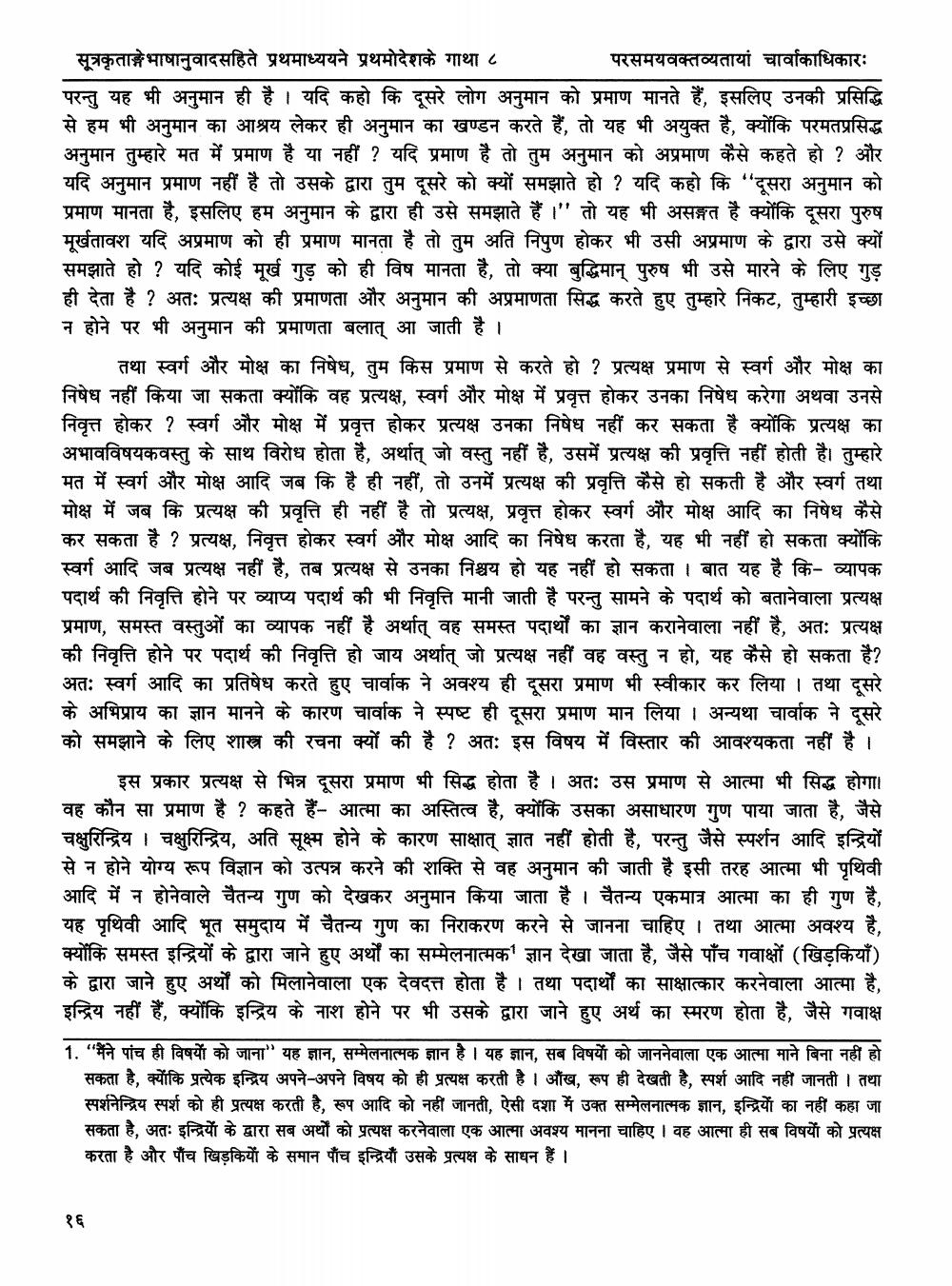________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते प्रथमाध्ययने प्रथमोदेशके गाथा ८
परसमयवक्तव्यतायां चार्वाकाधिकारः परन्तु यह भी अनुमान ही है। यदि कहो कि दूसरे लोग अनुमान को प्रमाण मानते हैं, इसलिए उनकी प्रसिद्धि से हम भी अनुमान का आश्रय लेकर ही अनुमान का खण्डन करते हैं, तो यह भी अयुक्त है, क्योंकि परमतप्रसिद्ध अनुमान तुम्हारे मत में प्रमाण है या नहीं ? यदि प्रमाण है तो तुम अनुमान को अप्रमाण कैसे कहते हो ? और यदि अनुमान प्रमाण नहीं है तो उसके द्वारा तुम दूसरे को क्यों समझाते हो ? यदि कहो कि "दूसरा अनुमान को प्रमाण मानता है, इसलिए हम अनुमान के द्वारा ही उसे समझाते हैं।" तो यह भी असङ्गत है क्योंकि दूसरा पुरुष मर्खतावश यदि अप्रमाण को ही प्रमाण मानता है तो तम अति निपण होकर भी उसी अप्रमाण के द्वारा उसे क्यों समझाते हो ? यदि कोई मूर्ख गुड़ को ही विष मानता है, तो क्या बुद्धिमान् पुरुष भी उसे मारने के लिए गुड़ ही देता है ? अतः प्रत्यक्ष की प्रमाणता और अनुमान की अप्रमाणता सिद्ध करते हुए तुम्हारे निकट, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी अनुमान की प्रमाणता बलात् आ जाती है ।
तथा स्वर्ग और मोक्ष का निषेध, तुम किस प्रमाण से करते हो ? प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वर्ग और मोक्ष का निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह प्रत्यक्ष, स्वर्ग और मोक्ष में प्रवृत्त होकर उनका निषेध करेगा अथवा उनसे निवृत्त होकर ? स्वर्ग और मोक्ष में प्रवृत्त होकर प्रत्यक्ष उनका निषेध नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष का अभावविषयकवस्तु के साथ विरोध होता है, अर्थात् जो वस्तु नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। तुम्हारे मत में स्वर्ग और मोक्ष आदि जब कि है ही नहीं, तो उनमें प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है और स्वर्ग तथा मोक्ष में जब कि प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं है तो प्रत्यक्ष, प्रवृत्त होकर स्वर्ग और मोक्ष आदि का निषेध कैसे कर सकता है ? प्रत्यक्ष, निवृत्त होकर स्वर्ग और मोक्ष आदि का निषेध करता है, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि स्वर्ग आदि जब प्रत्यक्ष नहीं है, तब प्रत्यक्ष से उनका निश्चय हो यह नहीं हो सकता । बात यह है कि- व्यापक पदार्थ की निवृत्ति होने पर व्याप्य पदार्थ की भी निवृत्ति मानी जाती है परन्तु सामने के पदार्थ को बतानेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण, समस्त वस्तुओं का व्यापक नहीं है अर्थात् वह समस्त पदार्थों का ज्ञान करानेवाला नहीं है, अतः प्रत्यक्ष की निवृत्ति होने पर पदार्थ की निवृत्ति हो जाय अर्थात् जो प्रत्यक्ष नहीं वह वस्तु न हो, यह कैसे हो सकता है? अतः स्वर्ग आदि का प्रतिषेध करते हुए चार्वाक ने अवश्य ही दूसरा प्रमाण भी स्वीकार कर लिया । तथा दूसरे के अभिप्राय का ज्ञान मानने के कारण चार्वाक ने स्पष्ट ही दूसरा प्रमाण मान लिया । अन्यथा चार्वाक ने दूसरे को समझाने के लिए शास्त्र की रचना क्यों की है ? अतः इस विषय में विस्तार की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार प्रत्यक्ष से भिन्न दूसरा प्रमाण भी सिद्ध होता है । अतः उस प्रमाण से आत्मा भी सिद्ध होगा। वह कौन सा प्रमाण है ? कहते हैं- आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि उसका असाधारण गुण पाया जाता है, जैसे चक्षुरिन्द्रिय । चक्षुरिन्द्रिय, अति सूक्ष्म होने के कारण साक्षात् ज्ञात नहीं होती है, परन्तु जैसे स्पर्शन आदि इन्द्रियों से न होने योग्य रूप विज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति से वह अनुमान की जाती है इसी तरह आत्मा भी पृथिवी आदि में न होनेवाले चैतन्य गुण को देखकर अनुमान किया जाता है । चैतन्य एकमात्र आत्मा का ही गुण है, यह पृथिवी आदि भूत समुदाय में चैतन्य गुण का निराकरण करने से जानना चाहिए । तथा आत्मा अवश्य है, क्योंकि समस्त इन्द्रियों के द्वारा जाने हुए अर्थों का सम्मेलनात्मक ज्ञान देखा जाता है, जैसे पाँच गवाक्षों (खिड़कियाँ) के द्वारा जाने हुए अर्थों को मिलानेवाला एक देवदत्त होता है । तथा पदार्थों का साक्षात्कार करनेवाला आत्मा है, इन्द्रिय नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रिय के नाश होने पर भी उसके द्वारा जाने हए अर्थ का स्मरण होता है, जैसे गवाक्ष
1. "मैंने पांच ही विषयों को जाना" यह ज्ञान, सम्मेलनात्मक ज्ञान है । यह ज्ञान, सब विषयों को जाननेवाला एक आत्मा माने बिना नहीं हो
सकता है, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को ही प्रत्यक्ष करती है । आँख, रूप ही देखती है, स्पर्श आदि नहीं जानती । तथा स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श को ही प्रत्यक्ष करती है, रूप आदि को नहीं जानती, ऐसी दशा में उक्त सम्मेलनात्मक ज्ञान, इन्द्रियों का नहीं कहा जा सकता है, अतः इन्द्रियों के द्वारा सब अर्थों को प्रत्यक्ष करनेवाला एक आत्मा अवश्य मानना चाहिए । वह आत्मा ही सब विषयों को प्रत्यक्ष करता है और पाँच खिड़कियों के समान पाँच इन्द्रियाँ उसके प्रत्यक्ष के साधन हैं।