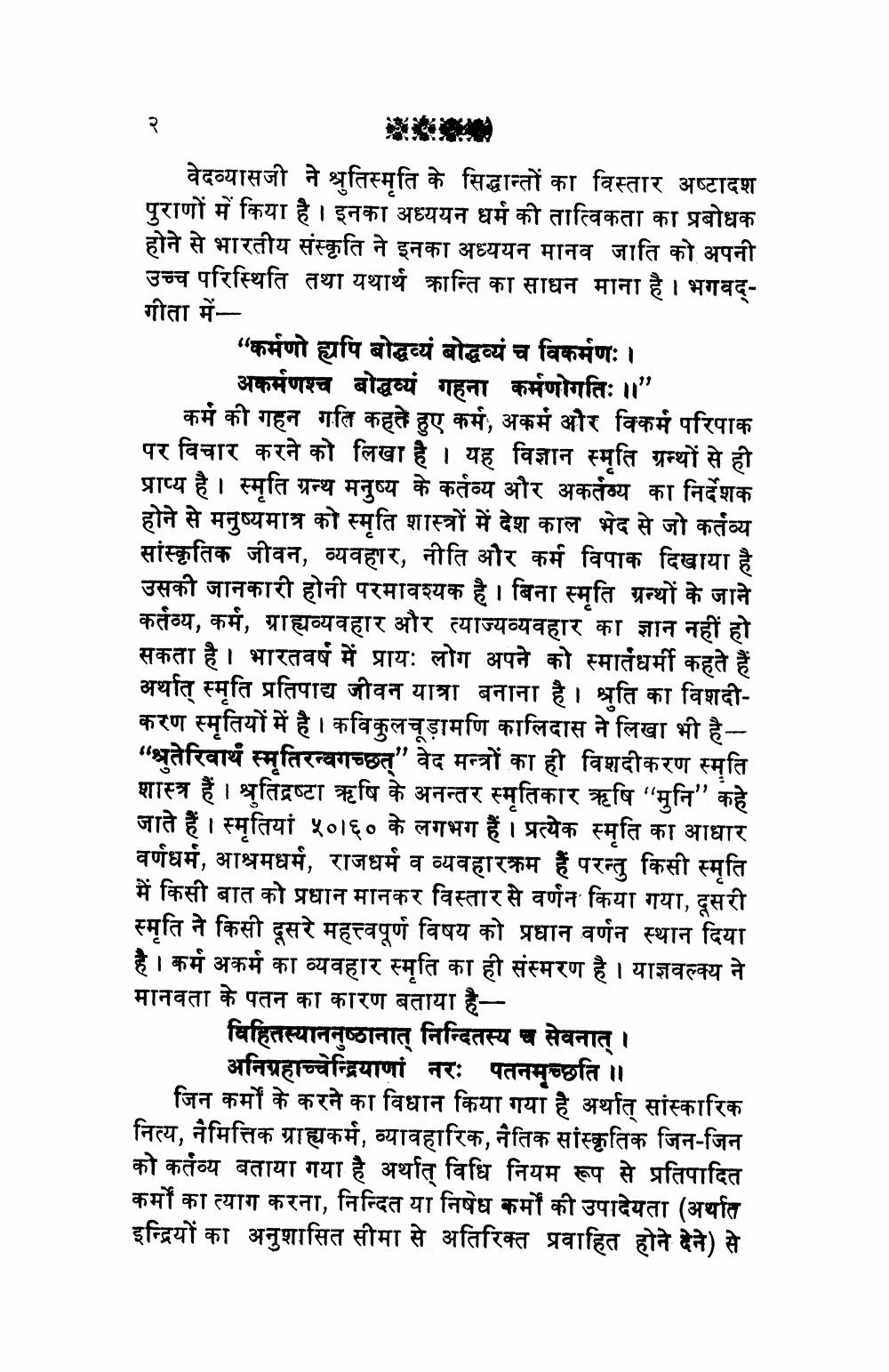________________
वेदव्यासजी ने श्रुतिस्मति के सिद्धान्तों का विस्तार अष्टादश पुराणों में किया है। इनका अध्ययन धर्म की तात्विकता का प्रबोधक होने से भारतीय संस्कृति ने इनका अध्ययन मानव जाति को अपनी उच्च परिस्थिति तथा यथार्थ क्रान्ति का साधन माना है । भगवद्गीता में
"कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । __ अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणोगतिः॥" कर्म की गहन गति कहते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म परिपाक पर विचार करने को लिखा है । यह विज्ञान स्मृति ग्रन्थों से ही प्राप्य है। स्मृति ग्रन्थ मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्देशक होने से मनुष्यमात्र को स्मृति शास्त्रों में देश काल भेद से जो कर्तव्य सांस्कृतिक जीवन, व्यवहार, नीति और कर्म विपाक दिखाया है उसकी जानकारी होनी परमावश्यक है। बिना स्मति ग्रन्थों के जाने कर्तव्य, कर्म, ग्राह्यव्यवहार और त्याज्यव्यवहार का ज्ञान नहीं हो सकता है। भारतवर्ष में प्रायः लोग अपने को स्मार्तधर्मी कहते हैं अर्थात् स्मृति प्रतिपाद्य जीवन यात्रा बनाना है। श्रुति का विशदीकरण स्मृतियों में है । कविकुलचूड़ामणि कालिदास ने लिखा भी है"श्रुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्" वेद मन्त्रों का ही विशदीकरण स्मति शास्त्र हैं। श्रतिद्रष्टा ऋषि के अनन्तर स्मतिकार ऋषि "मूनि" कहे जाते हैं। स्मृतियां ५०।६० के लगभग हैं। प्रत्येक स्मृति का आधार वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म व व्यवहारक्रम हैं परन्तु किसी स्मृति में किसी बात को प्रधान मानकर विस्तार से वर्णन किया गया, दूसरी स्मृति ने किसी दूसरे महत्त्वपूर्ण विषय को प्रधान वर्णन स्थान दिया है। कर्म अकर्म का व्यवहार स्मृति का ही संस्मरण है। याज्ञवल्क्य ने मानवता के पतन का कारण बताया है
विहितस्याननुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात् ।
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमच्छति ॥ जिन कर्मों के करने का विधान किया गया है अर्थात् सांस्कारिक नित्य, नैमित्तिक ग्राह्यकर्म, व्यावहारिक, नैतिक सांस्कृतिक जिन-जिन को कर्तव्य बताया गया है अर्थात् विधि नियम रूप से प्रतिपादित कर्मों का त्याग करना, निन्दित या निषेध कर्मों की उपादेयता (अर्थात इन्द्रियों का अनुशासित सीमा से अतिरिक्त प्रवाहित होने देने) से