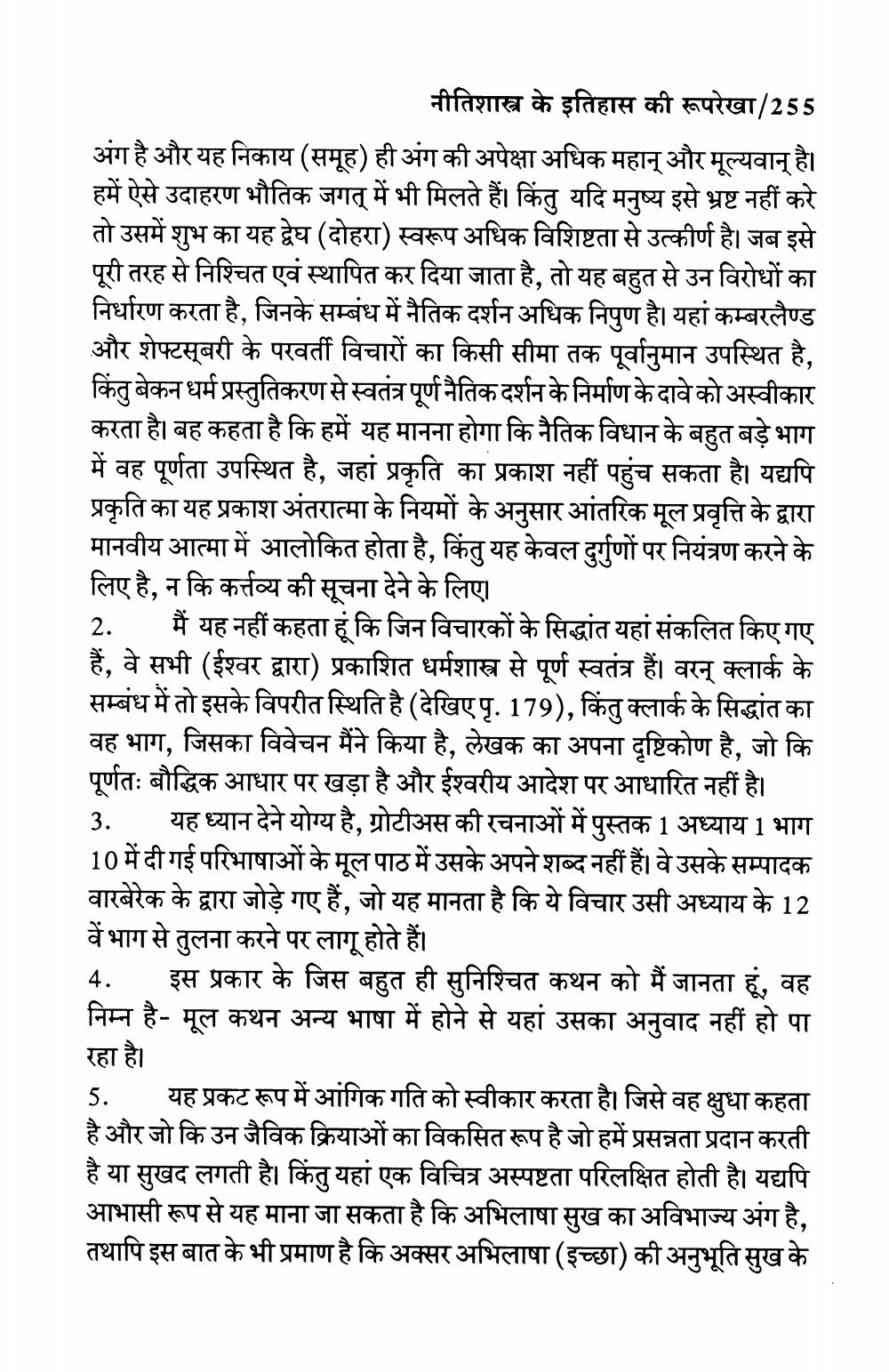________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/255 अंग है और यह निकाय (समूह) ही अंग की अपेक्षा अधिक महान् और मूल्यवान् है। हमें ऐसे उदाहरण भौतिक जगत् में भी मिलते हैं। किंतु यदि मनुष्य इसे भ्रष्ट नहीं करे तो उसमें शुभ का यह द्वेष (दोहरा) स्वरूप अधिक विशिष्टता से उत्कीर्ण है। जब इसे पूरी तरह से निश्चित एवं स्थापित कर दिया जाता है, तो यह बहुत से उन विरोधों का निर्धारण करता है, जिनके सम्बंध में नैतिक दर्शन अधिक निपुण है। यहां कम्बरलैण्ड
और शेफ्टस्बरी के परवर्ती विचारों का किसी सीमा तक पूर्वानुमान उपस्थित है, किंतु बेकन धर्म प्रस्तुतिकरण से स्वतंत्र पूर्णनैतिक दर्शन के निर्माण के दावे को अस्वीकार करता है। वह कहता है कि हमें यह मानना होगा कि नैतिक विधान के बहुत बड़े भाग में वह पूर्णता उपस्थित है, जहां प्रकृति का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है। यद्यपि प्रकृति का यह प्रकाश अंतरात्मा के नियमों के अनुसार आंतरिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा मानवीय आत्मा में आलोकित होता है, किंतु यह केवल दुर्गुणों पर नियंत्रण करने के लिए है, न कि कर्त्तव्य की सूचना देने के लिए। 2. मैं यह नहीं कहता हूं कि जिन विचारकों के सिद्धांत यहां संकलित किए गए हैं, वे सभी (ईश्वर द्वारा) प्रकाशित धर्मशास्त्र से पूर्ण स्वतंत्र हैं। वरन् क्लार्क के सम्बंध में तो इसके विपरीत स्थिति है (देखिए पृ. 179), किंतु क्लार्क के सिद्धांत का वह भाग, जिसका विवेचन मैंने किया है, लेखक का अपना दृष्टिकोण है, जो कि पूर्णतः बौद्धिक आधार पर खड़ा है और ईश्वरीय आदेश पर आधारित नहीं है। 3. यह ध्यान देने योग्य है, ग्रोटीअस की रचनाओं में पुस्तक 1 अध्याय 1 भाग 10 में दी गई परिभाषाओं के मूल पाठ में उसके अपने शब्द नहीं हैं। वे उसके सम्पादक वारबेरेक के द्वारा जोड़े गए हैं, जो यह मानता है कि ये विचार उसी अध्याय के 12 वेंभाग से तुलना करने पर लागू होते हैं। 4. इस प्रकार के जिस बहुत ही सुनिश्चित कथन को मैं जानता हूं, वह निम्न है- मूल कथन अन्य भाषा में होने से यहां उसका अनुवाद नहीं हो पा रहा है। 5. यह प्रकट रूप में आंगिक गति को स्वीकार करता है। जिसे वह क्षुधा कहता है और जो कि उन जैविक क्रियाओं का विकसित रूप है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती है या सुखद लगती है। किंतु यहां एक विचित्र अस्पष्टता परिलक्षित होती है। यद्यपि आभासी रूप से यह माना जा सकता है कि अभिलाषा सुख का अविभाज्य अंग है, तथापि इस बात के भी प्रमाण है कि अक्सर अभिलाषा (इच्छा) की अनुभूति सुख के