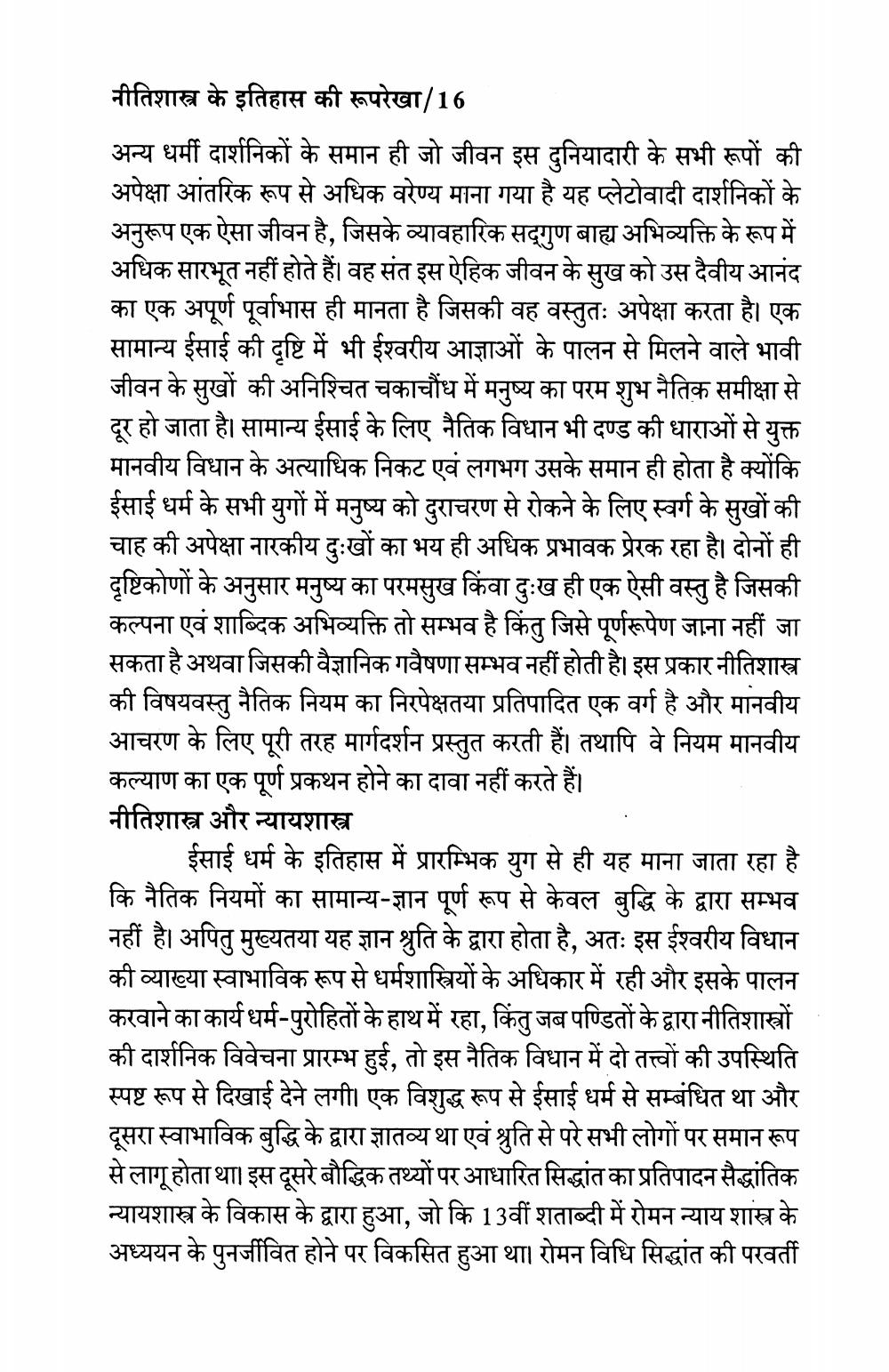________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/16 अन्य धर्मी दार्शनिकों के समान ही जो जीवन इस दुनियादारी के सभी रूपों की अपेक्षा आंतरिक रूप से अधिक वरेण्य माना गया है यह प्लेटोवादी दार्शनिकों के अनुरूप एक ऐसा जीवन है, जिसके व्यावहारिक सद्गुण बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में अधिक सारभूत नहीं होते हैं। वह संत इस ऐहिक जीवन के सुख को उस दैवीय आनंद का एक अपूर्ण पूर्वाभास ही मानता है जिसकी वह वस्तुतः अपेक्षा करता है। एक सामान्य ईसाई की दृष्टि में भी ईश्वरीय आज्ञाओं के पालन से मिलने वाले भावी जीवन के सुखों की अनिश्चित चकाचौंध में मनुष्य का परम शुभ नैतिक समीक्षा से दूर हो जाता है। सामान्य ईसाई के लिए नैतिक विधान भी दण्ड की धाराओं से युक्त मानवीय विधान के अत्याधिक निकट एवं लगभग उसके समान ही होता है क्योंकि ईसाई धर्म के सभी युगों में मनुष्य को दुराचरण से रोकने के लिए स्वर्ग के सुखों की चाह की अपेक्षा नारकीय दुःखों का भय ही अधिक प्रभावक प्रेरक रहा है। दोनों ही दृष्टिकोणों के अनुसार मनुष्य का परमसुख किंवा दुःख ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी कल्पना एवं शाब्दिक अभिव्यक्ति तो सम्भव है किंतु जिसे पूर्णरूपेण जाना नहीं जा सकता है अथवा जिसकी वैज्ञानिक गवैषणा सम्भव नहीं होती है। इस प्रकार नीतिशास्त्र की विषयवस्तु नैतिक नियम का निरपेक्षतया प्रतिपादित एक वर्ग है और मानवीय आचरण के लिए पूरी तरह मार्गदर्शन प्रस्तुत करती हैं। तथापि वे नियम मानवीय कल्याण का एक पूर्ण प्रकथन होने का दावा नहीं करते हैं। नीतिशास्त्र और न्यायशास्त्र
ईसाई धर्म के इतिहास में प्रारम्भिक युग से ही यह माना जाता रहा है कि नैतिक नियमों का सामान्य-ज्ञान पूर्ण रूप से केवल बुद्धि के द्वारा सम्भव नहीं है। अपितु मुख्यतया यह ज्ञान श्रुति के द्वारा होता है, अतः इस ईश्वरीय विधान की व्याख्या स्वाभाविक रूप से धर्मशास्त्रियों के अधिकार में रही और इसके पालन करवाने का कार्य धर्म-पुरोहितों के हाथ में रहा, किंतु जब पण्डितों के द्वारा नीतिशास्त्रों की दार्शनिक विवेचना प्रारम्भ हुई, तो इस नैतिक विधान में दो तत्त्वों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। एक विशुद्ध रूप से ईसाई धर्म से सम्बंधित था और दूसरा स्वाभाविक बुद्धि के द्वारा ज्ञातव्य था एवं श्रुति से परे सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता था। इस दूसरे बौद्धिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन सैद्धांतिक न्यायशास्त्र के विकास के द्वारा हुआ, जो कि 13वीं शताब्दी में रोमन न्याय शास्त्र के अध्ययन के पुनर्जीवित होने पर विकसित हुआ था। रोमन विधि सिद्धांत की परवर्ती