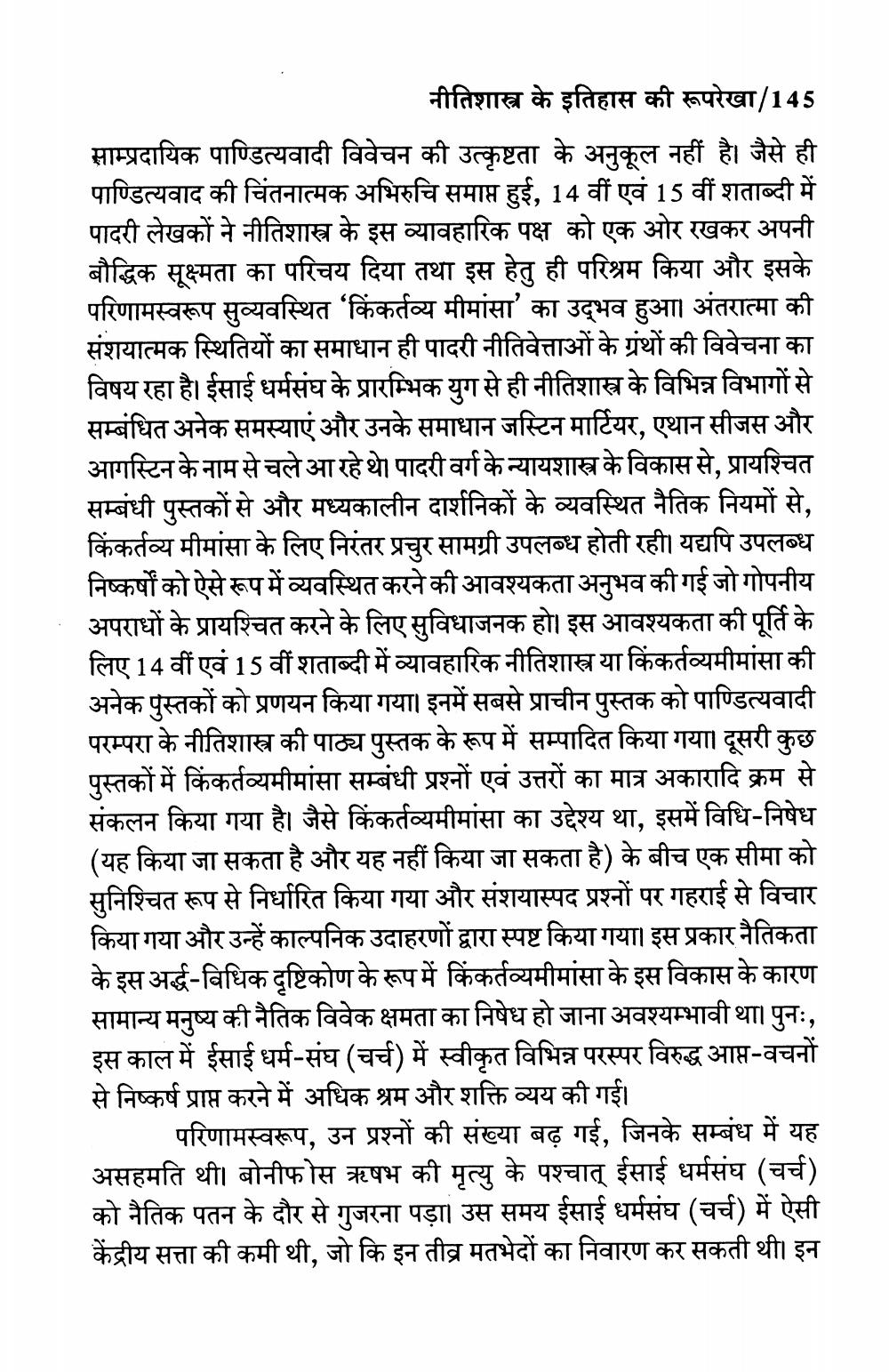________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/145 साम्प्रदायिक पाण्डित्यवादी विवेचन की उत्कृष्टता के अनुकूल नहीं है। जैसे ही पाण्डित्यवाद की चिंतनात्मक अभिरुचि समाप्त हुई, 14 वीं एवं 15 वीं शताब्दी में पादरी लेखकों ने नीतिशास्त्र के इस व्यावहारिक पक्ष को एक ओर रखकर अपनी बौद्धिक सूक्ष्मता का परिचय दिया तथा इस हेतु ही परिश्रम किया और इसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित 'किंकर्तव्य मीमांसा' का उद्भव हुआ। अंतरात्मा की संशयात्मक स्थितियों का समाधान ही पादरी नीतिवेत्ताओं के ग्रंथों की विवेचना का विषय रहा है। ईसाई धर्मसंघ के प्रारम्भिक युग से ही नीतिशास्त्र के विभिन्न विभागों से सम्बंधित अनेक समस्याएं और उनके समाधान जस्टिन मार्टियर, एथान सीजस और आगस्टिन के नाम से चले आ रहे थे। पादरी वर्ग के न्यायशास्त्र के विकास से, प्रायश्चित सम्बंधी पुस्तकों से और मध्यकालीन दार्शनिकों के व्यवस्थित नैतिक नियमों से, किंकर्तव्य मीमांसा के लिए निरंतर प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती रही। यद्यपि उपलब्ध निष्कर्षों को ऐसे रूप में व्यवस्थित करने की आवश्यकता अनुभव की गई जो गोपनीय अपराधों के प्रायश्चित करने के लिए सुविधाजनक हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 14 वीं एवं 15 वीं शताब्दी में व्यावहारिक नीतिशास्त्र या किंकर्तव्यमीमांसा की अनेक पुस्तकों को प्रणयन किया गया। इनमें सबसे प्राचीन पुस्तक को पाण्डित्यवादी परम्परा के नीतिशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के रूप में सम्पादित किया गया। दूसरी कुछ पुस्तकों में किंकर्तव्यमीमांसा सम्बंधी प्रश्नों एवं उत्तरों का मात्र अकारादि क्रम से संकलन किया गया है। जैसे किंकर्तव्यमीमांसा का उद्देश्य था, इसमें विधि-निषेध (यह किया जा सकता है और यह नहीं किया जा सकता है) के बीच एक सीमा को सुनिश्चित रूप से निर्धारित किया गया और संशयास्पद प्रश्नों पर गहराई से विचार किया गया और उन्हें काल्पनिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया। इस प्रकार नैतिकता के इस अर्द्ध-विधिक दृष्टिकोण के रूप में किंकर्तव्यमीमांसा के इस विकास के कारण सामान्य मनुष्य की नैतिक विवेक क्षमता का निषेध हो जाना अवश्यम्भावी था। पुनः, इस काल में ईसाई धर्म-संघ (चर्च) में स्वीकृत विभिन्न परस्पर विरुद्ध आप्त-वचनों से निष्कर्ष प्राप्त करने में अधिक श्रम और शक्ति व्यय की गई।
परिणामस्वरूप, उन प्रश्नों की संख्या बढ़ गई, जिनके सम्बंध में यह असहमति थी। बोनीफोस ऋषभ की मृत्यु के पश्चात् ईसाई धर्मसंघ (चर्च) को नैतिक पतन के दौर से गुजरना पड़ा। उस समय ईसाई धर्मसंघ (चर्च) में ऐसी केंद्रीय सत्ता की कमी थी, जो कि इन तीव्र मतभेदों का निवारण कर सकती थी। इन