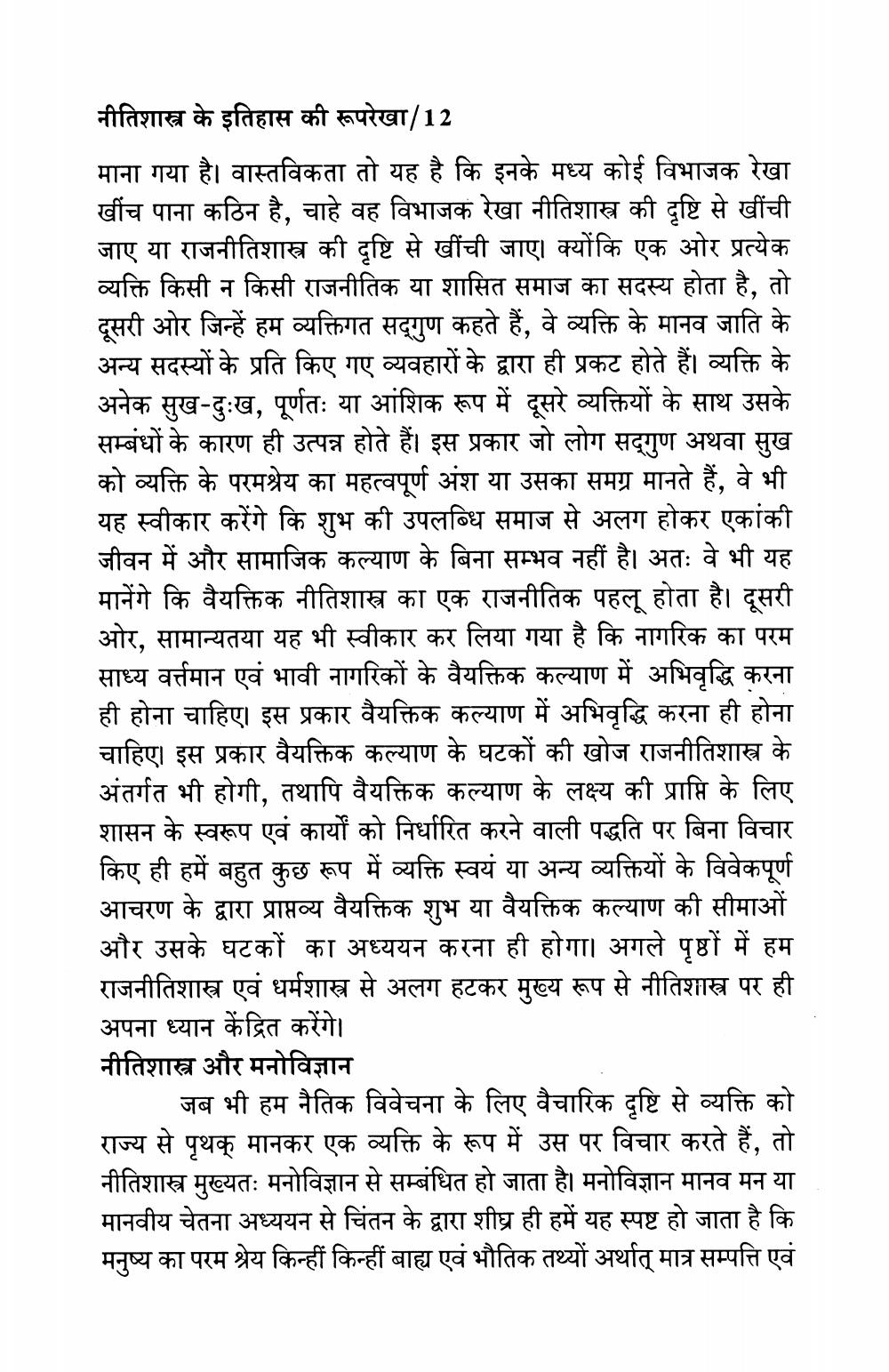________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/12 माना गया है। वास्तविकता तो यह है कि इनके मध्य कोई विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है, चाहे वह विभाजक रेखा नीतिशास्त्र की दृष्टि से खींची जाए या राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से खींची जाए। क्योंकि एक ओर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक या शासित समाज का सदस्य होता है, तो दूसरी ओर जिन्हें हम व्यक्तिगत सद्गुण कहते हैं, वे व्यक्ति के मानव जाति के अन्य सदस्यों के प्रति किए गए व्यवहारों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। व्यक्ति के अनेक सुख-दुःख, पूर्णतः या आंशिक रूप में दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके सम्बंधों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो लोग सद्गुण अथवा सुख को व्यक्ति के परमश्रेय का महत्वपूर्ण अंश या उसका समग्र मानते हैं, वे भी यह स्वीकार करेंगे कि शुभ की उपलब्धि समाज से अलग होकर एकांकी जीवन में और सामाजिक कल्याण के बिना सम्भव नहीं है। अतः वे भी यह मानेंगे कि वैयक्तिक नीतिशास्त्र का एक राजनीतिक पहलू होता है। दूसरी
ओर, सामान्यतया यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि नागरिक का परम साध्य वर्तमान एवं भावी नागरिकों के वैयक्तिक कल्याण में अभिवृद्धि करना ही होना चाहिए। इस प्रकार वैयक्तिक कल्याण में अभिवद्धि करना ही होना चाहिए। इस प्रकार वैयक्तिक कल्याण के घटकों की खोज राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत भी होगी, तथापि वैयक्तिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन के स्वरूप एवं कार्यों को निर्धारित करने वाली पद्धति पर बिना विचार किए ही हमें बहुत कुछ रूप में व्यक्ति स्वयं या अन्य व्यक्तियों के विवेकपूर्ण आचरण के द्वारा प्राप्तव्य वैयक्तिक शुभ या वैयक्तिक कल्याण की सीमाओं और उसके घटकों का अध्ययन करना ही होगा। अगले पृष्ठों में हम राजनीतिशास्त्र एवं धर्मशास्त्र से अलग हटकर मुख्य रूप से नीतिशास्त्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान
___ जब भी हम नैतिक विवेचना के लिए वैचारिक दृष्टि से व्यक्ति को राज्य से पृथक् मानकर एक व्यक्ति के रूप में उस पर विचार करते हैं, तो नीतिशास्त्र मुख्यतः मनोविज्ञान से सम्बंधित हो जाता है। मनोविज्ञान मानव मन या मानवीय चेतना अध्ययन से चिंतन के द्वारा शीघ्र ही हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का परम श्रेय किन्हीं किन्हीं बाह्य एवं भौतिक तथ्यों अर्थात् मात्र सम्पत्ति एवं