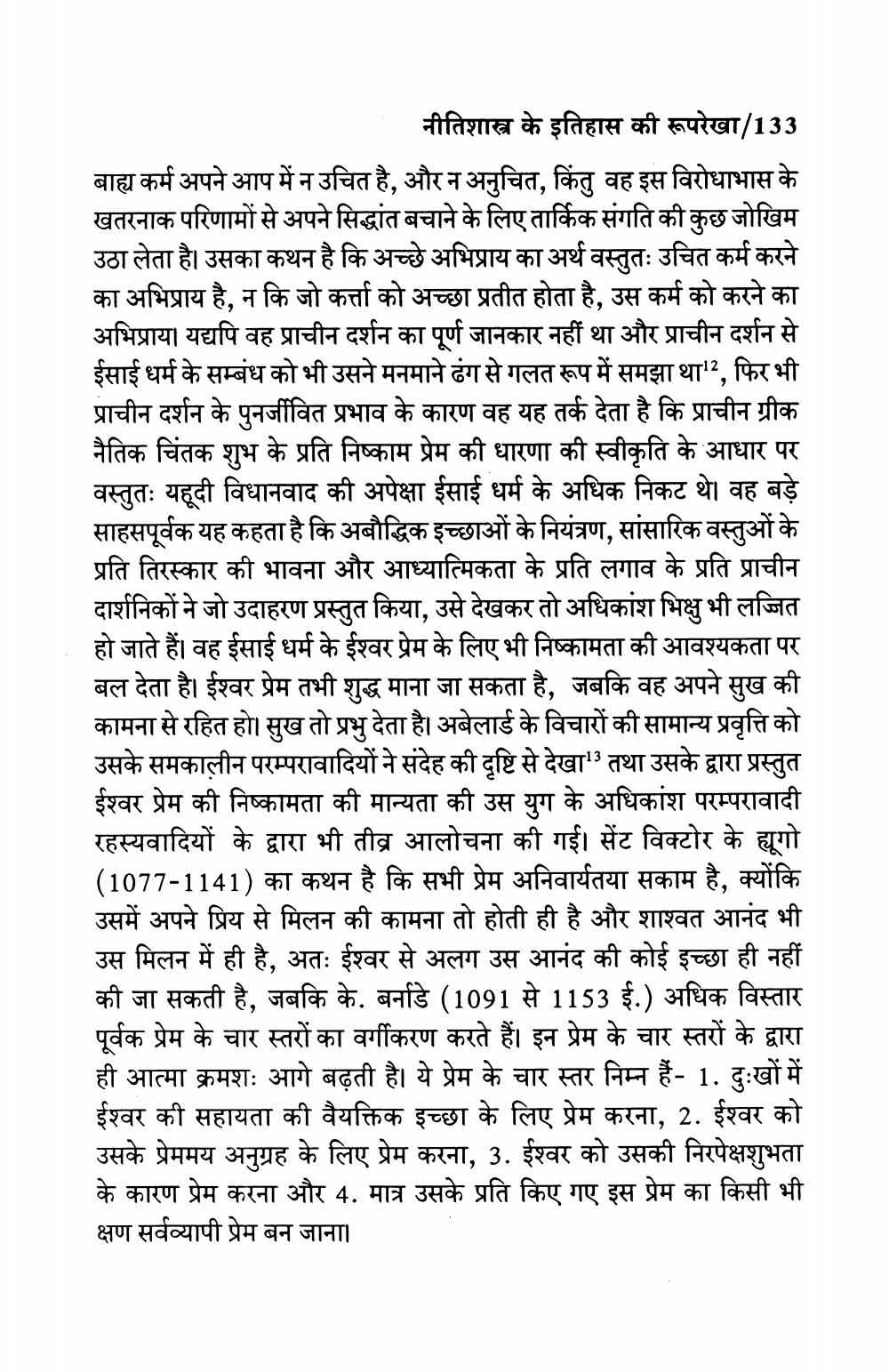________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/133 बाह्य कर्म अपने आप में न उचित है, और न अनुचित, किंतु वह इस विरोधाभास के खतरनाक परिणामों से अपने सिद्धांत बचाने के लिए तार्किक संगति की कुछ जोखिम उठा लेता है। उसका कथन है कि अच्छे अभिप्राय का अर्थ वस्तुतः उचित कर्म करने का अभिप्राय है, न कि जो कर्ता को अच्छा प्रतीत होता है, उस कर्म को करने का अभिप्राय। यद्यपि वह प्राचीन दर्शन का पूर्ण जानकार नहीं था और प्राचीन दर्शन से ईसाई धर्म के सम्बंध को भी उसने मनमाने ढंग से गलत रूप में समझा था', फिर भी प्राचीन दर्शन के पुनर्जीवित प्रभाव के कारण वह यह तर्क देता है कि प्राचीन ग्रीक नैतिक चिंतक शुभ के प्रति निष्काम प्रेम की धारणा की स्वीकृति के आधार पर वस्तुतः यहूदी विधानवाद की अपेक्षा ईसाई धर्म के अधिक निकट थे। वह बड़े साहसपूर्वक यह कहता है कि अबौद्धिक इच्छाओं के नियंत्रण, सांसारिक वस्तुओं के प्रति तिरस्कार की भावना और आध्यात्मिकता के प्रति लगाव के प्रति प्राचीन दार्शनिकों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसे देखकर तो अधिकांश भिक्षु भी लज्जित हो जाते हैं। वह ईसाई धर्म के ईश्वर प्रेम के लिए भी निष्कामता की आवश्यकता पर बल देता है। ईश्वर प्रेम तभी शुद्ध माना जा सकता है, जबकि वह अपने सुख की कामना से रहित हो। सुख तो प्रभु देता है। अबेलार्ड के विचारों की सामान्य प्रवृत्ति को उसके समकालीन परम्परावादियों ने संदेह की दृष्टि से देखा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत ईश्वर प्रेम की निष्कामता की मान्यता की उस युग के अधिकांश परम्परावादी रहस्यवादियों के द्वारा भी तीव्र आलोचना की गई। सेंट विक्टोर के ह्यूगो (1077-1141) का कथन है कि सभी प्रेम अनिवार्यतया सकाम है, क्योंकि उसमें अपने प्रिय से मिलन की कामना तो होती ही है और शाश्वत आनंद भी उस मिलन में ही है, अतः ईश्वर से अलग उस आनंद की कोई इच्छा ही नहीं की जा सकती है, जबकि के. बर्नाडे (1091 से 1153 ई.) अधिक विस्तार पूर्वक प्रेम के चार स्तरों का वर्गीकरण करते हैं। इन प्रेम के चार स्तरों के द्वारा ही आत्मा क्रमशः आगे बढ़ती है। ये प्रेम के चार स्तर निम्न हैं- 1. दुःखों में ईश्वर की सहायता की वैयक्तिक इच्छा के लिए प्रेम करना, 2. ईश्वर को उसके प्रेममय अनुग्रह के लिए प्रेम करना, 3. ईश्वर को उसकी निरपेक्षशुभता के कारण प्रेम करना और 4. मात्र उसके प्रति किए गए इस प्रेम का किसी भी क्षण सर्वव्यापी प्रेम बन जाना।