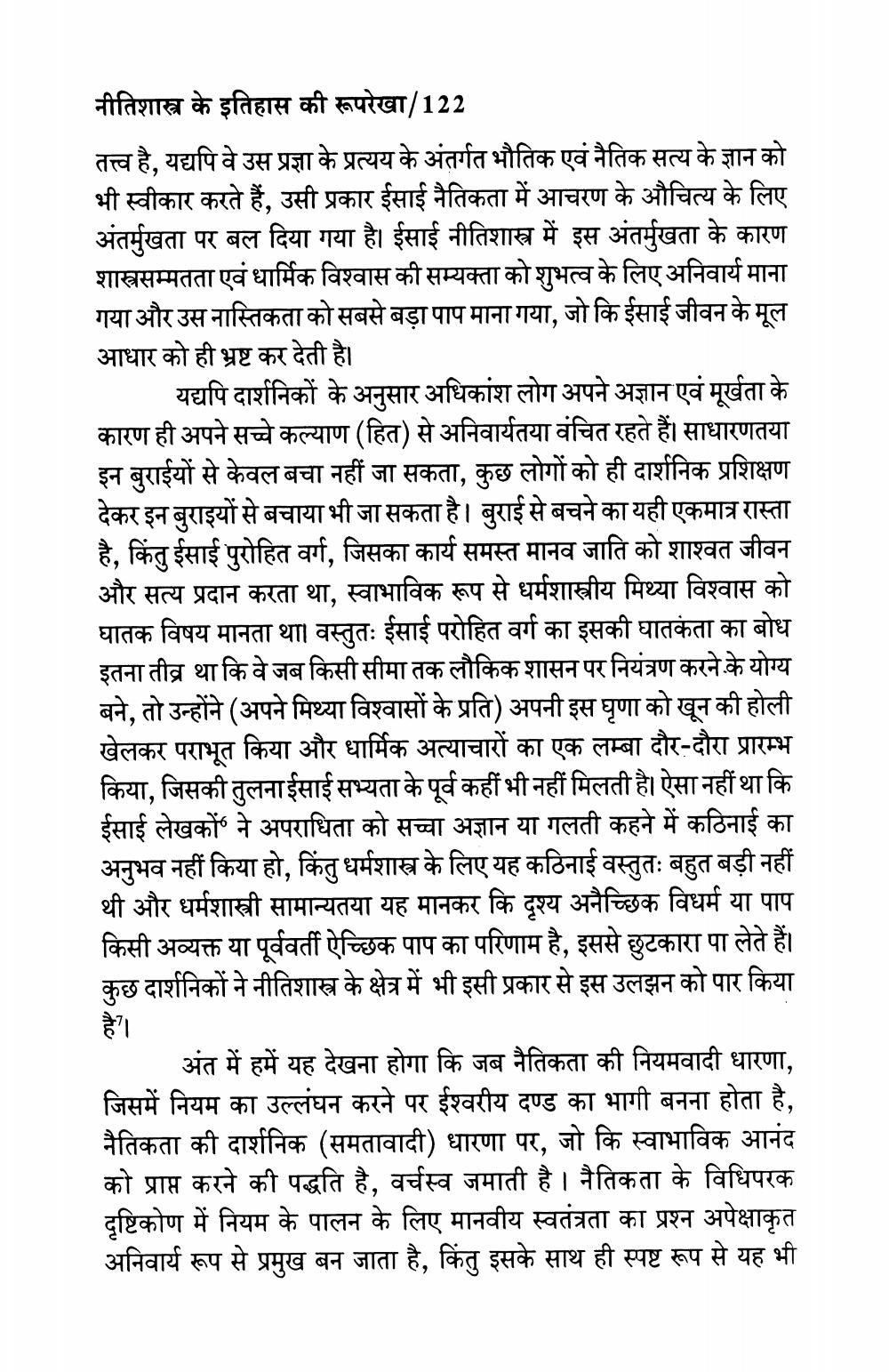________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/122 तत्त्व है, यद्यपि वे उस प्रज्ञा के प्रत्यय के अंतर्गत भौतिक एवं नैतिक सत्य के ज्ञान को भी स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ईसाई नैतिकता में आचरण के औचित्य के लिए अंतर्मुखता पर बल दिया गया है। ईसाई नीतिशास्त्र में इस अंतर्मुखता के कारण शास्त्रसम्मतता एवं धार्मिक विश्वास की सम्यक्ता को शुभत्व के लिए अनिवार्य माना गया और उस नास्तिकता को सबसे बड़ा पाप माना गया, जो कि ईसाई जीवन के मूल आधार को ही भ्रष्ट कर देती है।
यद्यपि दार्शनिकों के अनुसार अधिकांश लोग अपने अज्ञान एवं मूर्खता के कारण ही अपने सच्चे कल्याण (हित) से अनिवार्यतया वंचित रहते हैं। साधारणतया इन बुराईयों से केवल बचा नहीं जा सकता, कुछ लोगों को ही दार्शनिक प्रशिक्षण देकर इन बुराइयों से बचाया भी जा सकता है। बुराई से बचने का यही एकमात्र रास्ता है, किंतु ईसाई पुरोहित वर्ग, जिसका कार्य समस्त मानव जाति को शाश्वत जीवन
और सत्य प्रदान करता था, स्वाभाविक रूप से धर्मशास्त्रीय मिथ्या विश्वास को घातक विषय मानता था। वस्तुतः ईसाई परोहित वर्ग का इसकी घातकंता का बोध इतना तीव्र था कि वे जब किसी सीमा तक लौकिक शासन पर नियंत्रण करने के योग्य बने, तो उन्होंने (अपने मिथ्या विश्वासों के प्रति) अपनी इस घृणा को खून की होली खेलकर पराभूत किया और धार्मिक अत्याचारों का एक लम्बा दौर-दौरा प्रारम्भ किया, जिसकी तुलनाईसाई सभ्यता के पूर्व कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं था कि ईसाई लेखकों ने अपराधिता को सच्चा अज्ञान या गलती कहने में कठिनाई का अनुभव नहीं किया हो, किंतु धर्मशास्त्र के लिए यह कठिनाई वस्तुतः बहुत बड़ी नहीं थी और धर्मशास्त्री सामान्यतया यह मानकर कि दृश्य अनैच्छिक विधर्म या पाप किसी अव्यक्त या पूर्ववर्ती ऐच्छिक पाप का परिणाम है, इससे छुटकारा पा लेते हैं। कुछ दार्शनिकों ने नीतिशास्त्र के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से इस उलझन को पार किया
अंत में हमें यह देखना होगा कि जब नैतिकता की नियमवादी धारणा, जिसमें नियम का उल्लंघन करने पर ईश्वरीय दण्ड का भागी बनना होता है, नैतिकता की दार्शनिक (समतावादी) धारणा पर, जो कि स्वाभाविक आनंद को प्राप्त करने की पद्धति है, वर्चस्व जमाती है। नैतिकता के विधिपरक दृष्टिकोण में नियम के पालन के लिए मानवीय स्वतंत्रता का प्रश्न अपेक्षाकृत अनिवार्य रूप से प्रमुख बन जाता है, किंतु इसके साथ ही स्पष्ट रूप से यह भी