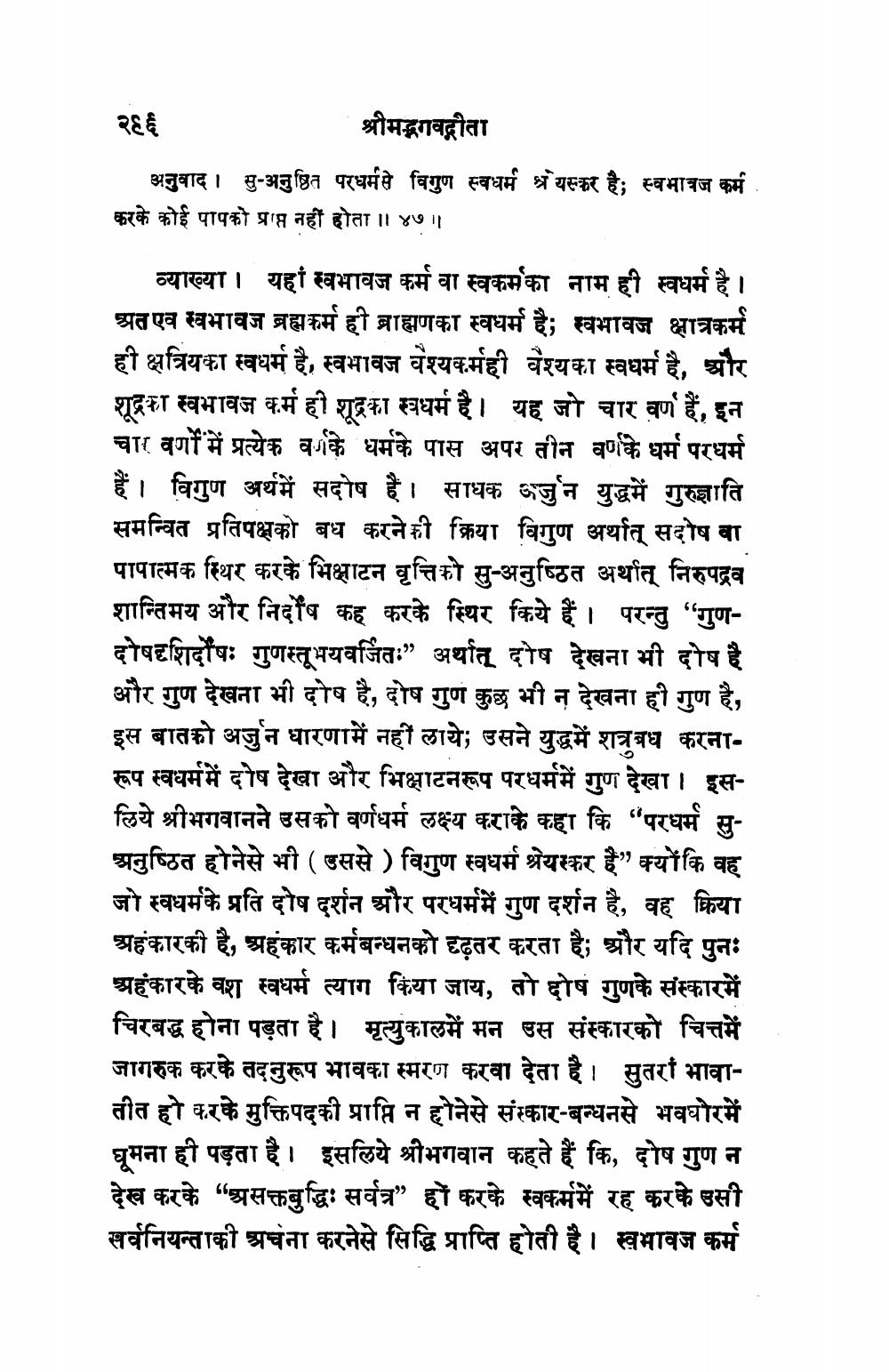________________
२६६
श्रीमद्भगवद्गीता अनुवाद। सु-अनुष्ठित परधर्मसे विगुण स्वधर्म श्रेयस्कर है; स्वभावज कर्म करके कोई पापको प्राप्त नहीं होता ।। ४७ ॥
व्याख्या। यहां स्वभावज कर्म वा स्वकर्मका नाम ही स्वधर्म है । अत एव स्वभावज ब्रह्मकर्म ही ब्राह्मणका स्वधर्म है; स्वभावज क्षात्रकर्म ही क्षत्रियका स्वधर्म है, स्वभावज वैश्यकर्मही वैश्यका स्वधर्म है, और शूद्रका स्वभावज कर्म ही शूद्रका स्वधर्म है। यह जो चार वर्ण हैं, इन चार वर्गों में प्रत्येक वर्गके धर्मके पास अपर तीन वर्णके धर्म परधर्म हैं। विगुण अर्थमें सदोष हैं। साधक अर्जुन युद्धमें गुरुज्ञाति समन्वित प्रतिपक्षको बध करने की क्रिया विगुण अर्थात् सदोष वा पापात्मक स्थिर करके भिक्षाटन वृत्तिको सु-अनुष्ठित अर्थात् निरुपद्रव शान्तिमय और निर्दोष कह करके स्थिर किये हैं। परन्तु "गुणदोषदृशिर्दोषः गुणस्तूभयवर्जितः” अर्थात् दोष देखना भी दोष है
और गुण देखना भी दोष है, दोष गुण कुछ भी न देखना ही गुण है, इस बातको अर्जुन धारणामें नहीं लाये; उसने युद्ध में शत्रुबध करनारूप स्वधर्म में दोष देखा और भिक्षाटनरूप परधर्ममें गुण देखा। इसलिये श्रीभगवानने उसको वर्णधर्म लक्ष्य कराके कहा कि "परधर्म सुअनुष्ठित होनेसे भी ( उससे ) विगुण स्वधर्म श्रेयस्कर है" क्योंकि वह जो स्वधर्मके प्रति दोष दर्शन और परधर्ममें गुण दर्शन है, वह क्रिया अहंकारकी है, अहंकार कर्मबन्धनको दृढ़तर करता है, और यदि पुनः अहंकारके वश स्वधर्म त्याग किया जाय, तो दोष गुणके संस्कारमें चिरबद्ध होना पड़ता है। मृत्युकालमें मन उस संस्कारको चित्तमें जागरुक करके तदनुरूप भावका स्मरण करवा देता है। सुतरां भावातीत हो करके मुक्तिपदकी प्राप्ति न होनेसे संस्कार-बन्धनसे भवघोरमें घूमना ही पड़ता है। इसलिये श्रीभगवान कहते हैं कि, दोष गुण न देख करके "असक्तबुद्धिः सर्वत्र” हो करके स्वकर्ममें रह करके उसी सर्वनियन्ताकी अर्चना करनेसे सिद्धि प्राप्ति होती है। स्वभावज कर्म
के मुक्तिपदी का स्मरण करवा इस संस्कारको संस्कारमें