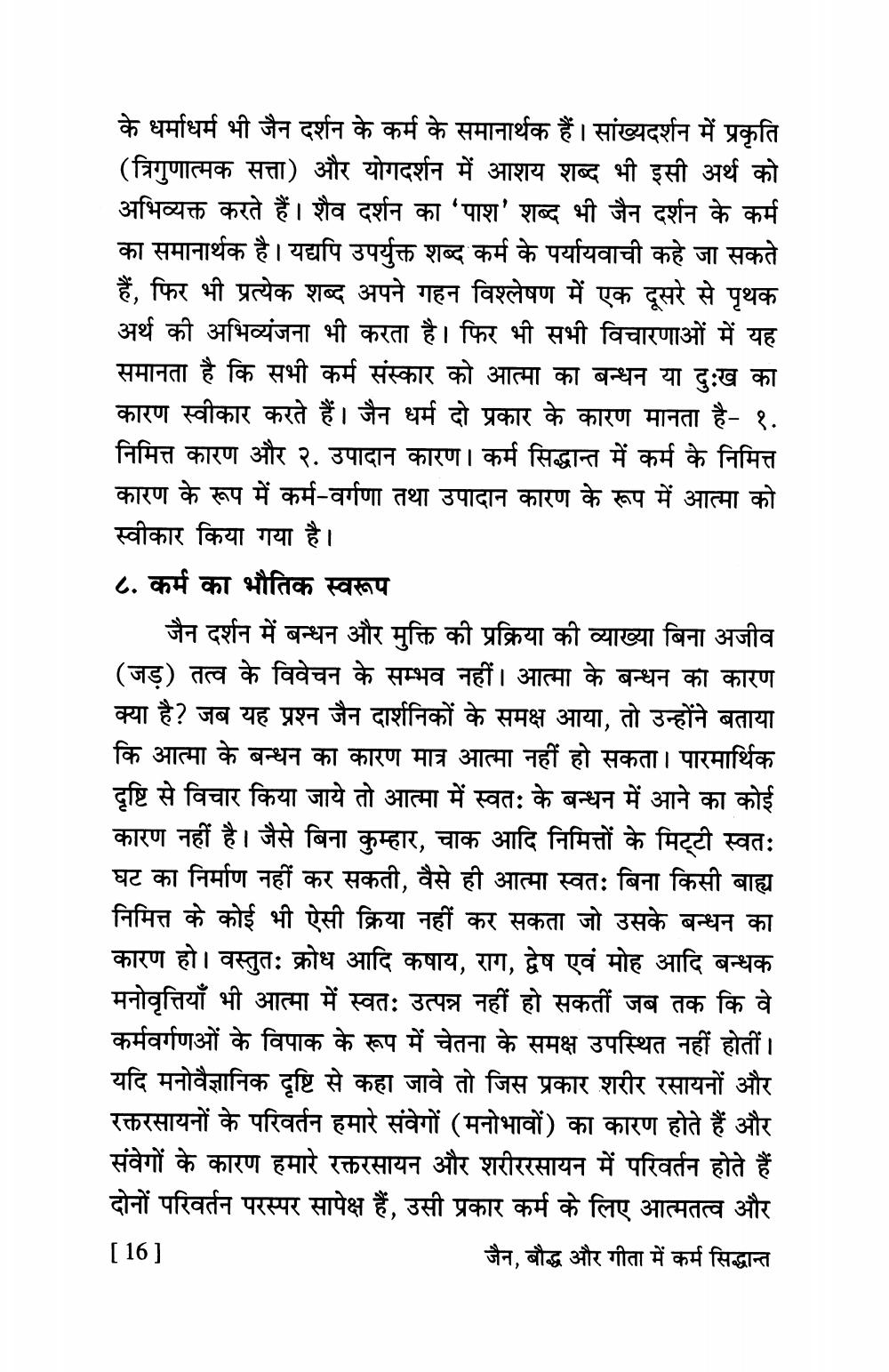________________
के धर्माधर्म भी जैन दर्शन के कर्म के समानार्थक हैं। सांख्यदर्शन में प्रकृति ( त्रिगुणात्मक सत्ता ) और योगदर्शन में आशय शब्द भी इसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं । शैव दर्शन का 'पाश' शब्द भी जैन दर्शन के कर्म का समानार्थक है। यद्यपि उपर्युक्त शब्द कर्म के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं, फिर भी प्रत्येक शब्द अपने गहन विश्लेषण में एक दूसरे से पृथक अर्थ की अभिव्यंजना भी करता है। फिर भी सभी विचारणाओं में यह समानता है कि सभी कर्म संस्कार को आत्मा का बन्धन या दुःख का कारण स्वीकार करते हैं । जैन धर्म दो प्रकार के कारण मानता है- १. निमित्त कारण और २. उपादान कारण । कर्म सिद्धान्त में कर्म के निमित्त कारण के रूप में कर्म-वर्गणा तथा उपादान कारण के रूप में आत्मा को स्वीकार किया गया है।
८. कर्म का भौतिक स्वरूप
जैन दर्शन में बन्धन और मुक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या बिना अजीव (जड़) तत्व के विवेचन के सम्भव नहीं । आत्मा के बन्धन का कारण क्या है? जब यह प्रश्न जैन दार्शनिकों के समक्ष आया, तो उन्होंने बताया कि आत्मा के बन्धन का कारण मात्र आत्मा नहीं हो सकता । पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाये तो आत्मा में स्वत: के बन्धन में आने का कोई कारण नहीं है। जैसे बिना कुम्हार, चाक आदि निमित्तों के मिट्टी स्वतः घट का निर्माण नहीं कर सकती, वैसे ही आत्मा स्वतः बिना किसी बाह्य निमित्त के कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर सकता जो उसके बन्धन का कारण हो । वस्तुतः क्रोध आदि कषाय, राग, द्वेष एवं मोह आदि बन्धक मनोवृत्तियाँ भी आत्मा में स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकतीं जब तक कि वे कर्मवर्गणओं के विपाक के रूप में चेतना के समक्ष उपस्थित नहीं होतीं । यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जावे तो जिस प्रकार शरीर रसायनों और रक्तरसायनों के परिवर्तन हमारे संवेगों (मनोभावों) का कारण होते हैं और संवेगों के कारण हमारे रक्तरसायन और शरीररसायन में परिवर्तन होते हैं दोनों परिवर्तन परस्पर सापेक्ष हैं, उसी प्रकार कर्म के लिए आत्मतत्व और जैन, बौद्ध और गीता में कर्म सिद्धान्त
[16]