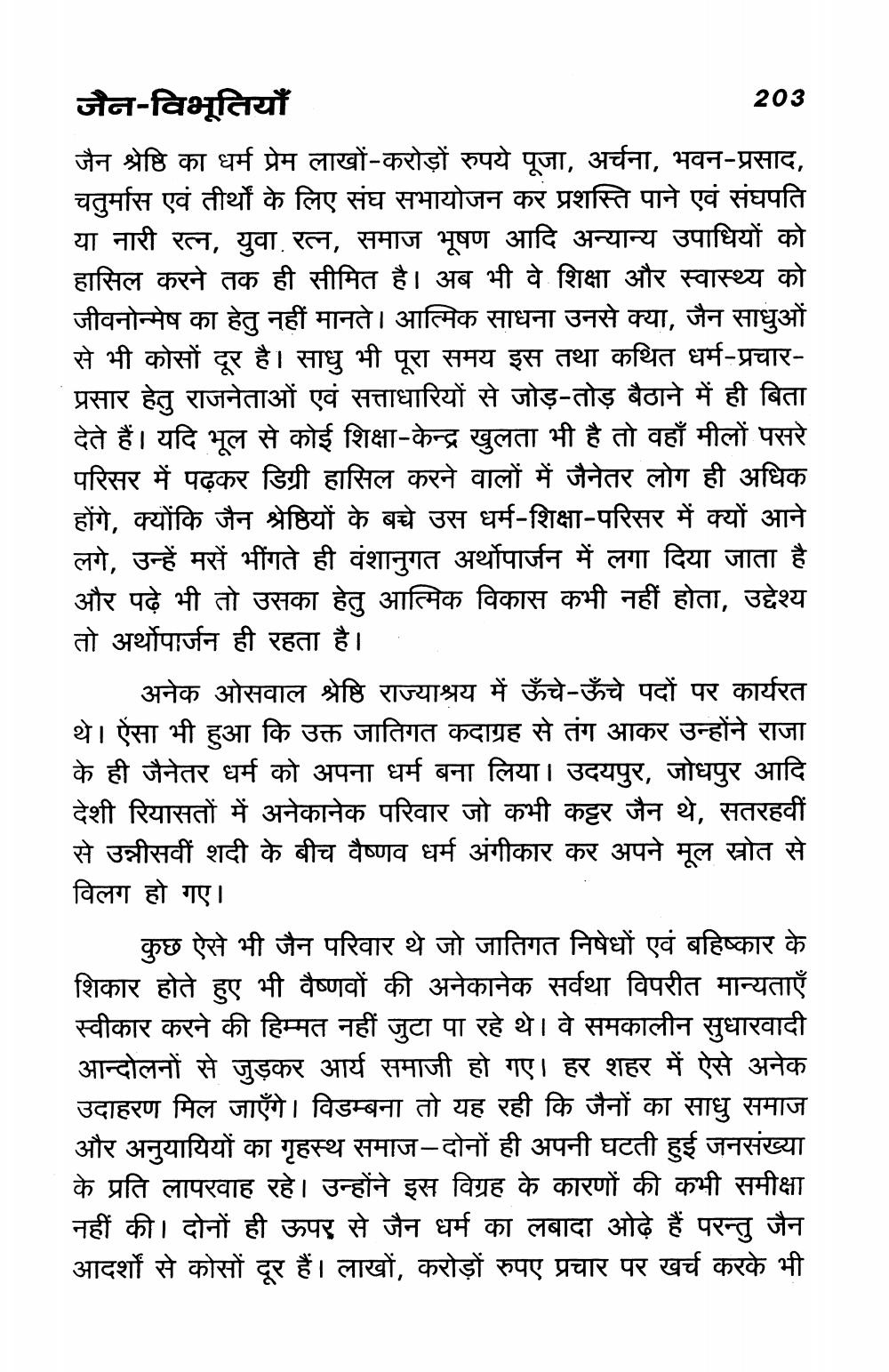________________
जैन-विभूतियाँ
203 जैन श्रेष्ठि का धर्म प्रेम लाखों-करोड़ों रुपये पूजा, अर्चना, भवन-प्रसाद, चतुर्मास एवं तीर्थों के लिए संघ सभायोजन कर प्रशस्ति पाने एवं संघपति या नारी रत्न, युवा रत्न, समाज भूषण आदि अन्यान्य उपाधियों को हासिल करने तक ही सीमित है। अब भी वे शिक्षा और स्वास्थ्य को जीवनोन्मेष का हेतु नहीं मानते। आत्मिक साधना उनसे क्या, जैन साधुओं से भी कोसों दूर है। साधु भी पूरा समय इस तथा कथित धर्म-प्रचारप्रसार हेतु राजनेताओं एवं सत्ताधारियों से जोड़-तोड़ बैठाने में ही बिता देते हैं। यदि भूल से कोई शिक्षा-केन्द्र खुलता भी है तो वहाँ मीलों पसरे परिसर में पढ़कर डिग्री हासिल करने वालों में जैनेतर लोग ही अधिक होंगे, क्योंकि जैन श्रेष्ठियों के बच्चे उस धर्म-शिक्षा-परिसर में क्यों आने लगे, उन्हें मसें भींगते ही वंशानुगत अर्थोपार्जन में लगा दिया जाता है
और पढ़े भी तो उसका हेतु आत्मिक विकास कभी नहीं होता, उद्देश्य तो अर्थोपार्जन ही रहता है। ..
अनेक ओसवाल श्रेष्ठि राज्याश्रय में ऊँचे-ऊँचे पदों पर कार्यरत थे। ऐसा भी हुआ कि उक्त जातिगत कदाग्रह से तंग आकर उन्होंने राजा के ही जैनेतर धर्म को अपना धर्म बना लिया। उदयपुर, जोधपुर आदि देशी रियासतों में अनेकानेक परिवार जो कभी कट्टर जैन थे, सतरहवीं से उन्नीसवीं शदी के बीच वैष्णव धर्म अंगीकार कर अपने मूल स्रोत से विलग हो गए।
कुछ ऐसे भी जैन परिवार थे जो जातिगत निषेधों एवं बहिष्कार के शिकार होते हुए भी वैष्णवों की अनेकानेक सर्वथा विपरीत मान्यताएँ स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे समकालीन सुधारवादी आन्दोलनों से जुड़कर आर्य समाजी हो गए। हर शहर में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएँगे। विडम्बना तो यह रही कि जैनों का साधु समाज और अनुयायियों का गृहस्थ समाज-दोनों ही अपनी घटती हुई जनसंख्या के प्रति लापरवाह रहे। उन्होंने इस विग्रह के कारणों की कभी समीक्षा नहीं की। दोनों ही ऊपर से जैन धर्म का लबादा ओढ़े हैं परन्तु जैन आदर्शों से कोसों दूर हैं। लाखों, करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च करके भी