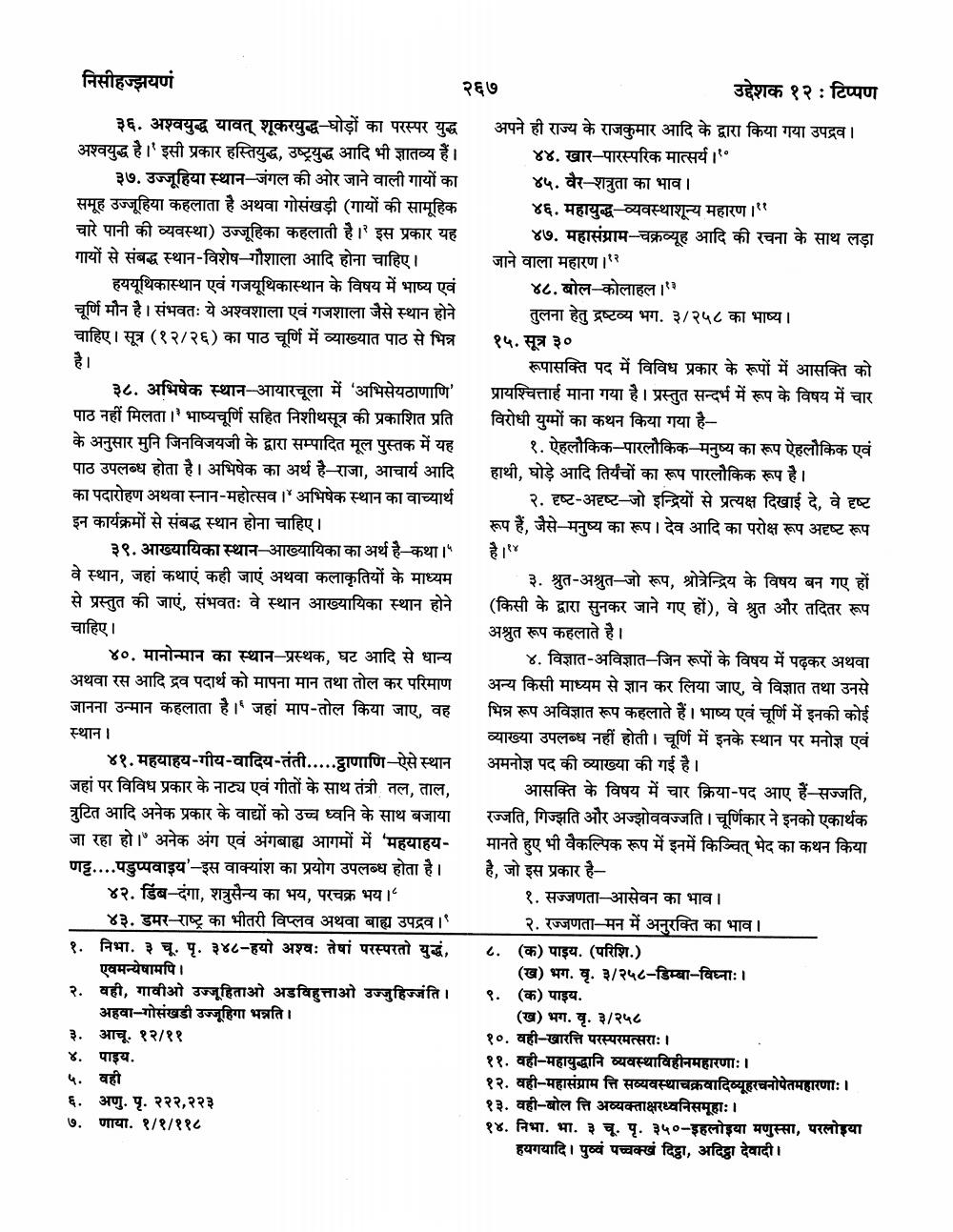________________
निसीहज्झयणं
२६७
उद्देशक १२:टिप्पण
८.
३६. अश्वयुद्ध यावत् शूकरयुद्ध-घोड़ों का परस्पर युद्ध अपने ही राज्य के राजकुमार आदि के द्वारा किया गया उपद्रव । अश्वयुद्ध है। इसी प्रकार हस्तियुद्ध, उष्ट्रयुद्ध आदि भी ज्ञातव्य हैं। ४४. खार-पारस्परिक मात्सर्य।
३७. उज्जूहिया स्थान-जंगल की ओर जाने वाली गायों का ४५. वैर-शत्रुता का भाव। समूह उज्जूहिया कहलाता है अथवा गोसंखड़ी (गायों की सामूहिक ४६. महायुद्ध-व्यवस्थाशून्य महारण।" चारे पानी की व्यवस्था) उज्जूहिका कहलाती है। इस प्रकार यह ४७. महासंग्राम-चक्रव्यूह आदि की रचना के साथ लड़ा गायों से संबद्ध स्थान-विशेष-गौशाला आदि होना चाहिए। जाने वाला महारण।१२
हययूथिकास्थान एवं गजयूथिकास्थान के विषय में भाष्य एवं ४८. बोल-कोलाहल।३ चूर्णि मौन है। संभवतः ये अश्वशाला एवं गजशाला जैसे स्थान होने तुलना हेतु द्रष्टव्य भग. ३/२५८ का भाष्य। चाहिए। सूत्र (१२/२६) का पाठ चूर्णि में व्याख्यात पाठ से भिन्न १५. सूत्र ३०
रूपासक्ति पद में विविध प्रकार के रूपों में आसक्ति को ३८. अभिषेक स्थान-आयारचूला में 'अभिसेयठाणाणि' प्रायश्चित्तार्ह माना गया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में रूप के विषय में चार पाठ नहीं मिलता। भाष्यचूर्णि सहित निशीथसूत्र की प्रकाशित प्रति विरोधी युग्मों का कथन किया गया हैके अनुसार मुनि जिनविजयजी के द्वारा सम्पादित मूल पुस्तक में यह १. ऐहलौकिक-पारलौकिक-मनुष्य का रूप ऐहलौकिक एवं पाठ उपलब्ध होता है। अभिषेक का अर्थ है-राजा, आचार्य आदि हाथी, घोड़े आदि तिर्यंचों का रूप पारलौकिक रूप है। का पदारोहण अथवा स्नान-महोत्सव। अभिषेक स्थान का वाच्यार्थ २. दृष्ट-अदृष्ट-जो इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई दे, वे दृष्ट इन कार्यक्रमों से संबद्ध स्थान होना चाहिए।
रूप हैं, जैसे-मनुष्य का रूप। देव आदि का परोक्ष रूप अदृष्ट रूप ३९. आख्यायिका स्थान-आख्यायिका का अर्थ है-कथा।' वे स्थान, जहां कथाएं कही जाएं अथवा कलाकृतियों के माध्यम ३. श्रुत-अश्रुत-जो रूप, श्रोत्रेन्द्रिय के विषय बन गए हों से प्रस्तुत की जाएं, संभवतः वे स्थान आख्यायिका स्थान होने (किसी के द्वारा सुनकर जाने गए हों), वे श्रुत और तदितर रूप चाहिए।
अश्रुत रूप कहलाते है। ४०. मानोन्मान का स्थान-प्रस्थक, घट आदि से धान्य ४. विज्ञात-अविज्ञात-जिन रूपों के विषय में पढ़कर अथवा अथवा रस आदि द्रव पदार्थ को मापना मान तथा तोल कर परिमाण ___अन्य किसी माध्यम से ज्ञान कर लिया जाए, वे विज्ञात तथा उनसे जानना उन्मान कहलाता है। जहां माप-तोल किया जाए, वह भिन्न रूप अविज्ञात रूप कहलाते हैं। भाष्य एवं चूर्णि में इनकी कोई स्थान।
व्याख्या उपलब्ध नहीं होती। चूर्णि में इनके स्थान पर मनोज्ञ एवं ४१. महयाहय-गीय-वादिय-तंती.....ट्ठाणाणि-ऐसे स्थान अमनोज्ञ पद की व्याख्या की गई है। जहां पर विविध प्रकार के नाट्य एवं गीतों के साथ तंत्री तल, ताल, आसक्ति के विषय में चार क्रिया-पद आए हैं-सज्जति, त्रुटित आदि अनेक प्रकार के वाद्यों को उच्च ध्वनि के साथ बजाया रज्जति, गिज्झति और अज्झोववज्जति । चूर्णिकार ने इनको एकार्थक जा रहा हो। अनेक अंग एवं अंगबाह्य आगमों में 'महयाहय- मानते हुए भी वैकल्पिक रूप में इनमें किञ्चित् भेद का कथन किया णट्ट....पडुप्पवाइय'-इस वाक्यांश का प्रयोग उपलब्ध होता है। है, जो इस प्रकार है४२. डिंब-दंगा, शत्रुसैन्य का भय, परचक्र भय।
१. सज्जणता आसेवन का भाव। ४३. डमर-राष्ट्र का भीतरी विप्लव अथवा बाह्य उपद्रव। २. रज्जणता-मन में अनुरक्ति का भाव । १. निभा. ३ चू. पृ. ३४८-हयो अश्वः तेषां परस्परतो युद्धं, ८. (क) पाइय. (परिशि.) एवमन्येषामपि।
(ख) भग. वृ. ३/२५८-डिम्बा-विघ्नाः । २. वही, गावीओ उज्जूहिताओ अडविहुत्ताओ उज्जुहिज्जति। ९. (क) पाइय. अहवा-गोसंखडी उज्जूहिगा भन्नति।
(ख) भग. ७.३/२५८ ३. आचू. १२/११
१०. वही-खारत्ति परस्परमत्सराः। ४. पाइय.
११. वही-महायुद्धानि व्यवस्थाविहीनमहारणाः। ५. वही
१२. वही-महासंग्राम ति सव्यवस्थाचक्रवादिव्यूहरचनोपेतमहारणाः । ६. अणु. पृ. २२२,२२३
१३. वही-बोल त्ति अव्यक्ताक्षरध्वनिसमूहाः। ७. णाया. १/१/११८
१४. निभा. भा. ३ चू. पृ. ३५०-इहलोइया मणुस्सा, परलोइया
हयगयादि। पुव्वं पच्चक्खं दिट्ठा, अदिट्ठा देवादी।