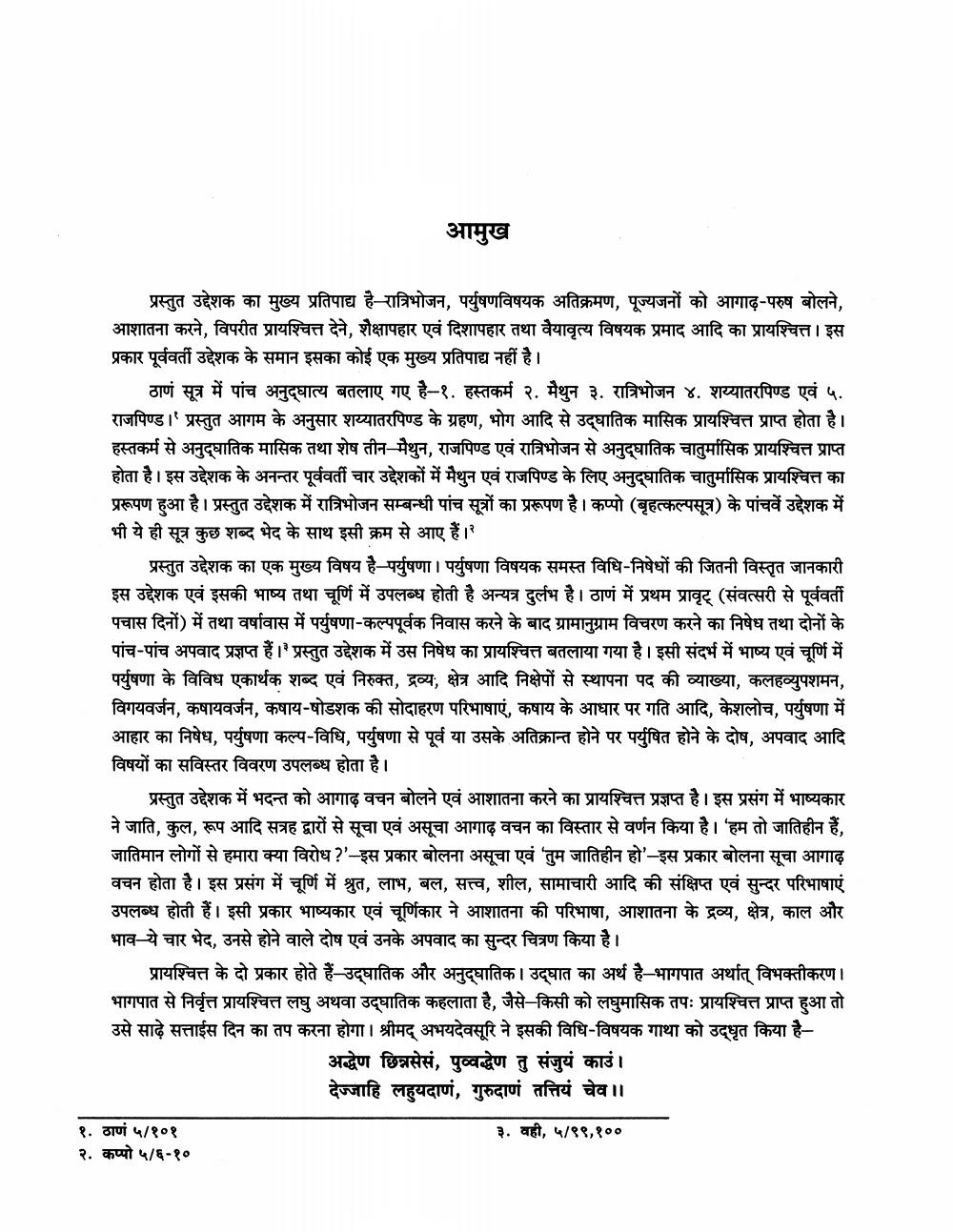________________
आमुख
प्रस्तुत उद्देशक का मुख्य प्रतिपाद्य है-रात्रिभोजन, पर्युषणविषयक अतिक्रमण, पूज्यजनों को आगाढ़-परुष बोलने, आशातना करने, विपरीत प्रायश्चित्त देने, शैक्षापहार एवं दिशापहार तथा वैयावृत्य विषयक प्रमाद आदि का प्रायश्चित्त। इस प्रकार पूर्ववर्ती उद्देशक के समान इसका कोई एक मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है।
ठाणं सूत्र में पांच अनुदात्य बतलाए गए है-१. हस्तकर्म २. मैथुन ३. रात्रिभोजन ४. शय्यातरपिण्ड एवं ५. राजपिण्ड।' प्रस्तुत आगम के अनुसार शय्यातरपिण्ड के ग्रहण, भोग आदि से उद्घातिक मासिक प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। हस्तकर्म से अनुद्घातिक मासिक तथा शेष तीन-मैथुन, राजपिण्ड एवं रात्रिभोजन से अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। इस उद्देशक के अनन्तर पूर्ववर्ती चार उद्देशकों में मैथुन एवं राजपिण्ड के लिए अनुद्घातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का प्ररूपण हुआ है। प्रस्तुत उद्देशक में रात्रिभोजन सम्बन्धी पांच सूत्रों का प्ररूपण है। कप्पो (बृहत्कल्पसूत्र) के पांचवें उद्देशक में भी ये ही सूत्र कुछ शब्द भेद के साथ इसी क्रम से आए हैं।
प्रस्तुत उद्देशक का एक मुख्य विषय है-पर्युषणा। पर्युषणा विषयक समस्त विधि-निषेधों की जितनी विस्तृत जानकारी इस उद्देशक एवं इसकी भाष्य तथा चूर्णि में उपलब्ध होती है अन्यत्र दुर्लभ है। ठाणं में प्रथम प्रावृट् (संवत्सरी से पूर्ववर्ती पचास दिनों) में तथा वर्षावास में पर्युषणा-कल्पपूर्वक निवास करने के बाद ग्रामानुग्राम विचरण करने का निषेध तथा दोनों के पांच-पांच अपवाद प्रज्ञप्त हैं। प्रस्तुत उद्देशक में उस निषेध का प्रायश्चित्त बतलाया गया है। इसी संदर्भ में भाष्य एवं चूर्णि में पर्युषणा के विविध एकार्थक शब्द एवं निरुक्त, द्रव्य, क्षेत्र आदि निक्षेपों से स्थापना पद की व्याख्या, कलहव्युपशमन, विगयवर्जन, कषायवर्जन, कषाय-षोडशक की सोदाहरण परिभाषाएं, कषाय के आधार पर गति आदि, केशलोच, पर्युषणा में
आहार का निषेध, पर्युषणा कल्प-विधि, पर्युषणा से पूर्व या उसके अतिक्रान्त होने पर पर्युषित होने के दोष, अपवाद आदि विषयों का सविस्तर विवरण उपलब्ध होता है।
प्रस्तुत उद्देशक में भदन्त को आगाढ़ वचन बोलने एवं आशातना करने का प्रायश्चित्त प्रज्ञप्त है। इस प्रसंग में भाष्यकार ने जाति, कुल, रूप आदि सत्रह द्वारों से सूचा एवं असूचा आगाढ़ वचन का विस्तार से वर्णन किया है। 'हम तो जातिहीन हैं, जातिमान लोगों से हमारा क्या विरोध?'-इस प्रकार बोलना असूचा एवं 'तुम जातिहीन हो'-इस प्रकार बोलना सूचा आगाढ़ वचन होता है। इस प्रसंग में चूर्णि में श्रुत, लाभ, बल, सत्त्व, शील, सामाचारी आदि की संक्षिप्त एवं सुन्दर परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार भाष्यकार एवं चूर्णिकार ने आशातना की परिभाषा, आशातना के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-ये चार भेद, उनसे होने वाले दोष एवं उनके अपवाद का सुन्दर चित्रण किया है।
प्रायश्चित्त के दो प्रकार होते हैं उद्घातिक और अनुद्घातिक। उद्घात का अर्थ है-भागपात अर्थात् विभक्तीकरण। भागपात से निवृत्त प्रायश्चित्त लघु अथवा उद्घातिक कहलाता है, जैसे किसी को लघुमासिक तपः प्रायश्चित्त प्राप्त हुआ तो उसे साढ़े सत्ताईस दिन का तप करना होगा। श्रीमद् अभयदेवसूरि ने इसकी विधि-विषयक गाथा को उद्धृत किया है
अद्धेण छिन्नसेसं, पुव्वद्धेण तु संजुयं काउं। देज्जाहि लहुयदाणं, गुरुदाणं तत्तियं चेव॥
३. वही, ५/९९,१००
१. ठाणं ५/१०१ २. कप्पो ५/६-१०