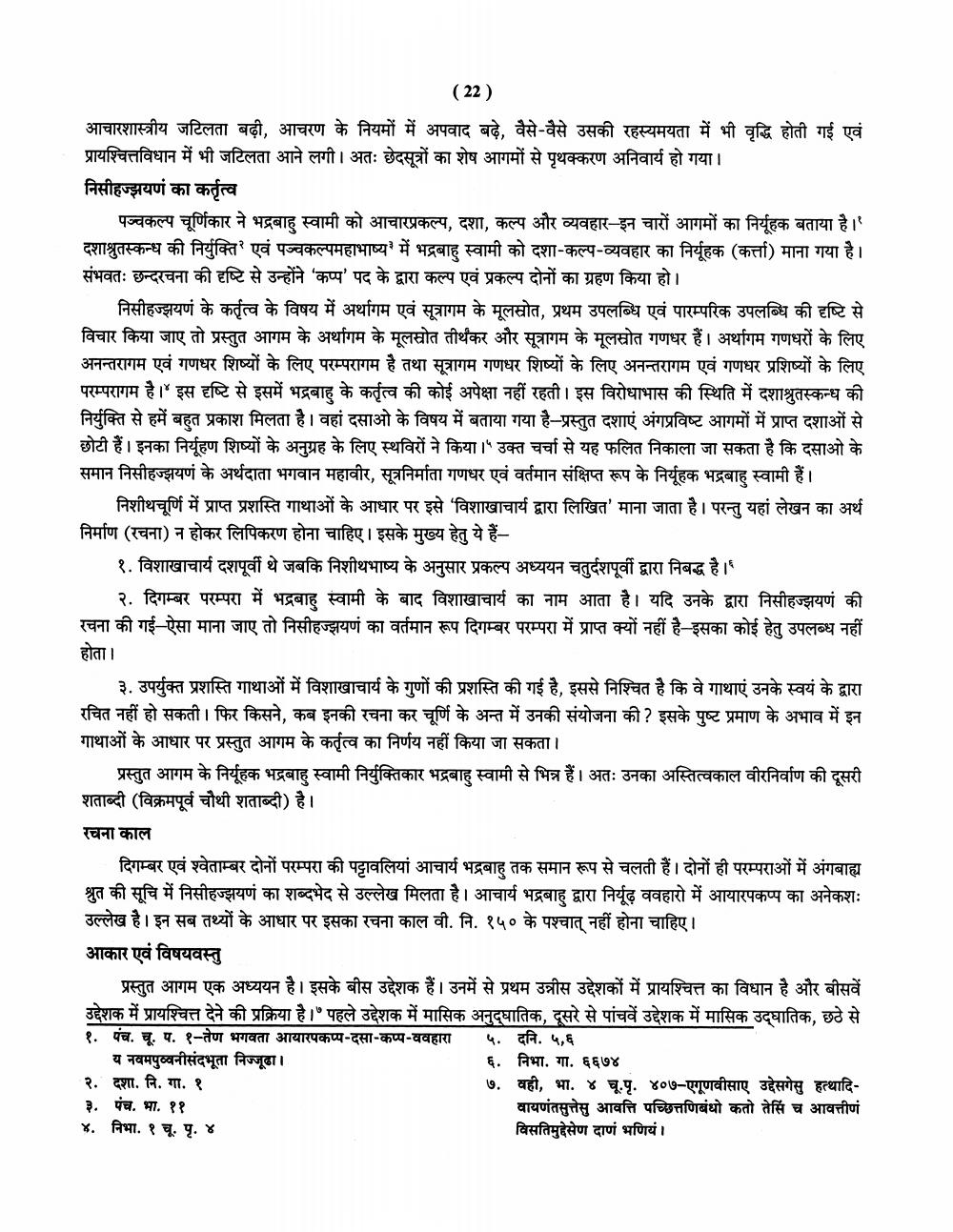________________
(22) आचारशास्त्रीय जटिलता बढ़ी, आचरण के नियमों में अपवाद बढ़े, वैसे-वैसे उसकी रहस्यमयता में भी वृद्धि होती गई एवं प्रायश्चित्तविधान में भी जटिलता आने लगी। अतः छेदसूत्रों का शेष आगमों से पृथक्करण अनिवार्य हो गया। निसीहज्झयणं का कर्तृत्व
पञ्चकल्प चूर्णिकार ने भद्रबाहु स्वामी को आचारप्रकल्प, दशा, कल्प और व्यवहार-इन चारों आगमों का निर्वृहक बताया है।' दशाश्रुतस्कन्ध की नियुक्ति एवं पञ्चकल्पमहाभाष्य में भद्रबाह स्वामी को दशा-कल्प-व्यवहार का निर्वृहक (कर्ता) माना गया है। संभवतः छन्दरचना की दृष्टि से उन्होंने 'कप्प' पद के द्वारा कल्प एवं प्रकल्प दोनों का ग्रहण किया हो।
निसीहज्झयणं के कर्तृत्व के विषय में अर्थागम एवं सूत्रागम के मूलस्रोत, प्रथम उपलब्धि एवं पारम्परिक उपलब्धि की दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रस्तुत आगम के अर्थागम के मूलस्रोत तीर्थंकर और सूत्रागम के मूलस्रोत गणधर हैं। अर्थागम गणधरों के लिए अनन्तरागम एवं गणधर शिष्यों के लिए परम्परागम है तथा सूत्रागम गणधर शिष्यों के लिए अनन्तरागम एवं गणधर प्रशिष्यों के लिए परम्परागम है। इस दृष्टि से इसमें भद्रबाहु के कर्तृत्व की कोई अपेक्षा नहीं रहती। इस विरोधाभास की स्थिति में दशाश्रुतस्कन्ध की नियुक्ति से हमें बहुत प्रकाश मिलता है। वहां दसाओ के विषय में बताया गया है-प्रस्तुत दशाएं अंगप्रविष्ट आगमों में प्राप्त दशाओं से छोटी हैं। इनका निप॑हण शिष्यों के अनुग्रह के लिए स्थविरों ने किया। उक्त चर्चा से यह फलित निकाला जा सकता है कि दसाओ के समान निसीहज्झयणं के अर्थदाता भगवान महावीर, सूत्रनिर्माता गणधर एवं वर्तमान संक्षिप्त रूप के निर्वृहक भद्रबाहु स्वामी हैं।
निशीथचूर्णि में प्राप्त प्रशस्ति गाथाओं के आधार पर इसे 'विशाखाचार्य द्वारा लिखित' माना जाता है। परन्तु यहां लेखन का अर्थ निर्माण (रचना) न होकर लिपिकरण होना चाहिए। इसके मुख्य हेतु ये हैं
१. विशाखाचार्य दशपूर्वी थे जबकि निशीथभाष्य के अनुसार प्रकल्प अध्ययन चतुर्दशपूर्वी द्वारा निबद्ध है।
२. दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु स्वामी के बाद विशाखाचार्य का नाम आता है। यदि उनके द्वारा निसीहज्झयणं की रचना की गई-ऐसा माना जाए तो निसीहज्झयणं का वर्तमान रूप दिगम्बर परम्परा में प्राप्त क्यों नहीं है इसका कोई हेतु उपलब्ध नहीं होता।
३. उपर्युक्त प्रशस्ति गाथाओं में विशाखाचार्य के गुणों की प्रशस्ति की गई है, इससे निश्चित है कि वे गाथाएं उनके स्वयं के द्वारा रचित नहीं हो सकती। फिर किसने, कब इनकी रचना कर चूर्णि के अन्त में उनकी संयोजना की? इसके पुष्ट प्रमाण के अभाव में इन गाथाओं के आधार पर प्रस्तुत आगम के कर्तृत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता।
प्रस्तुत आगम के निर्वृहक भद्रबाहु स्वामी नियुक्तिकार भद्रबाहु स्वामी से भिन्न हैं। अतः उनका अस्तित्वकाल वीरनिर्वाण की दूसरी शताब्दी (विक्रमपूर्व चौथी शताब्दी) है। रचना काल
दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों परम्परा की पट्टावलियां आचार्य भद्रबाह तक समान रूप से चलती हैं। दोनों ही परम्पराओं में अंगबाह्य श्रुत की सूचि में निसीहज्झयणं का शब्दभेद से उल्लेख मिलता है। आचार्य भद्रबाहु द्वारा निर्मूढ़ ववहारो में आयारपकप्प का अनेकशः उल्लेख है। इन सब तथ्यों के आधार पर इसका रचना काल वी. नि. १५० के पश्चात् नहीं होना चाहिए। आकार एवं विषयवस्तु
प्रस्तुत आगम एक अध्ययन है। इसके बीस उद्देशक हैं। उनमें से प्रथम उन्नीस उद्देशकों में प्रायश्चित्त का विधान है और बीसवें उद्देशक में प्रायश्चित्त देने की प्रक्रिया है। पहले उद्देशक में मासिक अनुद्घातिक, दूसरे से पांचवें उद्देशक में मासिक उद्घातिक, छठे से १. पंच. चू. प. १-तेण भगवता आयारपकप्प-दसा-कप्प-ववहारा ५. दनि. ५,६ य नवमपुव्वनीसंदभूता निज्जूढा।
६. निभा. गा. ६६७४ २. दशा. नि. गा. १
७. वही, भा. ४ चू.पृ. ४०७-एगूणवीसाए उद्देसगेसु हत्थादि३. पंच. भा. ११
वायणंतसुत्तेसु आवत्ति पच्छित्तणिबंधो कतो तेसिं च आवत्तीणं ४. निभा. १ चू. पृ. ४
विसतिमुद्देसेण दाणं भणियं।