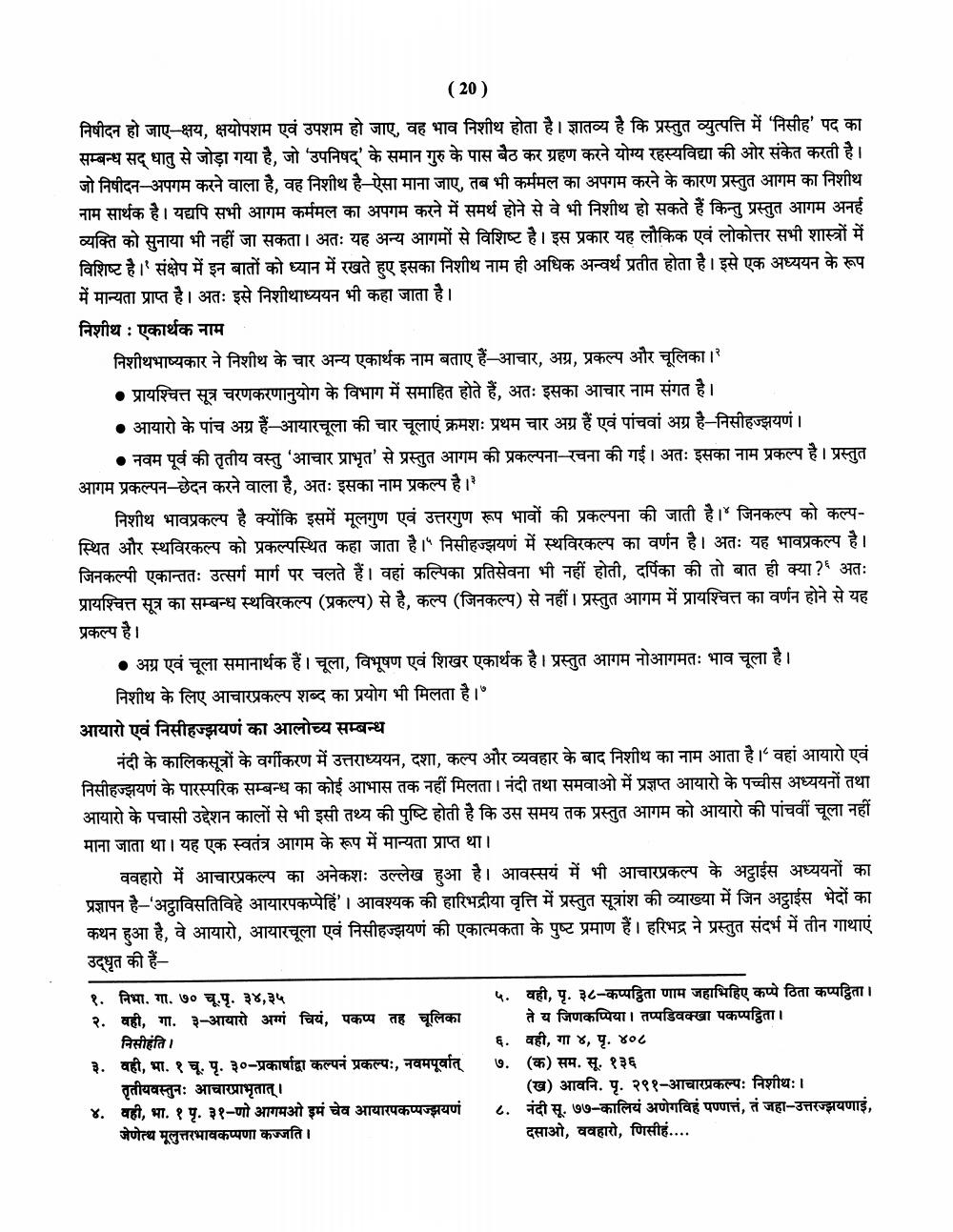________________
(20) निषीदन हो जाए-क्षय, क्षयोपशम एवं उपशम हो जाए, वह भाव निशीथ होता है। ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत व्युत्पत्ति में 'निसीह' पद का सम्बन्ध सद् धातु से जोड़ा गया है, जो 'उपनिषद्' के समान गुरु के पास बैठ कर ग्रहण करने योग्य रहस्यविद्या की ओर संकेत करती है। जो निषीदन-अपगम करने वाला है, वह निशीथ है-ऐसा माना जाए, तब भी कर्ममल का अपगम करने के कारण प्रस्तुत आगम का निशीथ नाम सार्थक है। यद्यपि सभी आगम कर्ममल का अपगम करने में समर्थ होने से वे भी निशीथ हो सकते हैं किन्तु प्रस्तुत आगम अनर्ह व्यक्ति को सुनाया भी नहीं जा सकता। अतः यह अन्य आगमों से विशिष्ट है। इस प्रकार यह लौकिक एवं लोकोत्तर सभी शास्त्रों में विशिष्ट है। संक्षेप में इन बातों को ध्यान में रखते हए इसका निशीथ नाम ही अधिक अन्वर्थ प्रतीत होता है। इसे एक अध्ययन के रूप में मान्यता प्राप्त है। अतः इसे निशीथाध्ययन भी कहा जाता है। निशीथ : एकार्थक नाम ।
निशीथभाष्यकार ने निशीथ के चार अन्य एकार्थक नाम बताए हैं आचार, अग्र, प्रकल्प और चूलिका। • प्रायश्चित्त सूत्र चरणकरणानुयोग के विभाग में समाहित होते हैं, अतः इसका आचार नाम संगत है। • आयारो के पांच अग्र हैं आयारचूला की चार चूलाएं क्रमशः प्रथम चार अग्र हैं एवं पांचवां अग्र है-निसीहज्झयणं ।
• नवम पूर्व की तृतीय वस्तु 'आचार प्राभृत' से प्रस्तुत आगम की प्रकल्पना-रचना की गई। अतः इसका नाम प्रकल्प है। प्रस्तुत आगम प्रकल्पन-छेदन करने वाला है, अतः इसका नाम प्रकल्प है।
निशीथ भावप्रकल्प है क्योंकि इसमें मूलगुण एवं उत्तरगुण रूप भावों की प्रकल्पना की जाती है। जिनकल्प को कल्पस्थित और स्थविरकल्प को प्रकल्पस्थित कहा जाता है। निसीहज्झयणं में स्थविरकल्प का वर्णन है। अतः यह भावप्रकल्प है। जिनकल्पी एकान्ततः उत्सर्ग मार्ग पर चलते हैं। वहां कल्पिका प्रतिसेवना भी नहीं होती, दर्पिका की तो बात ही क्या? अतः प्रायश्चित्त सूत्र का सम्बन्ध स्थविरकल्प (प्रकल्प) से है, कल्प (जिनकल्प) से नहीं। प्रस्तुत आगम में प्रायश्चित्त का वर्णन होने से यह प्रकल्प है।
• अग्र एवं चूला समानार्थक हैं। चूला, विभूषण एवं शिखर एकार्थक है। प्रस्तुत आगम नोआगमतः भाव चूला है।
निशीथ के लिए आचारप्रकल्प शब्द का प्रयोग भी मिलता है।' आयारो एवं निसीहज्झयणं का आलोच्य सम्बन्ध
नंदी के कालिकसूत्रों के वर्गीकरण में उत्तराध्ययन, दशा, कल्प और व्यवहार के बाद निशीथ का नाम आता है। वहां आयारो एवं निसीहज्झयणं के पारस्परिक सम्बन्ध का कोई आभास तक नहीं मिलता। नंदी तथा समवाओ में प्रज्ञप्त आयारो के पच्चीस अध्ययनों तथा आयारो के पचासी उद्देशन कालों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि उस समय तक प्रस्तुत आगम को आयारो की पांचवीं चूला नहीं माना जाता था। यह एक स्वतंत्र आगम के रूप में मान्यता प्राप्त था।
ववहारो में आचारप्रकल्प का अनेकशः उल्लेख हुआ है। आवस्सयं में भी आचारप्रकल्प के अट्ठाईस अध्ययनों का प्रज्ञापन है-'अट्ठाविसतिविहे आयारपकप्पेहिं'। आवश्यक की हारिभद्रीया वृत्ति में प्रस्तुत सूत्रांश की व्याख्या में जिन अट्ठाईस भेदों का कथन हुआ है, वे आयारो, आयारचूला एवं निसीहज्झयणं की एकात्मकता के पुष्ट प्रमाण हैं। हरिभद्र ने प्रस्तुत संदर्भ में तीन गाथाएं उद्धृत की हैं१. निभा. गा. ७० चू.पृ. ३४,३५
५. वही, पृ. ३८-कप्पट्ठिता णाम जहाभिहिए कप्पे ठिता कप्पट्ठिता। २. वही, गा. ३-आयारो अग्गं चियं, पकप्प तह चूलिका ते य जिणकप्पिया। तप्पडिवक्खा पकप्पट्ठिता। निसीहंति।
६. वही, गा ४, पृ. ४०८ ३. वही, भा. १चू. पृ. ३०-प्रकार्षाद्वा कल्पनं प्रकल्पः, नवमपूर्वात् ७. (क) सम. सू. १३६ तृतीयवस्तुनः आचारप्राभृतात्।
(ख) आवनि. पृ. २९१-आचारप्रकल्पः निशीथः । ४. वही, भा. १ पृ. ३१-णो आगमओ इमं चेव आयारपकप्पज्झयणं नंदी सू. ७७-कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा-उत्तरज्झयणाई, जेणेत्थ मूलुत्तरभावकप्पणा कज्जति।
दसाओ, ववहारो, णिसीहं....