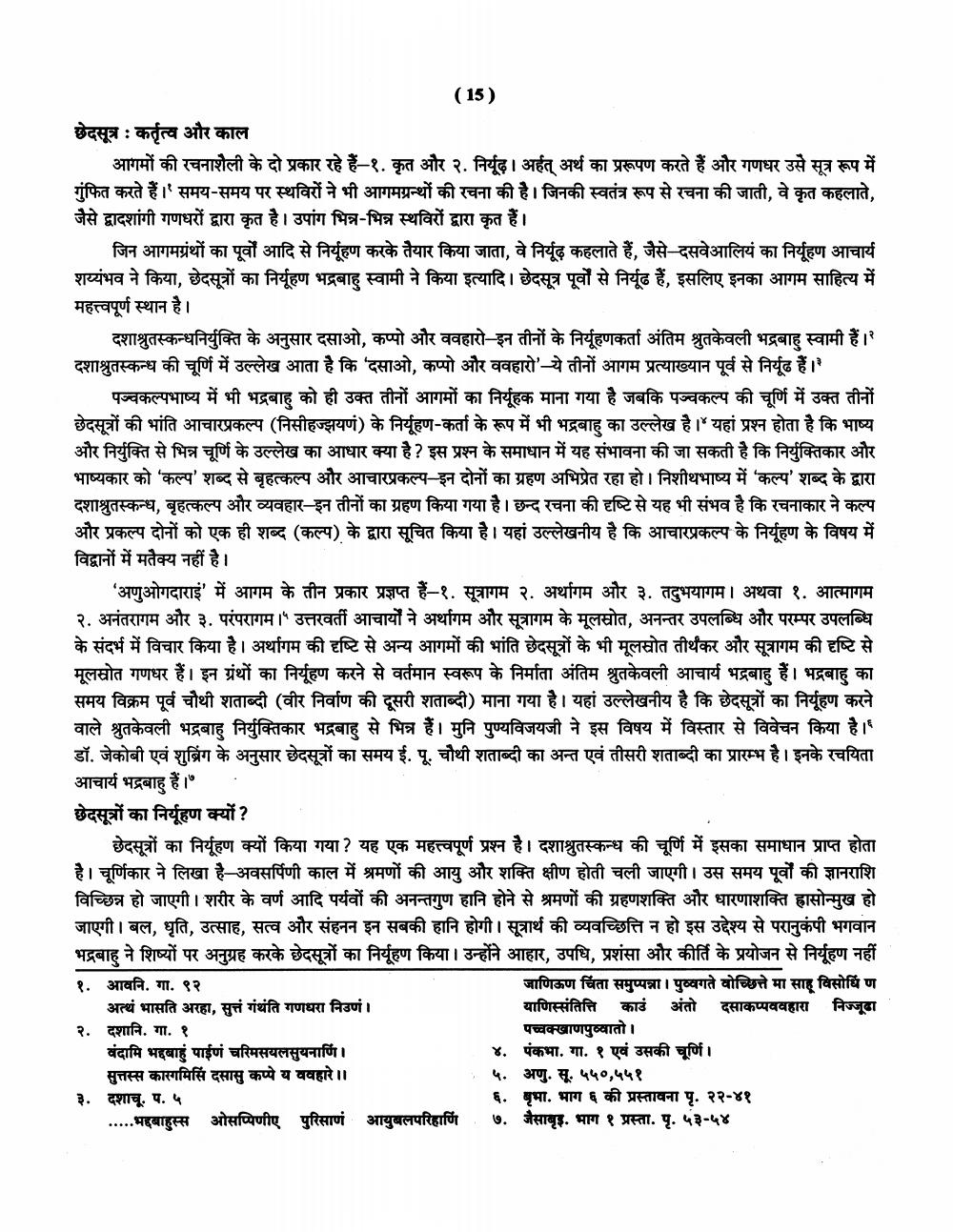________________
(15) छेदसूत्र : कर्तृत्व और काल
आगमों की रचनाशैली के दो प्रकार रहे हैं-१. कृत और २. निर्मूढ़ । अर्हत् अर्थ का प्ररूपण करते हैं और गणधर उसे सूत्र रूप में गुंफित करते हैं। समय-समय पर स्थविरों ने भी आगमग्रन्थों की रचना की है। जिनकी स्वतंत्र रूप से रचना की जाती, वे कृत कहलाते, जैसे द्वादशांगी गणधरों द्वारा कृत है। उपांग भिन्न-भिन्न स्थविरों द्वारा कृत हैं।
जिन आगमग्रंथों का पूर्वो आदि से निर्वृहण करके तैयार किया जाता, वे नियूंढ़ कहलाते हैं, जैसे-दसवेआलियं का नि!हण आचार्य शय्यंभव ने किया, छेदसूत्रों का निर्मूहण भद्रबाहु स्वामी ने किया इत्यादि। छेदसूत्र पूर्वो से नियूंढ हैं, इसलिए इनका आगम साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।
दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति के अनुसार दसाओ, कप्पो और ववहारो-इन तीनों के निर्गृहणकर्ता अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी हैं। दशाश्रुतस्कन्ध की चूर्णि में उल्लेख आता है कि 'दसाओ, कप्पो और ववहारो' ये तीनों आगम प्रत्याख्यान पूर्व से निर्मूढ हैं।'
पञ्चकल्पभाष्य में भी भद्रबाहु को ही उक्त तीनों आगमों का निर्वृहक माना गया है जबकि पञ्चकल्प की चूर्णि में उक्त तीनों छेदसूत्रों की भांति आचारप्रकल्प (निसीहज्झयणं) के नि!हण-कर्ता के रूप में भी भद्रबाहु का उल्लेख है। यहां प्रश्न होता है कि भाष्य
और नियुक्ति से भिन्न चूर्णि के उल्लेख का आधार क्या है? इस प्रश्न के समाधान में यह संभावना की जा सकती है कि नियुक्तिकार और भाष्यकार को 'कल्प' शब्द से बृहत्कल्प और आचारप्रकल्प-इन दोनों का ग्रहण अभिप्रेत रहा हो। निशीथभाष्य में 'कल्प' शब्द के द्वारा दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार-इन तीनों का ग्रहण किया गया है। छन्द रचना की दृष्टि से यह भी संभव है कि रचनाकार ने कल्प
और प्रकल्प दोनों को एक ही शब्द (कल्प) के द्वारा सूचित किया है। यहां उल्लेखनीय है कि आचारप्रकल्प के निर्वृहण के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है।
'अणुओगदाराई' में आगम के तीन प्रकार प्रज्ञप्त हैं-१. सूत्रागम २. अर्थागम और ३. तदुभयागम। अथवा १. आत्मागम २. अनंतरागम और ३. परंपरागम।' उत्तरवर्ती आचार्यों ने अर्थागम और सूत्रागम के मूलस्रोत, अनन्तर उपलब्धि और परम्पर उपलब्धि के संदर्भ में विचार किया है। अर्थागम की दृष्टि से अन्य आगमों की भांति छेदसूत्रों के भी मूलस्रोत तीर्थंकर और सूत्रागम की दृष्टि से मूलस्रोत गणधर हैं। इन ग्रंथों का नि!हण करने से वर्तमान स्वरूप के निर्माता अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु का समय विक्रम पूर्व चौथी शताब्दी (वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी) माना गया है। यहां उल्लेखनीय है कि छेदसूत्रों का नि!हण करने वाले श्रुतकेवली भद्रबाहु नियुक्तिकार भद्रबाहु से भिन्न हैं। मुनि पुण्यविजयजी ने इस विषय में विस्तार से विवेचन किया है। डॉ. जेकोबी एवं शुब्रिग के अनुसार छेदसूत्रों का समय ई. पू. चौथी शताब्दी का अन्त एवं तीसरी शताब्दी का प्रारम्भ है। इनके रचयिता आचार्य भद्रबाहु हैं।' छेदसूत्रों का नि!हण क्यों?
छेदसूत्रों का निर्वृहण क्यों किया गया? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। दशाश्रुतस्कन्ध की चूर्णि में इसका समाधान प्राप्त होता है। चूर्णिकार ने लिखा है-अवसर्पिणी काल में श्रमणों की आयु और शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। उस समय पूर्वो की ज्ञानराशि विच्छिन्न हो जाएगी। शरीर के वर्ण आदि पर्यवों की अनन्तगुण हानि होने से श्रमणों की ग्रहणशक्ति और धारणाशक्ति ह्रासोन्मुख हो जाएगी। बल, धृति, उत्साह, सत्व और संहनन इन सबकी हानि होगी। सूत्रार्थ की व्यवच्छित्ति न हो इस उद्देश्य से परानुकंपी भगवान भद्रबाहु ने शिष्यों पर अनुग्रह करके छेदसूत्रों का निर्वृहण किया। उन्होंने आहार, उपधि, प्रशंसा और कीर्ति के प्रयोजन से नि!हण नहीं १. आवनि. गा. ९२
जाणिऊण चिंता समुप्पन्ना। पुव्वगते वोच्छित्ते मा साहू विसोधि ण अत्थं भासति अरहा, सुत्तं गंथंति गणधरा निउणं।
याणिस्संतित्ति काउं अंतो दसाकप्पववहारा निज्जूढा २. दशानि. गा. १
पच्चक्खाणपुव्यातो। वंदामि भद्दबाहुं पाईणं चरिमसयलसुयनाणि।
४. पंकभा. गा. १ एवं उसकी चूर्णि। सुत्तस्स कारगमिसिं दसासु कप्पे य ववहारे।।
५. अणु. सू. ५५०,५५१ ३. दशाचू. प. ५
६. बृभा. भाग ६ की प्रस्तावना पृ. २२-४१ ......भद्दबाहुस्स ओसप्पिणीए पुरिसाणं आयुबलपरिहाणि । ७. जैसाबृह. भाग १ प्रस्ता. पृ. ५३-५४