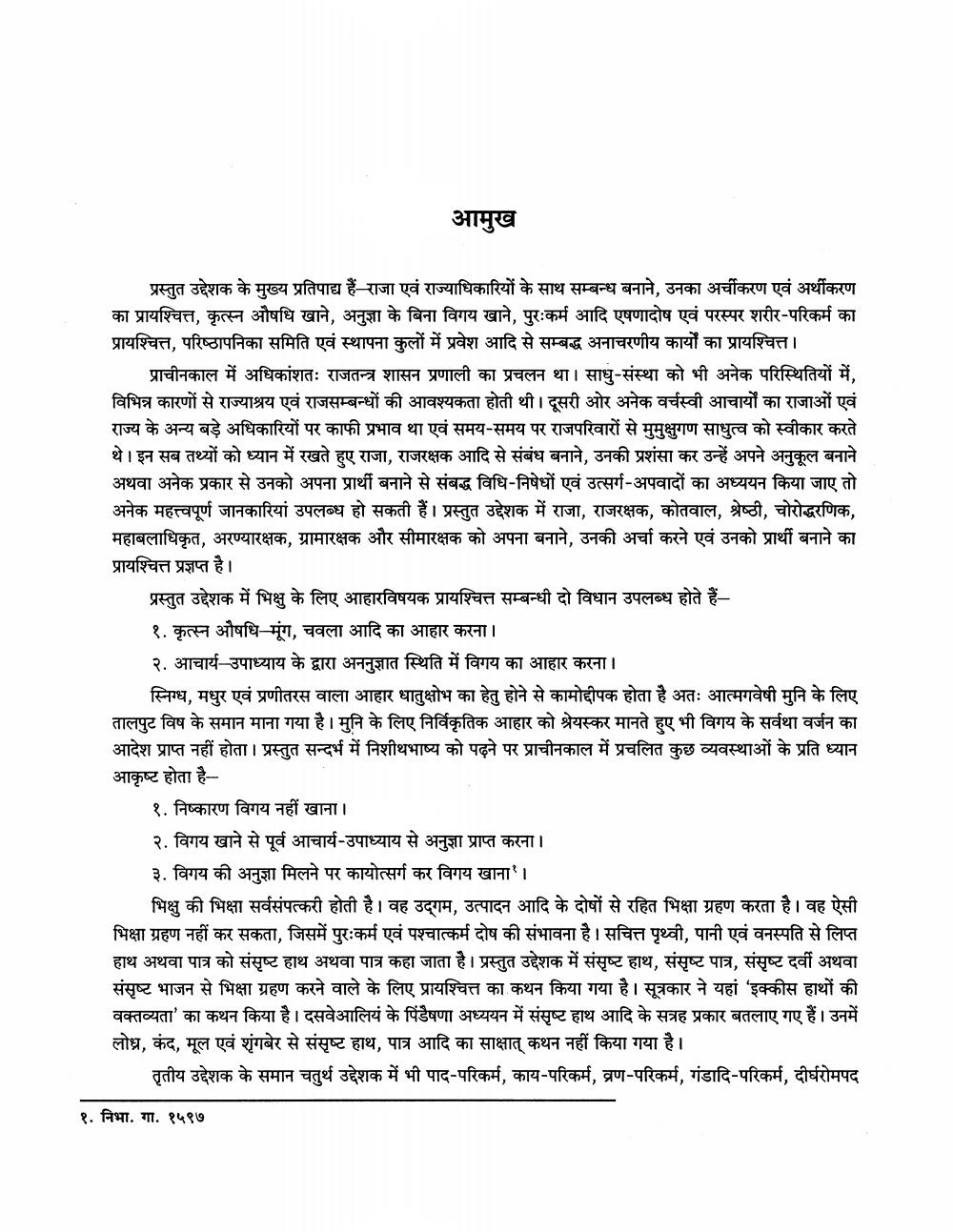________________
आमुख
प्रस्तुत उद्देशक के मुख्य प्रतिपाद्य हैं-राजा एवं राज्याधिकारियों के साथ सम्बन्ध बनाने, उनका अर्चीकरण एवं अर्थीकरण का प्रायश्चित्त, कृत्स्न औषधि खाने, अनुज्ञा के बिना विगय खाने, पुरःकर्म आदि एषणादोष एवं परस्पर शरीर-परिकर्म का प्रायश्चित्त, परिष्ठापनिका समिति एवं स्थापना कुलों में प्रवेश आदि से सम्बद्ध अनाचरणीय कार्यों का प्रायश्चित्त।
प्राचीनकाल में अधिकांशतः राजतन्त्र शासन प्रणाली का प्रचलन था। साधु-संस्था को भी अनेक परिस्थितियों में, विभिन्न कारणों से राज्याश्रय एवं राजसम्बन्धों की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर अनेक वर्चस्वी आचार्यों का राजाओं एवं राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों पर काफी प्रभाव था एवं समय-समय पर राजपरिवारों से मुमुक्षुगण साधुत्व को स्वीकार करते थे। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजा, राजरक्षक आदि से संबंध बनाने, उनकी प्रशंसा कर उन्हें अपने अनुकूल बनाने अथवा अनेक प्रकार से उनको अपना प्रार्थी बनाने से संबद्ध विधि-निषेधों एवं उत्सर्ग-अपवादों का अध्ययन किया जाए तो अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्रस्तुत उद्देशक में राजा, राजरक्षक, कोतवाल, श्रेष्ठी, चोरोद्धरणिक, महाबलाधिकृत, अरण्यारक्षक, ग्रामारक्षक और सीमारक्षक को अपना बनाने, उनकी अर्चा करने एवं उनको प्रार्थी बनाने का प्रायश्चित्त प्रज्ञप्त है।
प्रस्तुत उद्देशक में भिक्षु के लिए आहारविषयक प्रायश्चित्त सम्बन्धी दो विधान उपलब्ध होते हैं१. कृत्स्न औषधि-मूंग, चवला आदि का आहार करना। २. आचार्य-उपाध्याय के द्वारा अननुज्ञात स्थिति में विगय का आहार करना।
स्निग्ध, मधुर एवं प्रणीतरस वाला आहार धातुक्षोभ का हेतु होने से कामोद्दीपक होता है अतः आत्मगवेषी मुनि के लिए तालपुट विष के समान माना गया है। मुनि के लिए निर्विकृतिक आहार को श्रेयस्कर मानते हुए भी विगय के सर्वथा वर्जन का आदेश प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत सन्दर्भ में निशीथभाष्य को पढ़ने पर प्राचीनकाल में प्रचलित कुछ व्यवस्थाओं के प्रति ध्यान आकृष्ट होता है
१. निष्कारण विगय नहीं खाना। २. विगय खाने से पूर्व आचार्य-उपाध्याय से अनुज्ञा प्राप्त करना । ३. विगय की अनुज्ञा मिलने पर कायोत्सर्ग कर विगय खाना।
भिक्षु की भिक्षा सर्वसंपत्करी होती है। वह उद्गम, उत्पादन आदि के दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण करता है। वह ऐसी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, जिसमें पुरःकर्म एवं पश्चात्कर्म दोष की संभावना है। सचित्त पृथ्वी, पानी एवं वनस्पति से लिप्त हाथ अथवा पात्र को संसृष्ट हाथ अथवा पात्र कहा जाता है। प्रस्तुत उद्देशक में संसृष्ट हाथ, संसृष्ट पात्र, संसृष्ट दर्वी अथवा संसृष्ट भाजन से भिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का कथन किया गया है। सूत्रकार ने यहां 'इक्कीस हाथों की वक्तव्यता' का कथन किया है। दसवेआलियं के पिंडैषणा अध्ययन में संसृष्ट हाथ आदि के सत्रह प्रकार बतलाए गए हैं। उनमें लोध्र, कंद, मूल एवं शृंगबेर से संसृष्ट हाथ, पात्र आदि का साक्षात् कथन नहीं किया गया है। __ तृतीय उद्देशक के समान चतुर्थ उद्देशक में भी पाद-परिकर्म, काय-परिकर्म, व्रण-परिकर्म, गंडादि-परिकर्म, दीर्घरोमपद
१. निभा. गा. १५९७