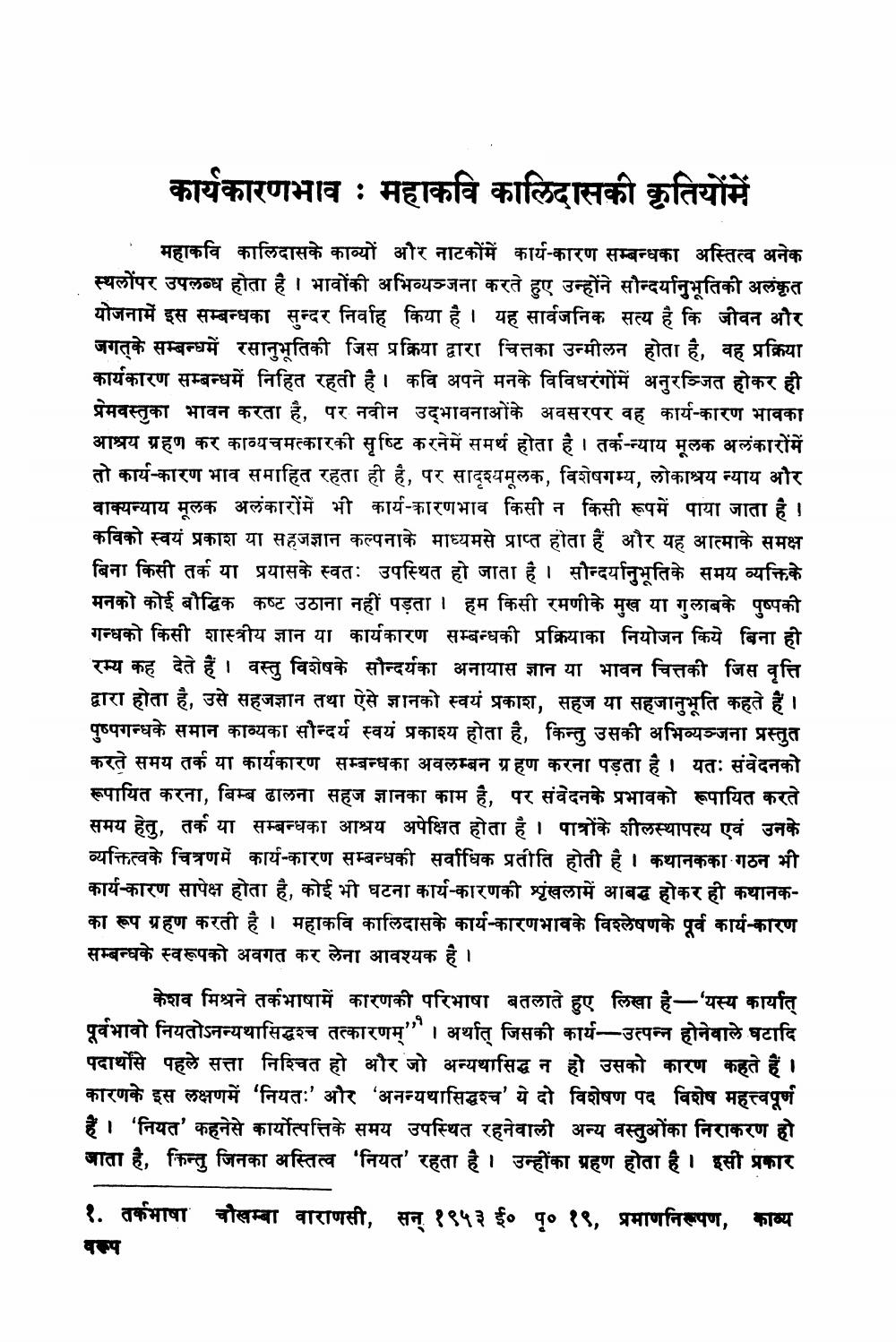________________
कार्यकारणभाव : महाकवि कालिदासकी कृतियोंमें
महाकवि कालिदासके काव्यों और नाटकोंमें कार्य-कारण सम्बन्धका अस्तित्व अनेक स्थलोंपर उपलब्ध होता है । भावोंकी अभिव्यञ्जना करते हुए उन्होंने सौन्दर्यानुभूतिकी अलंकृत योजनामें इस सम्बन्धका सुन्दर निर्वाह किया है । यह सार्वजनिक सत्य है कि जीवन और जगत्के सम्बन्धमें रसानुभूतिकी जिस प्रक्रिया द्वारा चित्तका उन्मीलन होता है, वह प्रक्रिया कार्यकारण सम्बन्धमें निहित रहती है । कवि अपने मनके विविधरंगोंमें अनुरञ्जित होकर ही प्रेमवस्तुका भावन करता है, पर नवीन उद्भावनाओंके अवसरपर वह कार्य-कारण भावका आश्रय ग्रहण कर काव्यचमत्कार की सृष्टि करने में समर्थ होता है। तर्क- न्याय मूलक अलंकारोंमें तो कार्यकारण भाव समाहित रहता ही है, पर सादृश्यमूलक, विशेषगम्य, लोकाश्रय न्याय और वाक्यन्याय मूलक अलंकारों में भी कार्य कारणभाव किसी न किसी रूप में पाया जाता है । कविको स्वयं प्रकाश या सहजज्ञान कल्पनाके माध्यमसे प्राप्त होता हैं और यह आत्माके समक्ष बिना किसी तर्क या प्रयासके स्वतः उपस्थित हो जाता है । सौन्दर्यानुभूति के समय व्यक्ति के मनको कोई बौद्धिक कष्ट उठाना नहीं पड़ता । हम किसी रमणीके मुख या गुलाबके पुष्पकी गन्धको किसी शास्त्रीय ज्ञान या कार्यकारण सम्बन्धकी प्रक्रियाका नियोजन किये बिना ही रम्य कह देते हैं । वस्तु विशेषके सौन्दर्यका अनायास ज्ञान या भावन चित्तकी जिस वृत्ति द्वारा होता है, उसे सहजज्ञान तथा ऐसे ज्ञानको स्वयं प्रकाश, सहज या सहजानुभूति कहते हैं । पुष्पगन्धके समान काव्यका सौन्दर्य स्वयं प्रकाश्य होता है, किन्तु उसकी अभिव्यञ्जना प्रस्तुत करते समय तर्क या कार्यकारण सम्बन्धका अवलम्बन ग्रहण करना पड़ता है । यतः संवेदनको रूपायित करना, बिम्ब ढालना सहज ज्ञानका काम है, पर संवेदनके प्रभावको रूपायित करते समय हेतु, तर्क या सम्बन्धका आश्रय अपेक्षित होता है । पात्रोंके शीलस्थापत्य एवं उनके व्यक्तित्वके चित्रण में कार्य-कारण सम्बन्धकी सर्वाधिक प्रतीति होती है । कथानकका गठन भी कार्य-कारण सापेक्ष होता है, कोई भी घटना कार्य-कारणकी श्रृंखलामें आबद्ध होकर ही कथानकका रूप ग्रहण करती है । महाकवि कालिदासके कार्य कारणभाव के विश्लेषणके पूर्व कार्य-कारण सम्बन्धके स्वरूपको अवगत कर लेना आवश्यक है ।
केशव मिश्रने तर्कभाषामें कारणकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा है - 'यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत्कारणम्"" । अर्थात् जिसकी कार्य — उत्पन्न होनेवाले घटादि पदार्थोंसे पहले सत्ता निश्चित हो और जो अन्यथासिद्ध न हो उसको कारण कहते हैं । कारण इस लक्षणमें 'नियत' और 'अनन्यथासिद्धश्च' ये दो विशेषण पद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 'नियत' कहनेसे कार्योत्पत्ति के समय उपस्थित रहनेवाली अन्य वस्तुओंका निराकरण हो जाता है, किन्तु जिनका अस्तित्व 'नियत' रहता है। उन्होंका ग्रहण होता है । इसी प्रकार
१. तर्कभाषा चौखम्बा वाराणसी, सन् १९५३ ई० पू० १९, प्रमाणनिरूपण, काव्य
वरूप