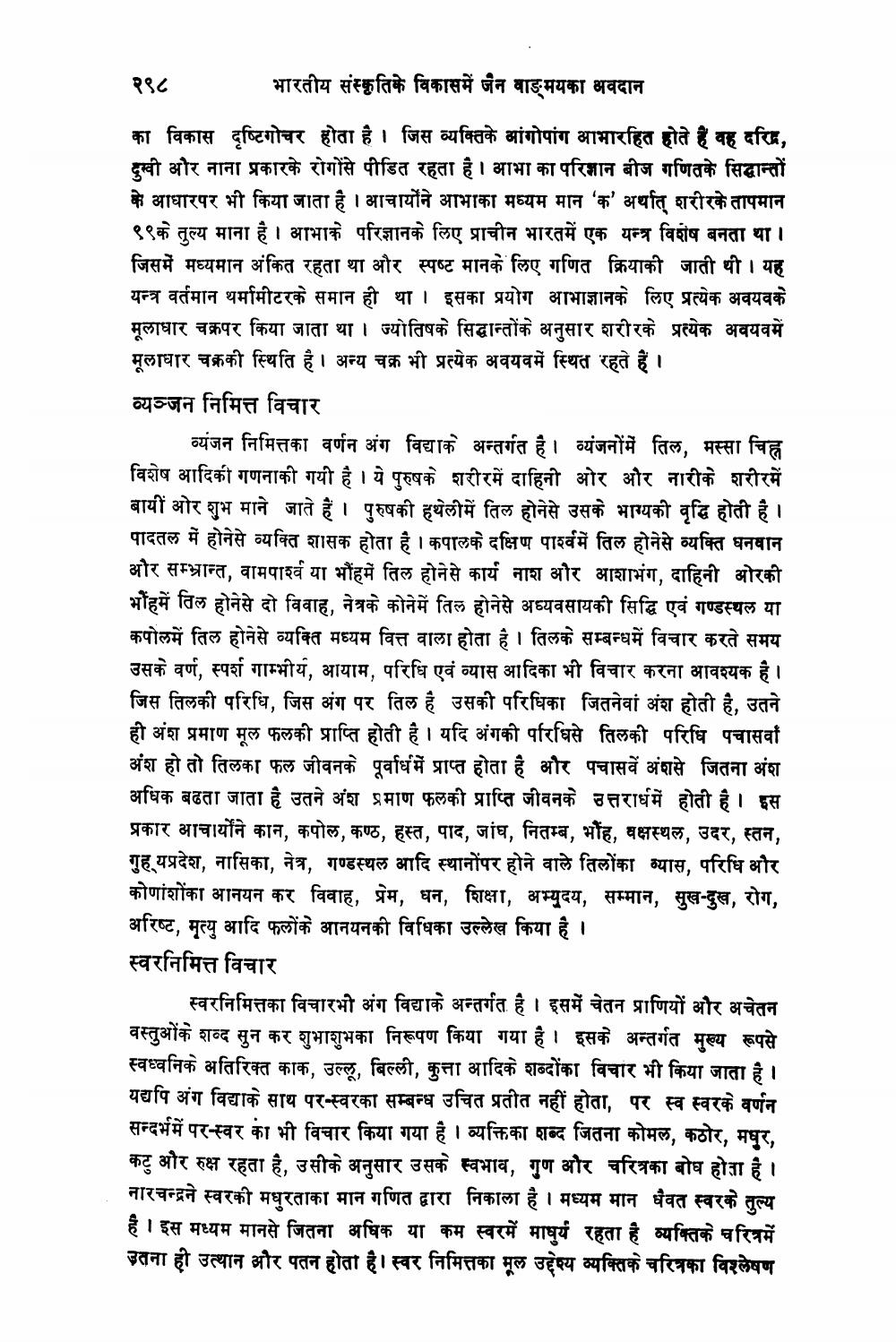________________
२९८
भारतीय संस्कृतिक विकासमें जैन वाङ्मयका अवदान
का विकास दृष्टिगोचर होता है । जिस व्यक्तिके आंगोपांग आभारहित होते हैं वह दरिद्र, दुखी और नाना प्रकारके रोगोंसे पीडित रहता है । आभा का परिज्ञान बीज गणितके सिद्धान्तों के आधारपर भी किया जाता है । आचार्योंने आभाका मध्यम मान 'क' अर्थात् शरीर के तापमान ९९ के तुल्य माना है । आभा के परिज्ञानके लिए प्राचीन भारतमें एक यन्त्र विशेष बनता था । जिसमें मध्यमान अंकित रहता था और स्पष्ट मानके लिए गणित क्रियाकी जाती थी । यह यन्त्र वर्तमान थर्मामीटरके समान ही था । इसका प्रयोग आभाज्ञानके लिए प्रत्येक अवयवके मूलाधार चक्रपर किया जाता था । ज्योतिष के सिद्धान्तोंके अनुसार शरीरके प्रत्येक अवयव में मूलाधार चक्रकी स्थिति है । अन्य चक्र भी प्रत्येक अवयव में स्थित रहते हैं ।
व्यञ्जन निमित्त विचार
व्यंजन निमित्तका वर्णन अंग विद्याके अन्तर्गत है । व्यंजनों में तिल, मस्सा चिह्न विशेष आदिकी गणना की गयी है । ये पुरुषके शरीर में दाहिनी ओर और नारीके शरीर में बायीं ओर शुभ माने जाते हैं । पुरुषकी हथेली में तिल होनेसे उसके भाग्य की वृद्धि होती है । पादतल में होनेसे व्यक्ति शासक होता है । कपालके दक्षिण पार्श्व में तिल होने से व्यक्ति धनवान और सम्भ्रान्त वामपार्श्व या भौंह में तिल होने से कार्य नाश और आशाभंग, दाहिनी ओरकी
हमें तिल होने से दो विवाह, नेत्रके कोने में तिल होनेसे अध्यवसाय की सिद्धि एवं गण्डस्थल या कपोल में तिल होने से व्यक्ति मध्यम वित्त वाला होता है । तिलके सम्बन्ध में विचार करते समय उसके वर्ण, स्पर्श गाम्भीर्य, आयाम, परिधि एवं व्यास आदिका भी विचार करना आवश्यक है । जिस तिलकी परिधि, जिस अंग पर तिल है उसकी परिधिका जितनेवां अंश होती है, उतने ही अंश प्रमाण मूल फलकी प्राप्ति होती है । यदि अंगको परिधिसे तिलकी परिधि पचासव अंश हो तो तिलका फल जीवनके पूर्वार्ध में प्राप्त होता है और पचासवें अंशसे जितना अंश अधिक बढता जाता है उतने अंश प्रमाण फलकी प्राप्ति जीवनके उत्तरार्ध में होती है । इस प्रकार आचार्योंने कान, कपोल, कण्ठ, हस्त, पाद, जांघ, नितम्ब, भौंह, वक्षस्थल, उदर, स्तन, गुह, यप्रदेश, नासिका, नेत्र, गण्डस्थल आदि स्थानोंपर होने वाले तिलोंका व्यास, परिधि और कोणांशोंका आनयन कर विवाह, प्रेम, धन, शिक्षा, अभ्युदय, सम्मान, सुख-दुख, रोग, अरिष्ट, मृत्यु आदि फलों के आनयनकी विधिका उल्लेख किया है ।
स्वरनिमित्त विचार
स्वरनिमित्तका विचारभी अंग विद्याके अन्तर्गत है । इसमें चेतन प्राणियों और अचेतन वस्तुओं के शब्द सुन कर शुभाशुभका निरूपण किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूपसे स्वध्वनिके अतिरिक्त काक, उल्लू, बिल्ली, कुत्ता आदिके शब्दोंका विचार भी किया जाता है । यद्यपि अंग विद्याके साथ पर-स्वरका सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता, पर स्व स्वरके वर्णन सन्दर्भ में पर-स्वर का भी विचार किया गया है । व्यक्तिका शब्द जितना कोमल, कठोर, मधुर, कटु और रुक्ष रहता है, उसीके अनुसार उसके स्वभाव, गुण और चरित्रका बोध होता है । नारचन्द्रने स्वरकी मधुरताका मान गणित द्वारा निकाला है । मध्यम मान धैवत स्वरके तुल्य है । इस मध्यम मानसे जितना अधिक या कम स्वरमें माधुर्यं रहता है व्यक्तिके चरित्रमें उतना ही उत्थान और पतन होता है। स्वर निमित्तका मूल उद्देश्य व्यक्तिके चरित्रका विश्लेषण