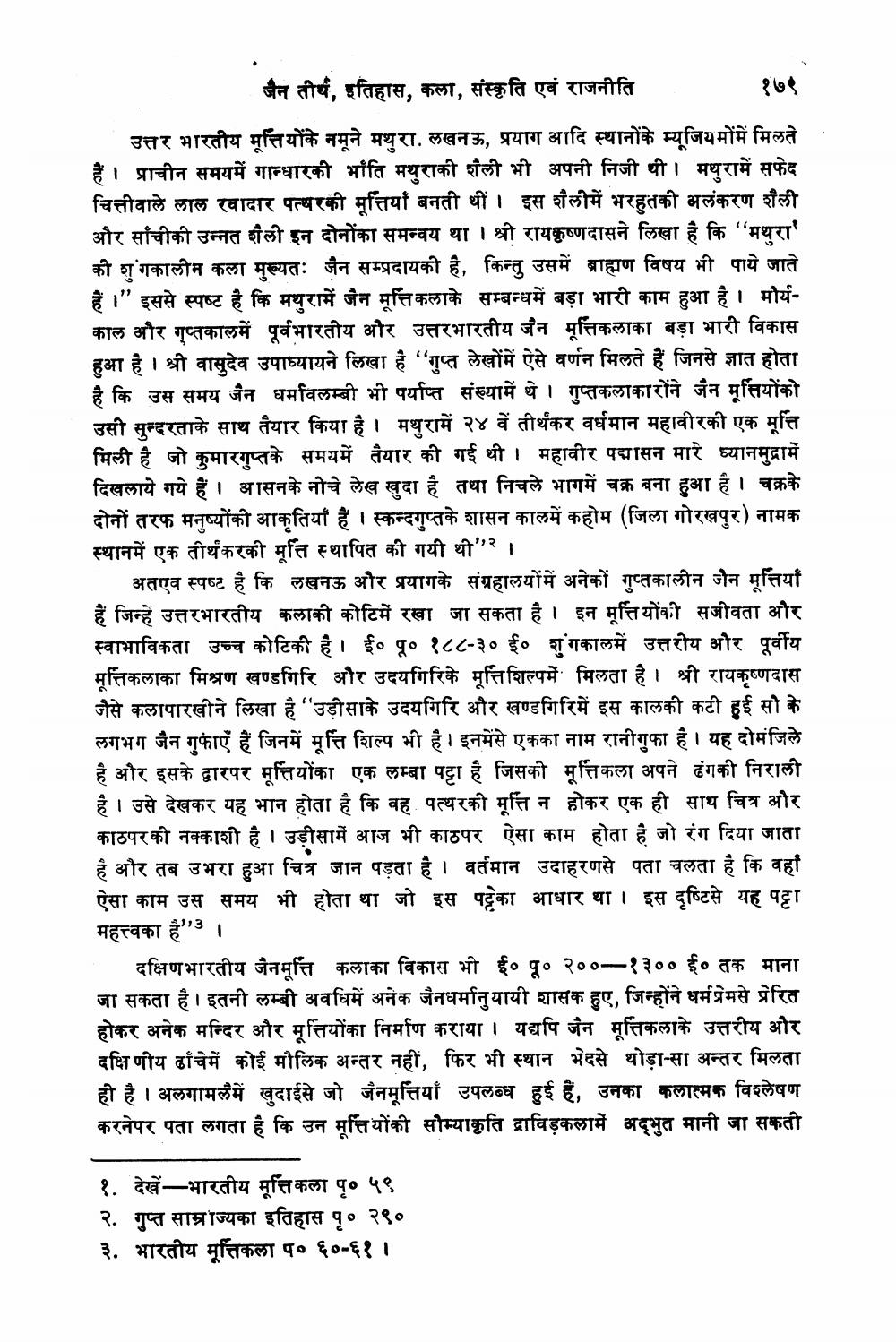________________
जैन तीर्थ, इतिहास, कला, संस्कृति एवं राजनीति
१७९ उत्तर भारतीय मूत्तियोंके नमूने मथुरा. लखनऊ, प्रयाग आदि स्थानोंके म्यूजियमोंमें मिलते हैं। प्राचीन समयमें गान्धारकी भाँति मथुराकी शैली भी अपनी निजी थी। मथुरामें सफेद चित्तीवाले लाल रवादार पत्थरकी मूत्तियाँ बनती थीं। इस शैलीमें भरहुतकी अलंकरण शैली और साँचीकी उन्नत शैली इन दोनोंका समन्वय था । श्री रायकृष्णदासने लिखा है कि "मथुरा' की शुगकालीन कला मुख्यतः जैन सम्प्रदायको है, किन्तु उसमें ब्राह्मण विषय भी पाये जाते हैं।" इससे स्पष्ट है कि मथुरामें जैन मूर्तिकलाके सम्बन्धमें बड़ा भारी काम हुआ है । मौर्यकाल और गुप्तकालमें पूर्वभारतीय और उत्तरभारतीय जैन मूर्तिकलाका बड़ा भारी विकास हुआ है । श्री वासुदेव उपाध्यायने लिखा है "गुप्त लेखोंमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय जैन धर्मावलम्बी भी पर्याप्त संख्यामें थे । गुप्तकलाकारोंने जैन मूर्तियोंको उसी सुन्दरताके साथ तैयार किया है । मथुरामें २४ वें तीर्थंकर वर्धमान महावीरकी एक मूत्ति मिली है जो कुमारगुप्तके समयमें तैयार की गई थी। महावीर पद्मासन मारे ध्यानमुद्रामें दिखलाये गये हैं। आसनके नीचे लेख खुदा है तथा निचले भागमें चक्र बना हुआ है । चक्रके दोनों तरफ मनुष्योंकी आकृतियाँ हैं । स्कन्दगुप्तके शासन कालमें कहोम (जिला गोरखपुर) नामक स्थानमें एक तीर्थंकरकी मूत्ति स्थापित की गयी थी"२ । ___ अतएव स्पष्ट है कि लखनऊ और प्रयागके संग्रहालयोंमें अनेकों गुप्तकालीन जैन मूत्तियाँ हैं जिन्हें उत्तरभारतीय कलाकी कोटिमें रखा जा सकता है। इन मूत्तियोंकी सजीवता और स्वाभाविकता उच्च कोटिकी है। ई० पू० १८८-३० ई० शुगकालमें उत्तरीय और पूर्वीय मूर्तिकलाका मिश्रण खण्डगिरि और उदयगिरिके मूतिशिल्पमें मिलता है। श्री रायकृष्णदास जैसे कलापारखीने लिखा है "उड़ीसाके उदयगिरि और खण्डगिरिमें इस कालकी कटी हुई सौ के लगभग जैन गुफाएँ हैं जिनमें मूत्ति शिल्प भी है। इनमेंसे एकका नाम रानीगुफा है। यह दोमंजिले है और इसके द्वारपर मूत्तियोंका एक लम्बा पट्टा है जिसकी मूर्तिकला अपने ढंगकी निराली है । उसे देखकर यह भान होता है कि वह पत्थरकी मूत्ति न होकर एक ही साथ चित्र और काठपरको नक्काशी है । उड़ीसामें आज भी काठपर ऐसा काम होता है जो रंग दिया जाता है और तब उभरा हुआ चित्र जान पड़ता है। वर्तमान उदाहरणसे पता चलता है कि वहाँ ऐसा काम उस समय भी होता था जो इस पट्टेका आधार था। इस दृष्टिसे यह पट्टा महत्त्वका है" ।
दक्षिणभारतीय जैनमूत्ति कलाका विकास भी ई० पू० २००-१३०० ई० तक माना जा सकता है। इतनी लम्बी अवधिमें अनेक जैनधर्मानुयायी शासक हुए, जिन्होंने धर्मप्रेमसे प्रेरित होकर अनेक मन्दिर और मूत्तियोंका निर्माण कराया। यद्यपि जैन मूर्तिकलाके उत्तरीय और दक्षिणीय ढाँचेमें कोई मौलिक अन्तर नहीं, फिर भी स्थान भेदसे थोड़ा-सा अन्तर मिलता ही है । अलगामलमें खुदाईसे जो जैनमूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनका कलात्मक विश्लेषण करनेपर पता लगता है कि उन मूत्तियोंकी सौम्याकृति द्राविड़कलामें अद्भुत मानी जा सकती
१. देखें भारतीय मूत्तिकला पृ० ५९ २. गुप्त साम्राज्यका इतिहास पृ० २९० ३. भारतीय मूर्तिकला प० ६०-६१ ।