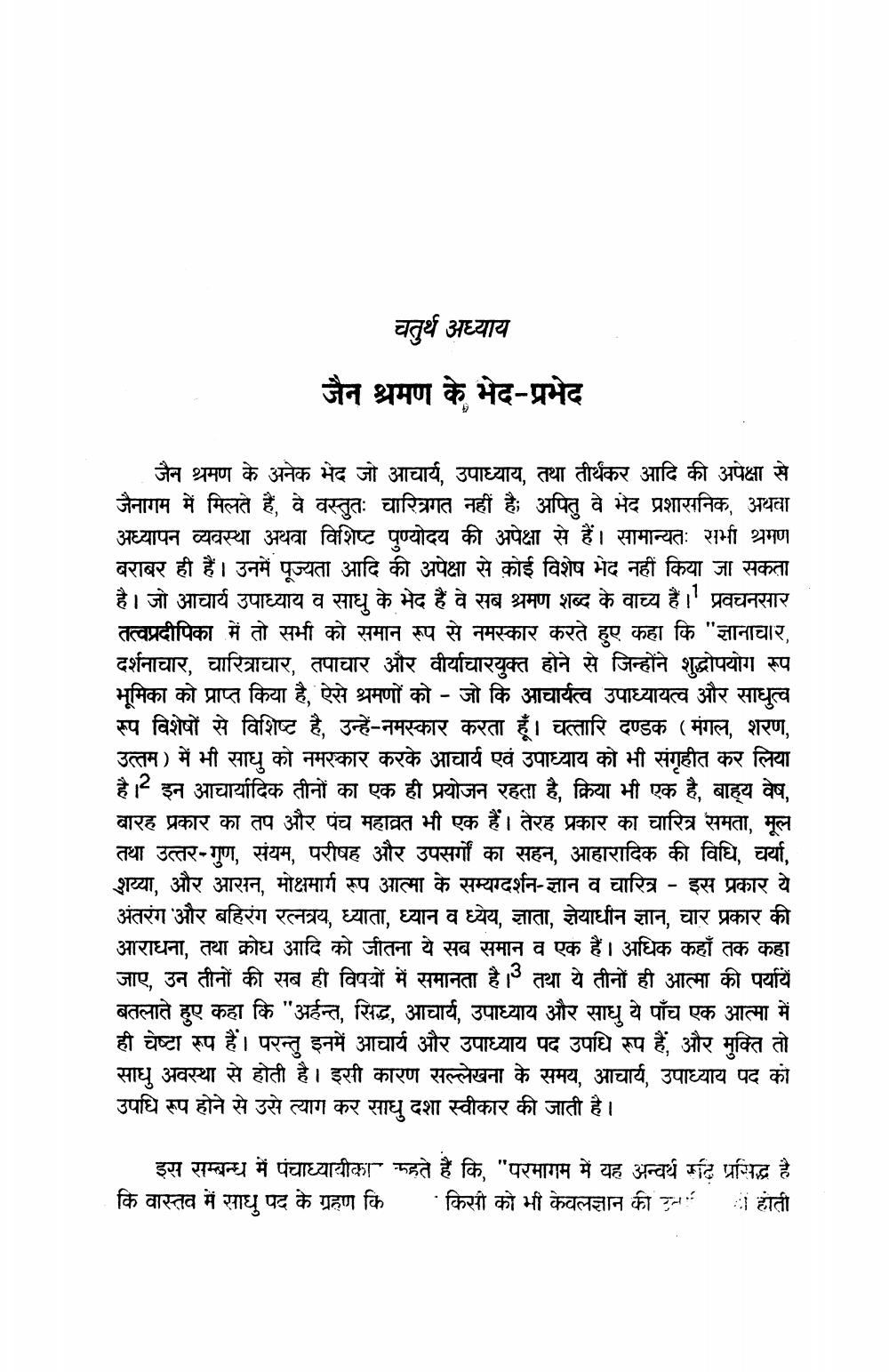________________
चतुर्थ अध्याय जैन श्रमण के भेद-प्रभेद
जैन श्रमण के अनेक भेद जो आचार्य, उपाध्याय, तथा तीर्थंकर आदि की अपेक्षा से जैनागम में मिलते हैं, वे वस्तुतः चारित्रगत नहीं है; अपितु वे भेद प्रशासनिक, अथवा अध्यापन व्यवस्था अथवा विशिष्ट पुण्योदय की अपेक्षा से हैं। सामान्यतः सभी श्रमण बराबर ही हैं। उनमें पूज्यता आदि की अपेक्षा से कोई विशेष भेद नहीं किया जा सकता है। जो आचार्य उपाध्याय व साधु के भेद हैं वे सब श्रमण शब्द के वाच्य हैं।' प्रवचनसार तत्वप्रदीपिका में तो सभी को समान रूप से नमस्कार करते हुए कहा कि "ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारयुक्त होने से जिन्होंने शुद्धोपयोग रूप भूमिका को प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणों को - जो कि आचार्यत्व उपाध्यायत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट है, उन्हें-नमस्कार करता हूँ। चत्तारि दण्डक (मंगल, शरण, उत्तम ) में भी साधु को नमस्कार करके आचार्य एवं उपाध्याय को भी संगृहीत कर लिया है। इन आचार्यादिक तीनों का एक ही प्रयोजन रहता है, क्रिया भी एक है, बाह्य वेष, बारह प्रकार का तप और पंच महाव्रत भी एक हैं। तेरह प्रकार का चारित्र समता, मूल तथा उत्तर-गुण, संयम, परीषह और उपसर्गों का सहन, आहारादिक की विधि, चर्या, शय्या, और आसन, मोक्षमार्ग रूप आत्मा के सम्यग्दर्शन-ज्ञान व चारित्र - इस प्रकार ये अंतरंग और बहिरंग रत्नत्रय, ध्याता, ध्यान व ध्येय, ज्ञाता, ज्ञेयाधीन ज्ञान, चार प्रकार की आराधना, तथा क्रोध आदि को जीतना ये सब समान व एक हैं। अधिक कहाँ तक कहा जाए, उन तीनों की सब ही विषयों में समानता है। तथा ये तीनों ही आत्मा की पर्यायें बतलाते हुए कहा कि "अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँच एक आत्मा में ही चेष्टा रूप हैं। परन्तु इनमें आचार्य और उपाध्याय पद उपधि रूप हैं, और मुक्ति तो साधु अवस्था से होती है। इसी कारण सल्लेखना के समय, आचार्य, उपाध्याय पद को उपधि रूप होने से उसे त्याग कर साधु दशा स्वीकार की जाती है।
इस सम्बन्ध में पंचाध्यायीका कहते हैं कि, "परमागम में यह अन्वर्थ मंद प्रसिद्ध है कि वास्तव में साधु पद के ग्रहण कि किसी को भी केवलज्ञान की उता होती