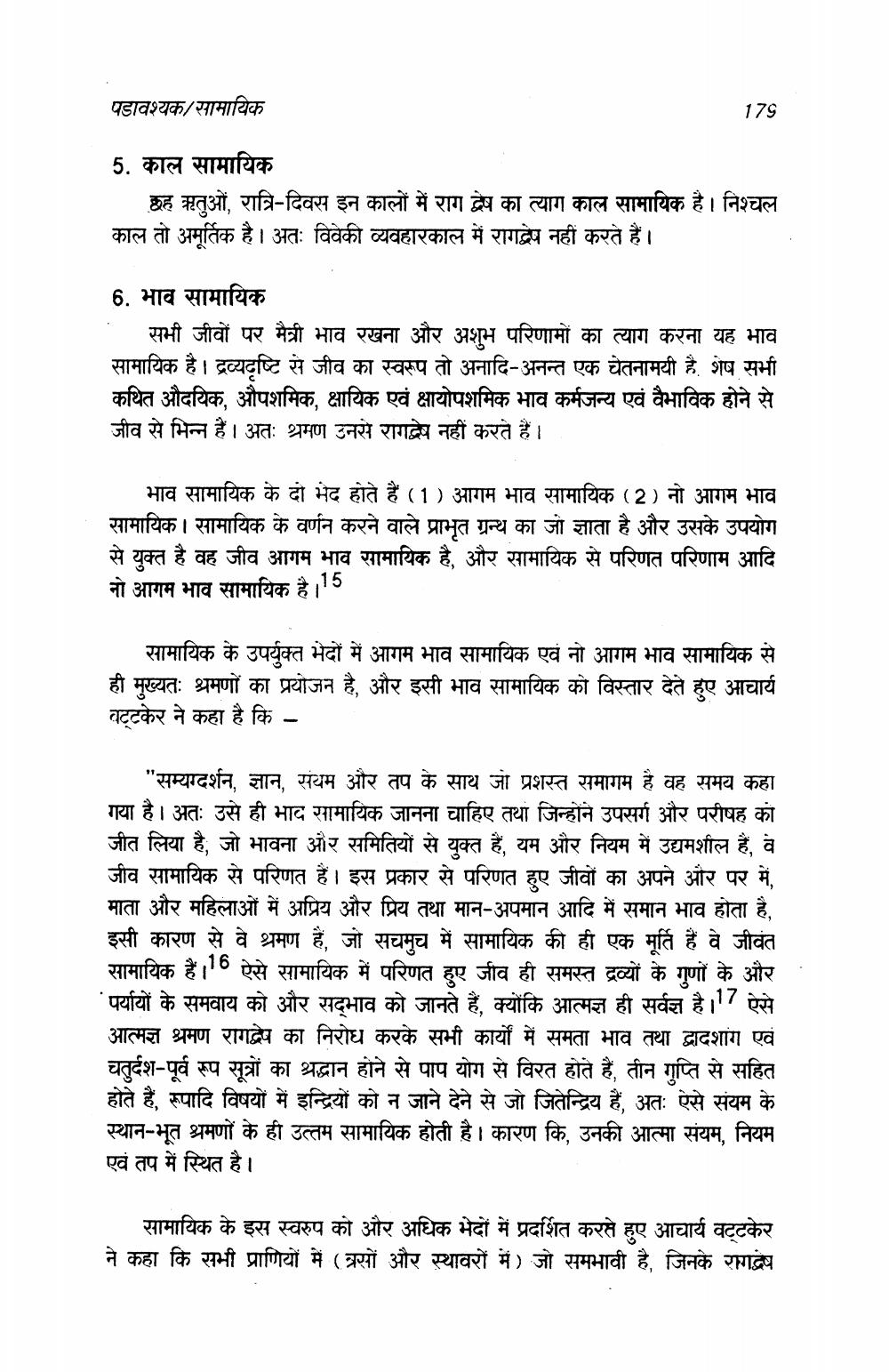________________
पडावश्यक/सामायिक
179
5. काल सामायिक
छह ऋतुओं, रात्रि-दिवस इन कालों में राग द्वेष का त्याग काल सामायिक है। निश्चल काल तो अमूर्तिक है। अतः विवेकी व्यवहारकाल में रागद्वेप नहीं करते हैं।
6. भाव सामायिक
सभी जीवों पर मैत्री भाव रखना और अशुभ परिणामों का त्याग करना यह भाव सामायिक है। द्रव्यदृष्टि से जीव का स्वरूप तो अनादि-अनन्त एक चेतनामयी है. शेष सभी कथित औदयिक, औपशमिक, क्षायिक एवं क्षायोपशमिक भाव कर्मजन्य एवं वैभाविक होने से जीव से भिन्न हैं। अतः श्रमण उनसे रागद्वेष नहीं करते हैं।
भाव सामायिक के दो भेद होते हैं (1) आगम भाव सामायिक (2) नो आगम भाव सामायिक । सामायिक के वर्णन करने वाले प्राभृत ग्रन्थ का जो ज्ञाता है और उसके उपयोग से युक्त है वह जीव आगम भाव सामायिक है, और सामायिक से परिणत परिणाम आदि नो आगम भाव सामायिक है।15
सामायिक के उपर्युक्त भेदों में आगम भाव सामायिक एवं नो आगम भाव सामायिक से ही मुख्यतः श्रमणों का प्रयोजन है, और इसी भाव सामायिक को विस्तार देते हुए आचार्य वट्टकेर ने कहा है कि -
"सम्यग्दर्शन, ज्ञान, संयम और तप के साथ जो प्रशस्त समागम है वह समय कहा गया है। अतः उसे ही भाद सामायिक जानना चाहिए तथा जिन्होंने उपसर्ग और परीषह को जीत लिया है, जो भावना और समितियों से युक्त हैं, यम और नियम में उद्यमशील हैं, वे जीव सामायिक से परिणत हैं। इस प्रकार से परिणत हुए जीवों का अपने और पर में, माता और महिलाओं में अप्रिय और प्रिय तथा मान-अपमान आदि में समान भाव होता है, इसी कारण से वे श्रमण हैं, जो सचमुच में सामायिक की ही एक मूर्ति हैं वे जीवंत सामायिक हैं।16 ऐसे सामायिक में परिणत हुए जीव ही समस्त द्रव्यों के गुणों के और पर्यायों के समवाय को और सद्भाव को जानते हैं, क्योंकि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है। ऐसे आत्मज्ञ श्रमण रागद्वेष का निरोध करके सभी कार्यों में समता भाव तथा द्वादशांग एवं चतुर्दश-पूर्व रूप सूत्रों का श्रद्धान होने से पाप योग से विरत होते हैं, तीन गुप्ति से सहित होते हैं, रूपादि विषयों में इन्द्रियों को न जाने देने से जो जितेन्द्रिय हैं, अतः ऐसे संयम के स्थान-भूत श्रमणों के ही उत्तम सामायिक होती है। कारण कि, उनकी आत्मा संयम, नियम एवं तप में स्थित है।
सामायिक के इस स्वरुप को और अधिक भेदों में प्रदर्शित करते हुए आचार्य वट्टकेर ने कहा कि सभी प्राणियों में (सों और स्थावरों में ) जो समभावी है, जिनके रागद्रय