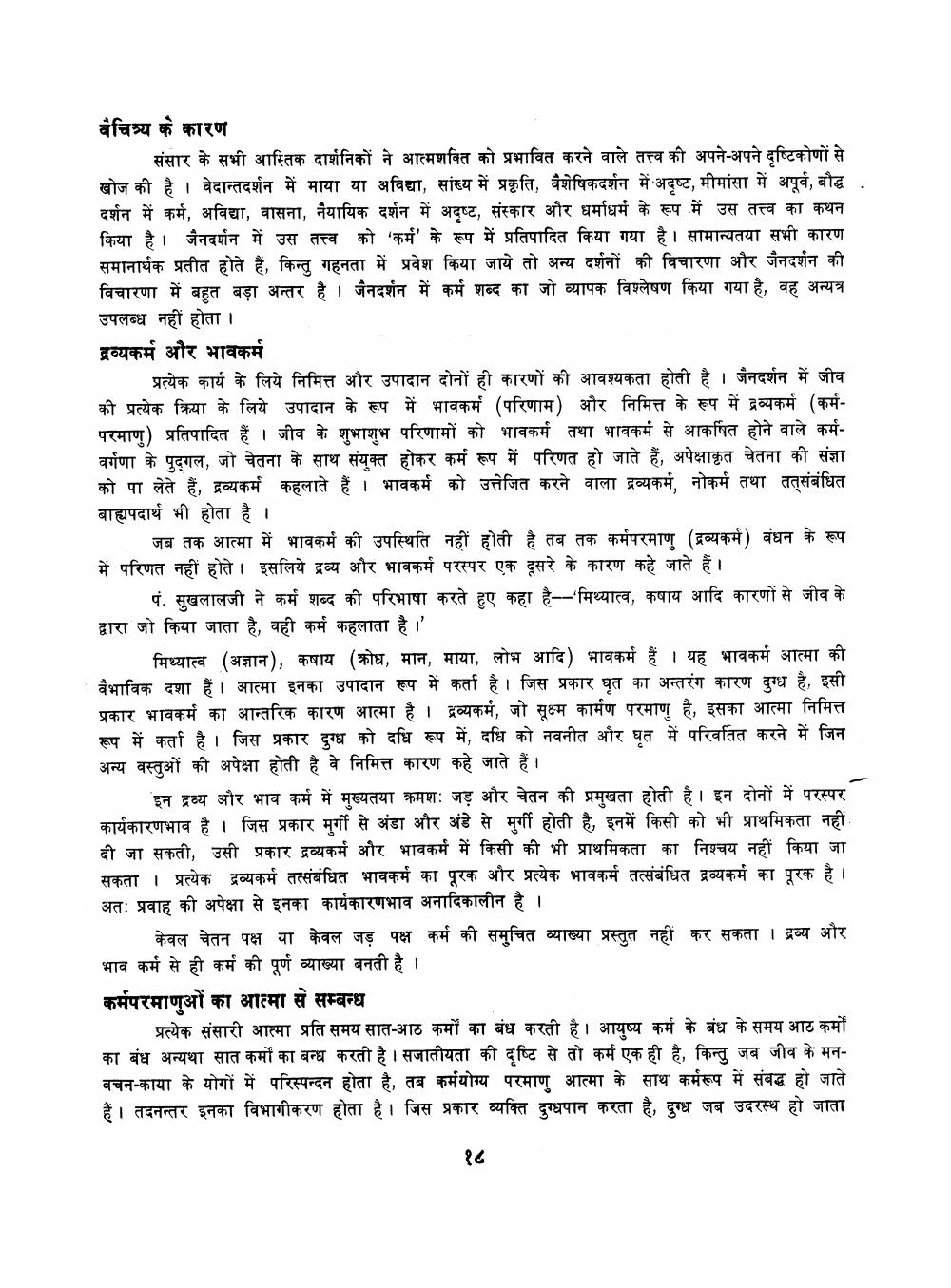________________
वैचित्र्य के कारण
संसार के सभी आस्तिक दार्शनिकों ने आत्मशक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व की अपने-अपने दृष्टिकोणों से खोज की है । वेदान्तदर्शन में माया या अविद्या, सांख्य में प्रकृति, वैशेषिकदर्शन में अदृष्ट, मीमांसा में अपूर्व, बौद्ध दर्शन में कर्म, अविद्या, वासना, नैयायिक दर्शन में अदृष्ट, संस्कार और धर्माधर्म के रूप में उस तत्त्व का कथन किया है। जैनदर्शन में उस तत्व को 'कर्म' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। सामान्यतया सभी कारण समानार्थक प्रतीत होते हैं, किन्तु गहनता में प्रवेश किया जाये तो अन्य दर्शनों की विचारणा और जैनदर्शन की विचारणा में बहुत बड़ा अन्तर है । जैनदर्शन में कर्म शब्द का जो व्यापक विश्लेषण किया गया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता ।
द्रव्यकर्म और भावकर्म
प्रत्येक कार्य के लिये निमित्त और उपादान दोनों ही कारणों की आवश्यकता होती है । जैनदर्शन में जीव की प्रत्येक क्रिया के लिये उपादान के रूप में भावकर्म (परिणाम) और निमित्त के रूप में द्रव्यकर्म (कर्मपरमाणु) प्रतिपादित हैं। जीव के शुभाशुभ परिणामों को भावकर्म तथा भावकर्म से आकर्षित होने वाले कर्मवर्गणा के पुद्गल, जो चेतना के साथ संयुक्त होकर कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं, अपेक्षाकृत चेतना की संज्ञा को पा लेते हैं, द्रव्यकर्म कहलाते हैं। भावकर्म को उत्तेजित करने वाला द्रव्यकर्म, नोकर्म तथा तत्संबंधित बाह्यपदार्थ भी होता है ।
जब तक आत्मा में भावकर्म की उपस्थिति नहीं होती है तब तक कर्मपरमाणु ( द्रव्यकर्म) बंधन के रूप में परिणत नहीं होते। इसलिये द्रव्य और भावकर्म परस्पर एक दूसरे के कारण कहे जाते हैं।
पं. सुखलालजी ने कर्म शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है -- ' मिथ्यात्व कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है, वही कर्म कहलाता है।'
1
मिथ्यात्व ( अज्ञान), कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोभ आदि) भावकर्म हैं। यह भावकर्म आत्मा की वैभाविक दशा हैं । आत्मा इनका उपादान रूप में कर्ता है। जिस प्रकार घृत का अन्तरंग कारण दुग्ध है, इसी प्रकार भावकर्म का आन्तरिक कारण आत्मा है द्रव्यकर्म, जो सूक्ष्म कार्मण परमाणु है, इसका आत्मा निमित्त रूप में कर्ता है। जिस प्रकार दुग्ध को दधि रूप में, दधि को नवनीत और घृत में परिवर्तित करने में जिन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा होती है वे निमित्त कारण कहे जाते हैं ।
।
इन द्रव्य और भाव कर्म में मुख्यतया क्रमश: जड़ और चेतन की प्रमुखता होती है। इन दोनों में परस्पर कार्यकारणभाव है। जिस प्रकार मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी होती है, इनमें किसी को भी प्राथमिकता नहींदी जा सकती, उसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म में किसी की भी प्राथमिकता का निश्चय नहीं किया जा सकता । प्रत्येक द्रव्यकर्म तत्संबंधित भावकर्म का पूरक और प्रत्येक भावकर्म तत्संबंधित द्रव्यकर्म का पूरक है । अतः प्रवाह की अपेक्षा से इनका कार्यकारणभाव अनादिकालीन है।
केवल चेतन पक्ष या केवल जड़ पक्ष कर्म की समुचित व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता । द्रव्य और भाव कर्म से ही कर्म की पूर्ण व्याख्या बनती है।
कर्मपरमाणुओं का आत्मा से सम्बन्ध
प्रत्येक संसारी आत्मा प्रति समय सात-आठ कर्मों का बंध करती है। आयुष्य कर्म के बंध के समय आठ कर्मों का बंध अन्यथा सात कर्मों का बन्ध करती है। सजातीयता की दृष्टि से तो कर्म एक ही है, किन्तु जब जीव के मनवचन काया के योगों में परिस्पन्दन होता है, तब कर्मयोग्य परमाणु आत्मा के साथ कर्मरूप में संबद्ध हो जाते हैं। तदनन्तर इनका विभागीकरण होता है। जिस प्रकार व्यक्ति दुग्धपान करता है, दुग्ध जब उदरस्थ हो जाता
१८