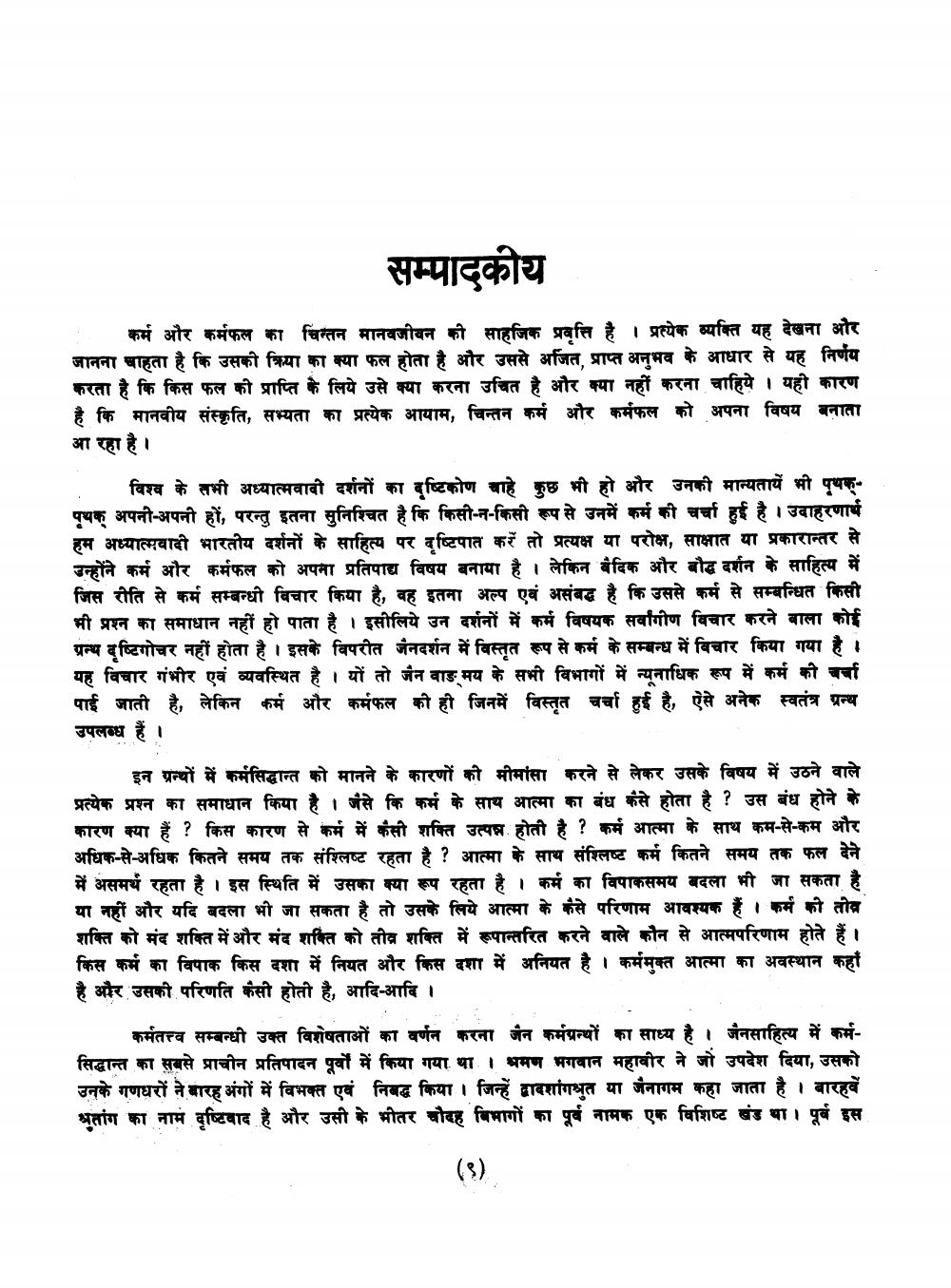________________
सम्पादकीय
कर्म और कर्मफल का चिन्तन मानवजीवन की साहजिक प्रवृत्ति है । प्रत्येक व्यक्ति यह देखना और जानना चाहता है कि उसकी क्रिया का क्या फल होता है और उससे अजित, प्राप्त अनुभव के आधार से यह निर्णय करता है कि किस फल की प्राप्ति के लिये उसे क्या करना उचित है और क्या नहीं करना चाहिये । यही कारण है कि मानवीय संस्कृति, सभ्यता का प्रत्येक आयाम, चिन्तन कर्म और कर्मफल को अपना विषय बनाता आ रहा है।
विश्व के सभी अध्यात्मवादी दर्शनों का दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो और उनकी मान्यतायें भी पृथक्पृथक् अपनी-अपनी हों, परन्तु इतना सुनिश्चित है कि किसी-न-किसी रूप से उनमें कर्म की चर्चा हुई है । उदाहरणार्थ हम अध्यात्मवादी भारतीय दर्शनों के साहित्य पर दृष्टिपात करें तो प्रत्यक्ष या परोक्ष, साक्षात या प्रकारान्तर से उन्होंने कर्म और कर्मफल को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है । लेकिन वैदिक और बौद्ध दर्शन के साहित्य में जिस रीति से कर्म सम्बन्धी विचार किया है, वह इतना अल्प एवं असंबद्ध है कि उससे कर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता है । इसीलिये उन दर्शनों में कर्म विषयक सर्वांगीण विचार करने वाला कोई ग्रन्थ दृष्टिगोचर नहीं होता है । इसके विपरीत जैनदर्शन में विस्तृत रूप से कर्म के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह विचार गंभीर एवं व्यवस्थित है। यों तो जैन वाङमय के सभी विभागों में न्यूनाधिक रूप में कर्म की चर्चा पाई जाती है, लेकिन कर्म और कर्मफल को ही जिनमें विस्तृत चर्चा हुई है, ऐसे अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं।
इन ग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त को मानने के कारणों की मीमांसा करने से लेकर उसके विषय में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का समाधान किया है। जैसे कि कर्म के साथ आत्मा का बंध कैसे होता है ? उस बंध होने के कारण क्या हैं ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति उत्पन्न होती है ? कर्म आत्मा के साथ कम-से-कम और अधिक-से-अधिक कितने समय तक संश्लिष्ट रहता है ? आत्मा के साथ संश्लिष्ट कर्म कितने समय तक फल देने में असमर्थ रहता है । इस स्थिति में उसका क्या रूप रहता है । कर्म का विपाकसमय बदला भी जा सकता है या नहीं और यदि बदला भी जा सकता है तो उसके लिये आत्मा के कैसे परिणाम आवश्यक हैं। कर्म को तोत्र शक्ति को मंद शक्ति में और मंद शक्ति को तीव्र शक्ति में रूपान्तरित करने वाले कौन से आत्मपरिणाम होते हैं। किस कर्म का विपाक किस दशा में नियत और किस दशा में अनियत है । कर्ममुक्त आत्मा का अवस्थान कहाँ है और उसकी परिणति कैसी होती है, आदि-आदि ।
कर्मतत्त्व सम्बन्धी उक्त विशेषताओं का वर्णन करना जैन कर्मग्रन्थों का साध्य है । जनसाहित्य में कर्मसिद्धान्त का सबसे प्राचीन प्रतिपादन पूर्वो में किया गया था । श्रमण भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, उसको उनके गणधरों ने बारह अंगों में विभक्त एवं निबद्ध किया। जिन्हें द्वादशांगश्रुत या जैनागम कहा जाता है । बारहवें श्रुतांग का नाम दृष्टिवाद है और उसी के भीतर चौदह विभागों का पूर्व नामक एक विशिष्ट खंड था। पूर्व इस
(९)