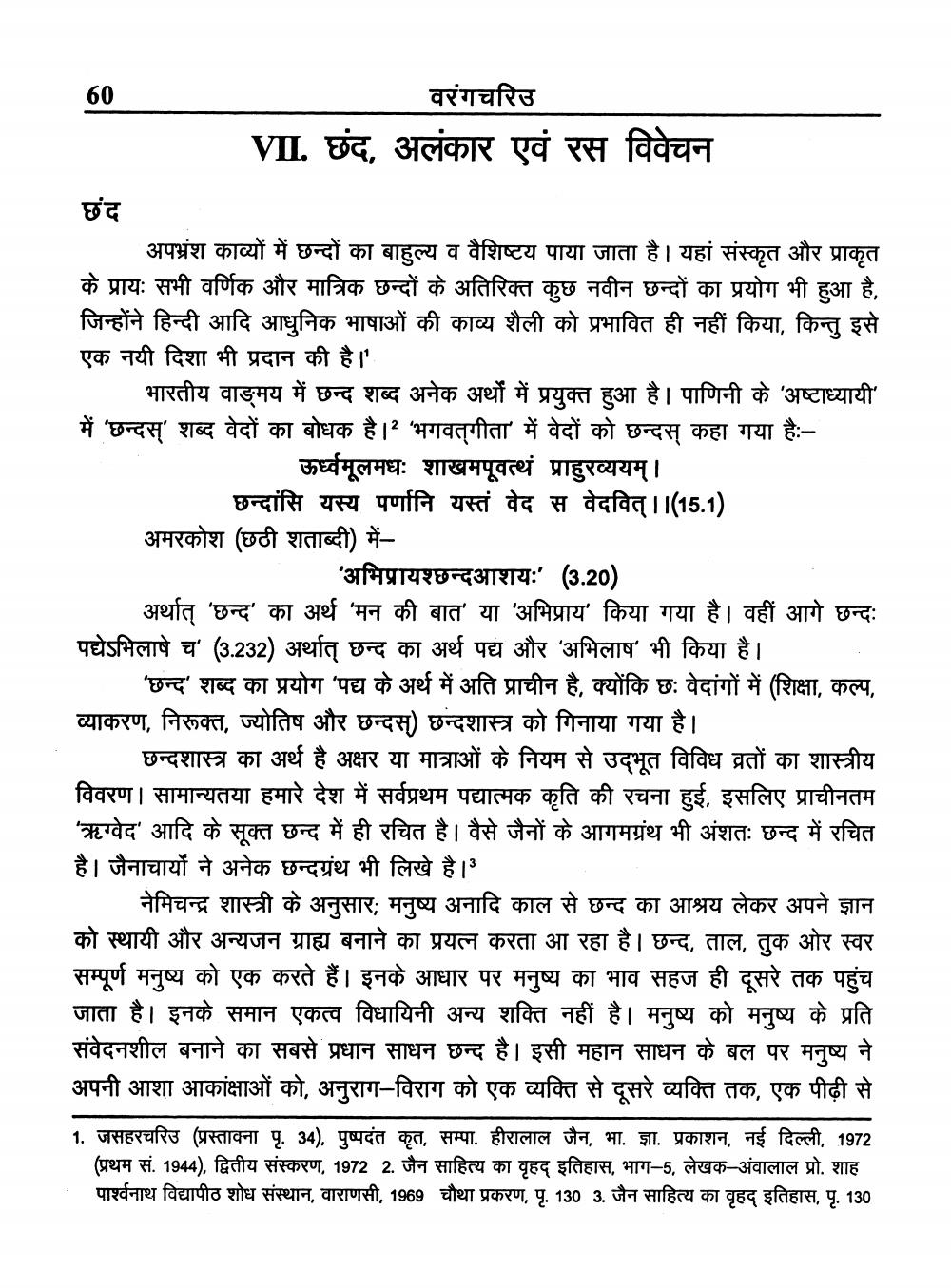________________
60
वरंगचरिउ VII. छंद, अलंकार एवं रस विवेचन
छंद
अपभ्रंश काव्यों में छन्दों का बाहुल्य व वैशिष्टय पाया जाता है। यहां संस्कृत और प्राकृत के प्रायः सभी वर्णिक और मात्रिक छन्दों के अतिरिक्त कुछ नवीन छन्दों का प्रयोग भी हुआ है, जिन्होंने हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं की काव्य शैली को प्रभावित ही नहीं किया, किन्तु इसे एक नयी दिशा भी प्रदान की है।'
भारतीय वाङ्मय में छन्द शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' में 'छन्दस्' शब्द वेदों का बोधक है। 'भगवत्गीता' में वेदों को छन्दस् कहा गया है:
__ऊर्ध्वमूलमधः शाखमपूवत्थं प्राहुरव्ययम्।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् । ।(15.1) अमरकोश (छठी शताब्दी) में
__'अभिप्रायश्छन्दआशयः' (3.20) अर्थात् 'छन्द' का अर्थ 'मन की बात' या 'अभिप्राय' किया गया है। वहीं आगे छन्दः पद्येऽभिलाषे च' (3.232) अर्थात् छन्द का अर्थ पद्य और 'अभिलाष' भी किया है।
'छन्द' शब्द का प्रयोग ‘पद्य के अर्थ में अति प्राचीन है, क्योंकि छः वेदांगों में (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष और छन्दस्) छन्दशास्त्र को गिनाया गया है।
छन्दशास्त्र का अर्थ है अक्षर या मात्राओं के नियम से उद्भूत विविध व्रतों का शास्त्रीय विवरण। सामान्यतया हमारे देश में सर्वप्रथम पद्यात्मक कृति की रचना हुई, इसलिए प्राचीनतम 'ऋग्वेद' आदि के सूक्त छन्द में ही रचित है। वैसे जैनों के आगमग्रंथ भी अंशतः छन्द में रचित है। जैनाचार्यों ने अनेक छन्दग्रंथ भी लिखे है।।
नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार; मनुष्य अनादि काल से छन्द का आश्रय लेकर अपने ज्ञान को स्थायी और अन्यजन ग्राह्य बनाने का प्रयत्न करता आ रहा है। छन्द, ताल, तुक ओर स्वर सम्पूर्ण मनुष्य को एक करते हैं। इनके आधार पर मनुष्य का भाव सहज ही दूसरे तक पहुंच जाता है। इनके समान एकत्व विधायिनी अन्य शक्ति नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे प्रधान साधन छन्द है। इसी महान साधन के बल पर मनुष्य ने अपनी आशा आकांक्षाओं को, अनुराग-विराग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से
1. जसहरचरिउ (प्रस्तावना पृ. 34). पुष्पदंत कृत, सम्पा. हीरालाल जैन, भा. ज्ञा. प्रकाशन, नई दिल्ली, 1972
(प्रथम सं. 1944), द्वितीय संस्करण, 1972 2. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग-5, लेखक-अंवालाल प्रो. शाह पार्श्वनाथ विद्यापीठ शोध संस्थान, वाराणसी, 1969 चौथा प्रकरण, पृ. 130 3. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, पृ. 130