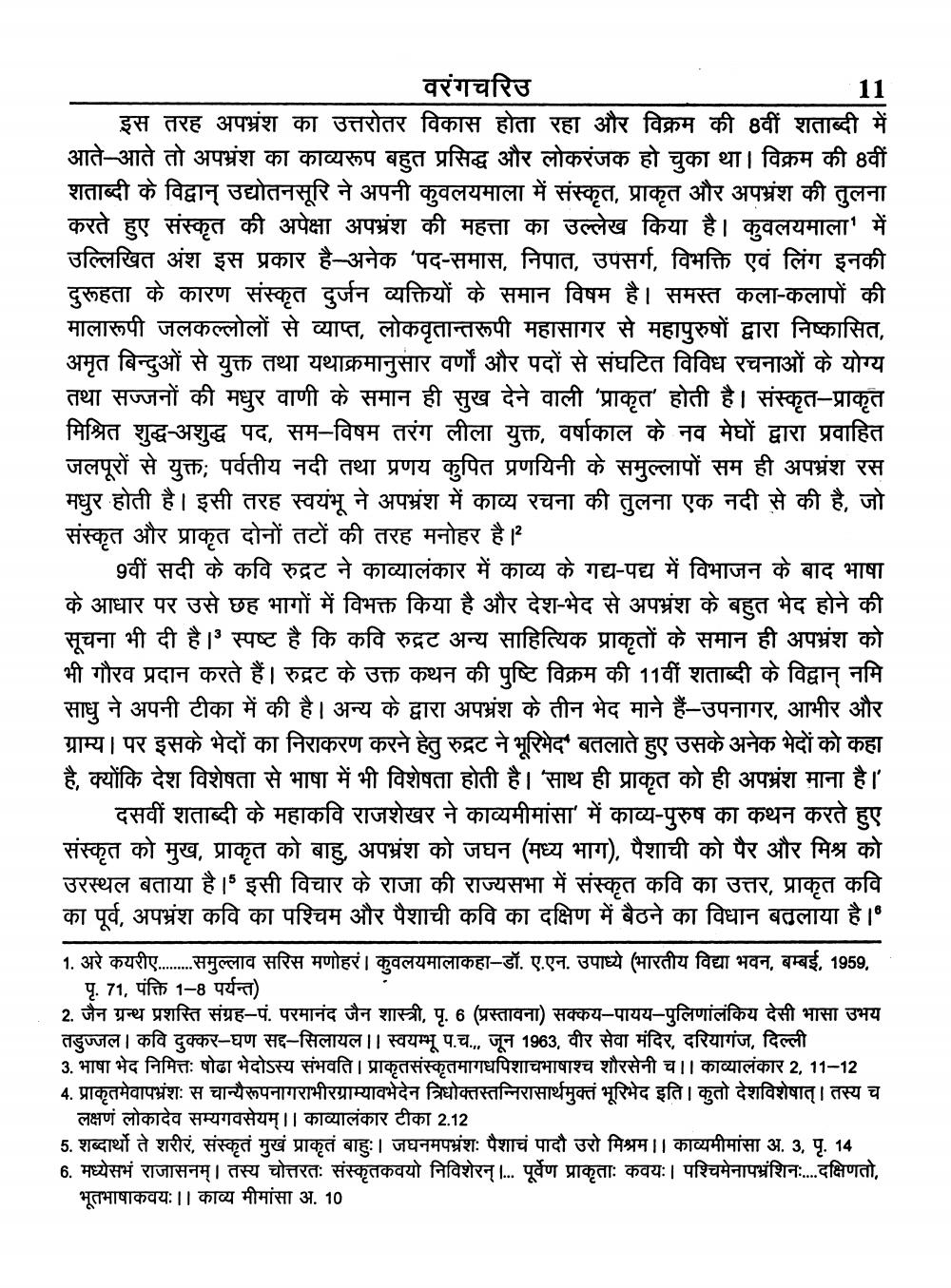________________
वरंगचरिउ
11 इस तरह अपभ्रंश का उत्तरोतर विकास होता रहा और विक्रम की 8वीं शताब्दी में आते-आते तो अपभ्रंश का काव्यरूप बहुत प्रसिद्ध और लोकरंजक हो चुका था । विक्रम की 8वीं शताब्दी के विद्वान् उद्योतनसूरि ने अपनी कुवलयमाला में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की तुलना करते हुए संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश की महत्ता का उल्लेख किया है। कुवलयमाला' में उल्लिखित अंश इस प्रकार है - अनेक 'पद- समास, निपात, उपसर्ग, विभक्ति एवं लिंग इनकी दुरूहता के कारण संस्कृत दुर्जन व्यक्तियों के समान विषम है । समस्त कला-कलापों की मालारूपी जलकल्लोलों से व्याप्त, लोकवृतान्तरूपी महासागर से महापुरुषों द्वारा निष्कासित, अमृत बिन्दुओं से युक्त तथा यथाक्रमानुसार वर्णों और पदों से संघटित विविध रचनाओं के योग्य तथा सज्जनों की मधुर वाणी के समान ही सुख देने वाली 'प्राकृत होती है। संस्कृत - प्राकृत मिश्रित शुद्ध - अशुद्ध पद, सम-विषम तरंग लीला युक्त, वर्षाकाल के नव मेघों द्वारा प्रवाहित जलपूरों से युक्त; पर्वतीय नदी तथा प्रणय कुपित प्रणयिनी के समुल्लापों सम ही अपभ्रंश रस मधुर होती है। इसी तरह स्वयंभू ने अपभ्रंश में काव्य रचना की तुलना एक नदी से की है, जो संस्कृत और प्राकृत दोनों तटों की तरह मनोहर है। 2
9वीं सदी के कवि रुद्रट ने काव्यालंकार में काव्य के गद्य-पद्य में विभाजन के बाद भाषा के आधार पर उसे छह भागों में विभक्त किया है और देश-भेद से अपभ्रंश के बहुत भेद होने की सूचना भी दी है।' स्पष्ट है कि कवि रुद्रट अन्य साहित्यिक प्राकृतों के समान ही अपभ्रंश को भी गौरव प्रदान करते हैं । रुद्रट के उक्त कथन की पुष्टि विक्रम की 11वीं शताब्दी के विद्वान् नमि साधु ने अपनी टीका में की है। अन्य के द्वारा अपभ्रंश के तीन भेद माने हैं- उपनागर, आभीर और ग्राम्य । पर इसके भेदों का निराकरण करने हेतु रुद्रट ने भूरिभेद' बतलाते हुए उसके अनेक भेदों को कहा है, क्योंकि देश विशेषता से भाषा में भी विशेषता होती है। 'साथ ही प्राकृत को ही अपभ्रंश माना है।' दसवीं शताब्दी के महाकवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा' में काव्य-पुरुष का कथन करते हुए संस्कृत को मुख, प्राकृत को बाहु, अपभ्रंश को जघन (मध्य भाग), पैशाची को पैर और मिश्र को उरस्थल बताया है।' इसी विचार के राजा की राज्यसभा में संस्कृत कवि का उत्तर, प्राकृत कवि का पूर्व, अपभ्रंश कवि का पश्चिम और पैशाची कवि का दक्षिण में बैठने का विधान बतलाया है । "
1. अरे कयरीए ........ ..समुल्लाव सरिस मणोहरं । कुवलयमालाकहा- डॉ. ए. एन. उपाध्ये (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1959, पृ. 71, पंक्ति 1-8 पर्यन्त)
2. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह - पं. परमानंद जैन शास्त्री, पृ. 6 (प्रस्तावना) सक्कय-पायय- पुलिणांलंकिय देसी भासा उभय तडुज्जल। कवि दुक्कर- घण सद्द- सिलायल । । स्वयम्भू प.च. जून 1963 वीर सेवा मंदिर, दरियागंज, दिल्ली
3. भाषा भेद निमित्तः षोढा भेदोऽस्य संभवति । प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्च शौरसेनी च ।। काव्यालंकार 2, 11-12 4. प्राकृतमेवापभ्रंशः स चान्यैरूपनागराभीरग्राम्यावभेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासार्थमुक्तं भूरिभेद इति । कुतो देशविशेषात् । तस्य च लक्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम् ।। काव्यालंकार टीका 2.12
5. शब्दार्थो ते शरीरं, संस्कृतं मुखं प्राकृतं बाहुः । जघनमपभ्रंशः पैशाचं पादौ उरो मिश्रम ।। काव्यमीमांसा अ. 3, पृ. 14 6. मध्येसभं राजासनम्। तस्य चोत्तरतः संस्कृतकवयो निविशेरन् ।... पूर्वेण प्राकृताः कवयः । पश्चिमेनापभ्रंशिनः...दक्षिणतो, भूतभाषाकवयः ।। काव्य मीमांसा अ. 10