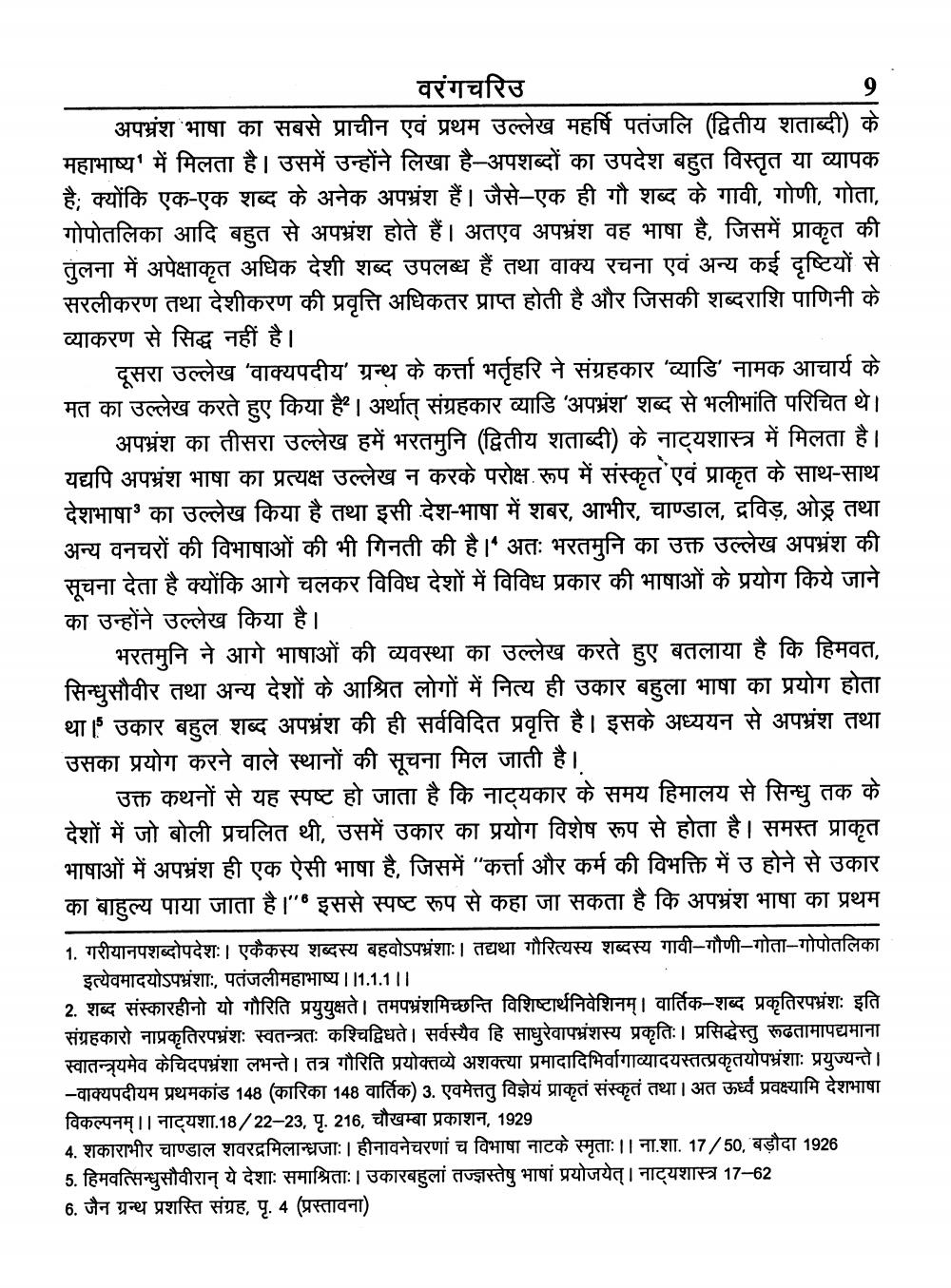________________
वरंगचरिउ अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीन एवं प्रथम उल्लेख महर्षि पतंजलि (द्वितीय शताब्दी) के महाभाष्य' में मिलता है। उसमें उन्होंने लिखा है-अपशब्दों का उपदेश बहुत विस्तृत या व्यापक है; क्योंकि एक-एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं। जैसे-एक ही गौ शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि बहुत से अपभ्रंश होते हैं। अतएव अपभ्रंश वह भाषा है, जिसमें प्राकृत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक देशी शब्द उपलब्ध हैं तथा वाक्य रचना एवं अन्य कई दृष्टियों से सरलीकरण तथा देशीकरण की प्रवृत्ति अधिकतर प्राप्त होती है और जिसकी शब्दराशि पाणिनी के व्याकरण से सिद्ध नहीं है।
दूसरा उल्लेख 'वाक्यपदीय' ग्रन्थ के कर्ता भर्तृहरि ने संग्रहकार 'व्याडि' नामक आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए किया है । अर्थात् संग्रहकार व्याडि 'अपभ्रंश' शब्द से भलीभांति परिचित थे। ___अपभ्रंश का तीसरा उल्लेख हमें भरतमुनि (द्वितीय शताब्दी) के नाट्यशास्त्र में मिलता है। यद्यपि अपभ्रंश भाषा का प्रत्यक्ष उल्लेख न करके परोक्ष रूप में संस्कृत एवं प्राकृत के साथ-साथ देशभाषा' का उल्लेख किया है तथा इसी देश-भाषा में शबर, आभीर, चाण्डाल, द्रविड़, ओड्र तथा अन्य वनचरों की विभाषाओं की भी गिनती की है। अतः भरतमुनि का उक्त उल्लेख अपभ्रंश की सूचना देता है क्योंकि आगे चलकर विविध देशों में विविध प्रकार की भाषाओं के प्रयोग किये जाने का उन्होंने उल्लेख किया है।
भरतमुनि ने आगे भाषाओं की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि हिमवत, सिन्धुसौवीर तथा अन्य देशों के आश्रित लोगों में नित्य ही उकार बहुला भाषा का प्रयोग होता था। उकार बहुल शब्द अपभ्रंश की ही सर्वविदित प्रवृत्ति है। इसके अध्ययन से अपभ्रंश तथा उसका प्रयोग करने वाले स्थानों की सूचना मिल जाती है।
उक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्यकार के समय हिमालय से सिन्धु तक के देशों में जो बोली प्रचलित थी, उसमें उकार का प्रयोग विशेष रूप से होता है। समस्त प्राकृत भाषाओं में अपभ्रंश ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें "कर्ता और कर्म की विभक्ति में उ होने से उकार का बाहुल्य पाया जाता है। इससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम 1. गरीयानपशब्दोपदेशः। एकैकस्य शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी-गौणी-गोता-गोपोतलिका
इत्येवमादयोऽपभ्रंशाः, पतंजलीमहाभाष्य ।।1.1.1 ।। 2. शब्द संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते। तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्। वार्तिक-शब्द प्रकृतिरपभ्रंशः इति संग्रहकारो नाप्रकृतिरपभ्रंशः स्वतन्त्रतः कश्चिद्विधते। सर्वस्यैव हि साधुरेवापभ्रंशस्य प्रकृतिः। प्रसिद्धेस्तु रूढतामापद्यमाना स्वातन्त्र्यमेव केचिदपभ्रंशा लभन्ते। तत्र गौरिति प्रयोक्तव्ये अशक्त्या प्रमादादिभिर्वागाव्यादयस्तत्प्रकृतयोपभ्रंशाः प्रयुज्यन्ते। -वाक्यपदीयम प्रथमकांड 148 (कारिका 148 वार्तिक) 3. एवमेत्ततु विज्ञेयं प्राकृतं संस्कृतं तथा। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषा विकल्पनम्।। नाट्यशा.18/22-23, पृ. 216, चौखम्बा प्रकाशन, 1929 4. शकाराभीर चाण्डाल शवरद्रमिलान्ध्रजाः । हीनावनेचरणां च विभाषा नाटके स्मृताः ।। ना.शा. 17/50, बड़ौदा 1926 5. हिमवत्सिन्धुसौवीरान् ये देशाः समाश्रिताः । उकारबहुलां तज्ज्ञस्तेषु भाषां प्रयोजयेत् । नाट्यशास्त्र 17-62 6. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, पृ. 4 (प्रस्तावना)