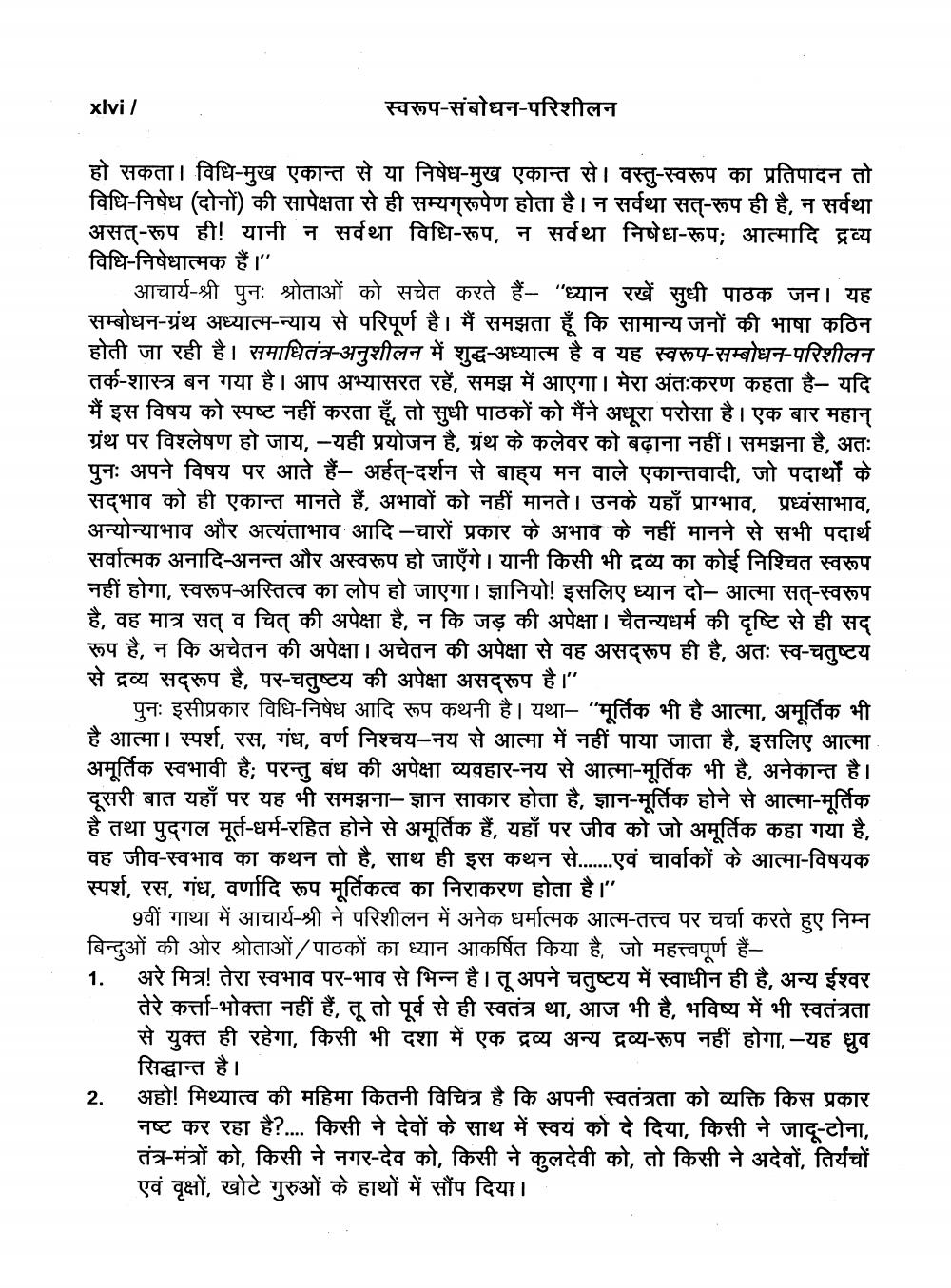________________
स्वरूप-संबोधन - परिशीलन
हो सकता। विधि-मुख एकान्त से या निषेध - मुख एकान्त से । वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन तो विधि - निषेध (दोनों) की सापेक्षता से ही सम्यग्रुपेण होता है । न सर्वथा सत्-रूप ही है, न सर्वथा असत्-रूप ही! यानी न सर्वथा विधि-रूप, न सर्वथा निषेध-रूप; आत्मादि द्रव्य विधि - निषेधात्मक हैं।"
xlvi /
आचार्य श्री पुनः श्रोताओं को सचेत करते हैं- "ध्यान रखें सुधी पाठक जन । यह सम्बोधन ग्रंथ अध्यात्म- न्याय से परिपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सामान्य जनों की भाषा कठिन होती जा रही है। समाधितंत्र - अनुशीलन में शुद्ध - अध्यात्म है व यह स्वरूप-सम्बोधन-परिशीलन तर्क - शास्त्र बन गया है। आप अभ्यासरत रहें, समझ में आएगा । मेरा अंतःकरण कहता है- यदि मैं इस विषय को स्पष्ट नहीं करता हूँ, तो सुधी पाठकों को मैंने अधूरा परोसा है। एक बार महान् ग्रंथ पर विश्लेषण हो जाय, यही प्रयोजन है, ग्रंथ के कलेवर को बढ़ाना नहीं । समझना है, अतः पुनः अपने विषय पर आते हैं- अर्हत्-दर्शन से बाह्य मन वाले एकान्तवादी, जो पदार्थों के सद्भाव को ही एकान्त मानते हैं, अभावों को नहीं मानते। उनके यहाँ प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव आदि - चारों प्रकार के अभाव के नहीं मानने से सभी पदार्थ सर्वात्मक अनादि-अनन्त और अस्वरूप हो जाएँगे। यानी किसी भी द्रव्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होगा, स्वरूप- अस्तित्व का लोप हो जाएगा । ज्ञानियो ! इसलिए ध्यान दो- आत्मा सत्-स्वरूप है, वह मात्र सत् व चित् की अपेक्षा है, न कि जड़ की अपेक्षा । चैतन्यधर्म की दृष्टि से ही सद् रूप है, न कि अचेतन की अपेक्षा । अचेतन की अपेक्षा से वह असद्रूप ही है, अतः स्व-चतुष्टय से द्रव्य सद्रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असद्रूप है ।"
पुनः इसीप्रकार विधि-निषेध आदि रूप कथनी है । यथा- "मूर्तिक भी है आत्मा, अमूर्तिक भी है आत्मा । स्पर्श, रस, गंध, वर्ण निश्चय - नय से आत्मा में नहीं पाया जाता है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक स्वभावी है; परन्तु बंध की अपेक्षा व्यवहार- नय से आत्मा - मूर्तिक भी है, अनेकान्त है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझना - ज्ञान साकार होता है, ज्ञान- मूर्तिक होने से आत्मा - मूर्तिक है तथा पुद्गल मूर्त-धर्म- रहित होने से अमूर्तिक हैं, यहाँ पर जीव को जो अमूर्तिक कहा गया है, वह जीव-स्वभाव का कथन तो है, साथ ही इस कथन से.......एवं चार्वाकों के आत्मा-विषयक स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि रूप मूर्तिकत्व का निराकरण होता है।"
9वीं गाथा में आचार्य श्री ने परिशीलन में अनेक धर्मात्मक आत्म-तत्त्व पर चर्चा करते हुए निम्न बिन्दुओं की ओर श्रोताओं / पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो महत्त्वपूर्ण हैं
1.
अरे मित्र! तेरा स्वभाव पर भाव से भिन्न है। तू अपने चतुष्टय में स्वाधीन ही है, अन्य ईश्वर तेरे कर्त्ता - भोक्ता नहीं हैं, तू तो पूर्व से ही स्वतंत्र था, आज भी है, भविष्य में भी स्वतंत्रता से युक्त ही रहेगा, किसी भी दशा में एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होगा - यह ध्रुव सिद्धान्त है।
2.
अहो! मिथ्यात्व की महिमा कितनी विचित्र है कि अपनी स्वतंत्रता को व्यक्ति किस प्रकार नष्ट कर रहा है?.... किसी ने देवों के साथ में स्वयं को दे दिया, किसी ने जादू-टोना, तंत्र-मंत्रों को, किसी ने नगर देव को, किसी ने कुलदेवी को, तो किसी ने अदेवों, तिर्यंचों एवं वृक्षों, खोटे गुरुओं के हाथों में सौंप दिया ।