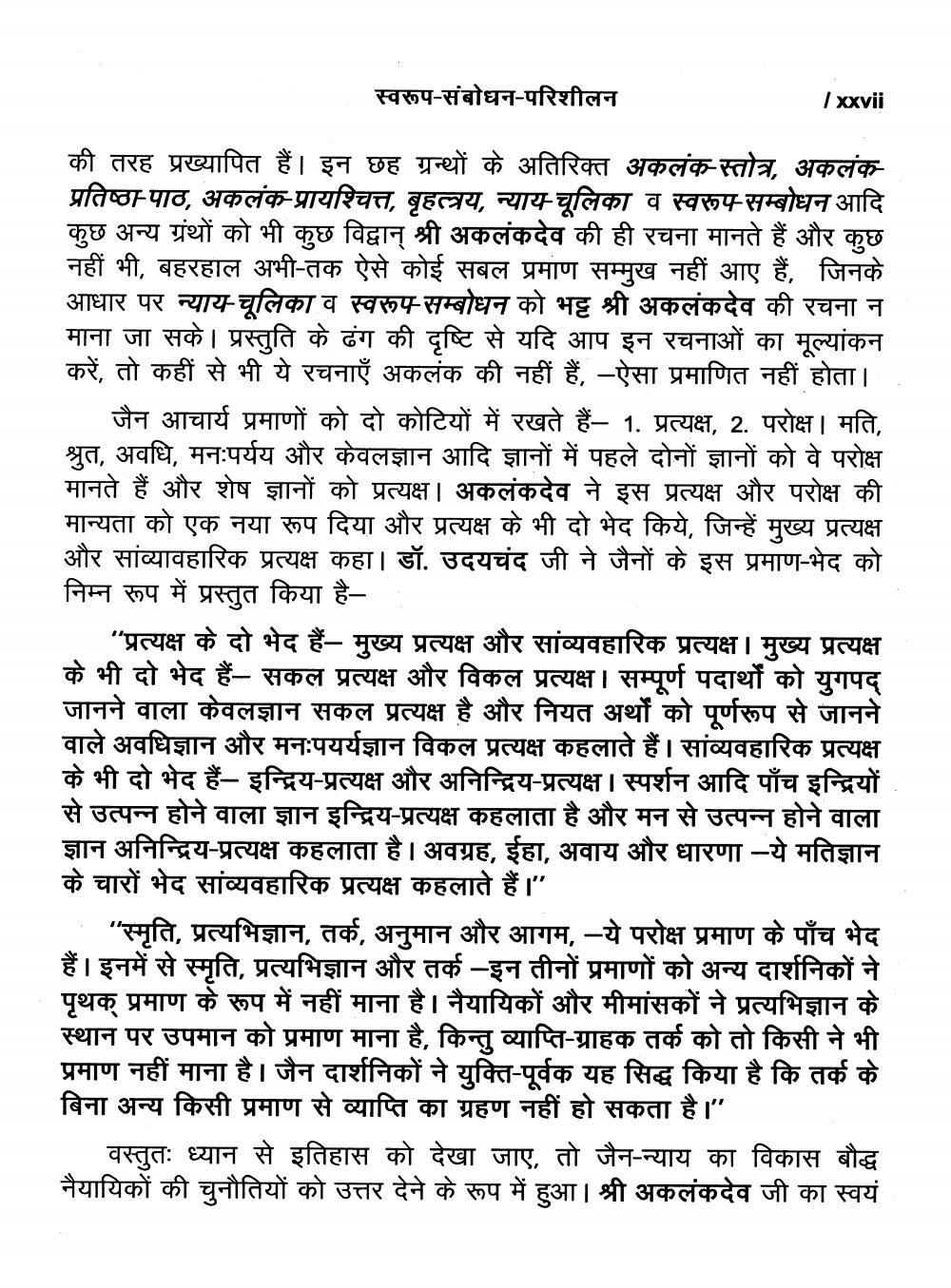________________
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
/ xxvii
की तरह प्रख्यापित हैं। इन छह ग्रन्थों के अतिरिक्त अकलंक-स्तोत्र, अकलंक प्रतिष्ठा पाठ, अकलंक-प्रायश्चित्त, बृहत्त्रय, न्याय-चूलिका व स्वरूप सम्बोधन आदि कुछ अन्य ग्रंथों को भी कुछ विद्वान् श्री अकलंकदेव की ही रचना मानते हैं और कुछ नहीं भी, बहरहाल अभी-तक ऐसे कोई सबल प्रमाण सम्मुख नहीं आए हैं, जिनके आधार पर न्यायचूलिका व स्वरूप-सम्बोधन को भट्ट श्री अकलंकदेव की रचना न माना जा सके। प्रस्तुति के ढंग की दृष्टि से यदि आप इन रचनाओं का मूल्यांकन करें, तो कहीं से भी ये रचनाएँ अकलंक की नहीं हैं, -ऐसा प्रमाणित नहीं होता। ___ जैन आचार्य प्रमाणों को दो कोटियों में रखते हैं- 1. प्रत्यक्ष, 2. परोक्ष। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान आदि ज्ञानों में पहले दोनों ज्ञानों को वे परोक्ष मानते हैं और शेष ज्ञानों को प्रत्यक्ष। अकलंकदेव ने इस प्रत्यक्ष और परोक्ष की मान्यता को एक नया रूप दिया और प्रत्यक्ष के भी दो भेद किये, जिन्हें मुख्य प्रत्यक्ष
और सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा। डॉ. उदयचंद जी ने जैनों के इस प्रमाण-भेद को निम्न रूप में प्रस्तुत किया है___"प्रत्यक्ष के दो भेद हैं- मुख्य प्रत्यक्ष और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष । मुख्य प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं- सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष । सम्पूर्ण पदार्थों को युगपद् जानने वाला केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और नियत अर्थों को पूर्णरूप से जानने वाले अवधिज्ञान और मनःपयर्यज्ञान विकल प्रत्यक्ष कहलाते हैं। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष । स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कहलाता है और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष कहलाता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा -ये मतिज्ञान के चारों भेद सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं।" ____ "स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, –ये परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं। इनमें से स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क-इन तीनों प्रमाणों को अन्य दार्शनिकों ने पृथक् प्रमाण के रूप में नहीं माना है। नैयायिकों और मीमांसकों ने प्रत्यभिज्ञान के स्थान पर उपमान को प्रमाण माना है, किन्तु व्याप्ति-ग्राहक तर्क को तो किसी ने भी प्रमाण नहीं माना है। जैन दार्शनिकों ने युक्ति-पूर्वक यह सिद्ध किया है कि तर्क के बिना अन्य किसी प्रमाण से व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो सकता है।"
वस्तुतः ध्यान से इतिहास को देखा जाए, तो जैन-न्याय का विकास बौद्ध नैयायिकों की चुनौतियों को उत्तर देने के रूप में हुआ। श्री अकलंकदेव जी का स्वयं