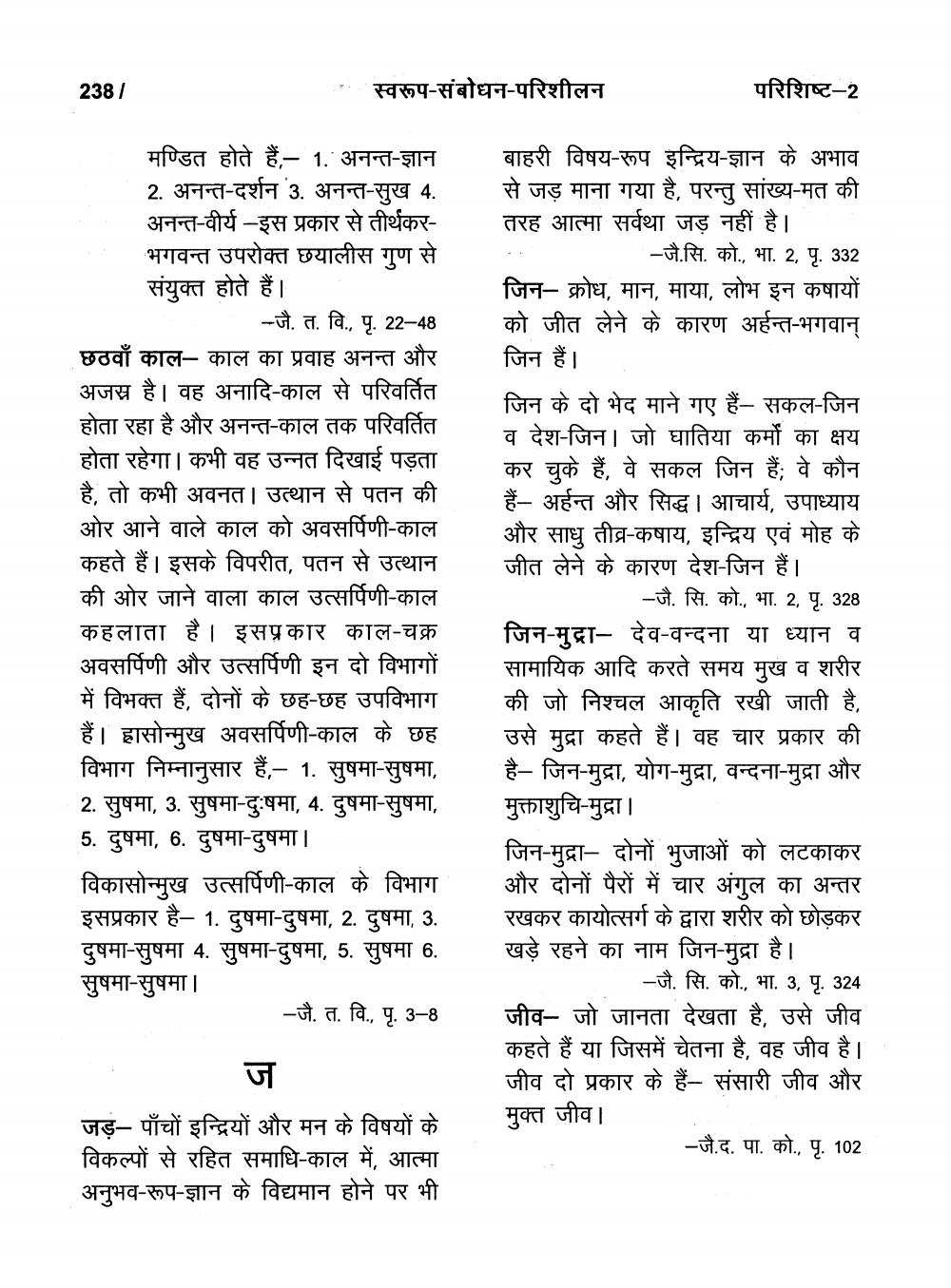________________
238/
स्वरूप - संबोधन - परिशीलन
मण्डित होते हैं, - 1. अनन्त - ज्ञान 2. अनन्त - दर्शन 3. अनन्त सुख 4. अनन्त-वीर्य - इस प्रकार से तीर्थंकरभगवन्त उपरोक्त छयालीस गुण से संयुक्त होते हैं।
त. वि., पृ. 22-48 छठवाँ काल- काल का प्रवाह अनन्त और अजस्र है । वह अनादि काल से परिवर्तित होता रहा है और अनन्त काल तक परिवर्तित होता रहेगा। कभी वह उन्नत दिखाई पड़ता है, तो कभी अवनत । उत्थान से पतन की ओर आने वाले काल को अवसर्पिणी-काल कहते हैं । इसके विपरीत, पतन से उत्थान की ओर जाने वाला काल उत्सर्पिणी-काल कहलाता है । इसप्रकार काल-चक्र अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इन दो विभागों में विभक्त हैं, दोनों के छह-छह उपविभाग हैं । ह्रासोन्मुख अवसर्पिणी-काल के छह विभाग निम्नानुसार हैं, - 1. सुषमा- सुषमा, 2. सुषमा, 3. सुषमा- दुःषमा, 4. दुषमा- सुषमा, 5. दुषमा, 6. दुषमा-दुषमा । विकासोन्मुख उत्सर्पिणी-काल के विभाग इसप्रकार है - 1. दुषमा - दुषमा, 2. दुषमा, 3. दुषमा- सुषमा 4. सुषमा - दुषमा, 5. सुषमा 6. सुषमा- सुषमा ।
-जै. त. वि., पृ. 3-8
ज
जड़- पाँचों इन्द्रियों और मन के विषयों के विकल्पों से रहित समाधि-काल में, आत्मा अनुभव-रूप- ज्ञान के विद्यमान होने पर भी
परिशिष्ट-2
बाहरी विषय-रूप इन्द्रिय- ज्ञान के अभाव से जड़ माना गया है, परन्तु सांख्य-मत की तरह आत्मा सर्वथा जड़ नहीं है। - जै. सि. को. भा. 2, पृ. 332 जिन - क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों को जीत लेने के कारण अर्हन्त-भगवान् जिन हैं।
जिन के दो भेद माने गए हैं- सकल- जिन व देश - जिन । जो घातिया कर्मों का क्षय कर चुके हैं, वे सकल जिन हैं; वे कौन हैं - अर्हन्त और सिद्ध । आचार्य, उपाध्याय और साधु तीव्र - कषाय, इन्द्रिय एवं मोह के जीत लेने के कारण देश - जिन हैं ।
- जै. सि. को, भा. 2, पृ. 328 जिन - मुद्रा - देव- वन्दना या ध्यान व सामायिक आदि करते समय मुख व शरीर की जो निश्चल आकृति रखी जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। वह चार प्रकार की है - जिन-मुद्रा, योग-मुद्रा, वन्दना - मुद्रा और मुक्ताशुचि-मुद्रा ।
जिन-मुद्रा- दोनों भुजाओं को लटकाकर और दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर को छोड़कर खड़े रहने का नाम जिन - मुद्रा है।
- जै. सि. को., भा. 3, पृ. 324 जीव- जो जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं या जिसमें चेतना है, वह जीव है । जीव दो प्रकार के हैं- संसारी जीव और मुक्त जीव ।
- जै. द. पा. को., पृ. 102