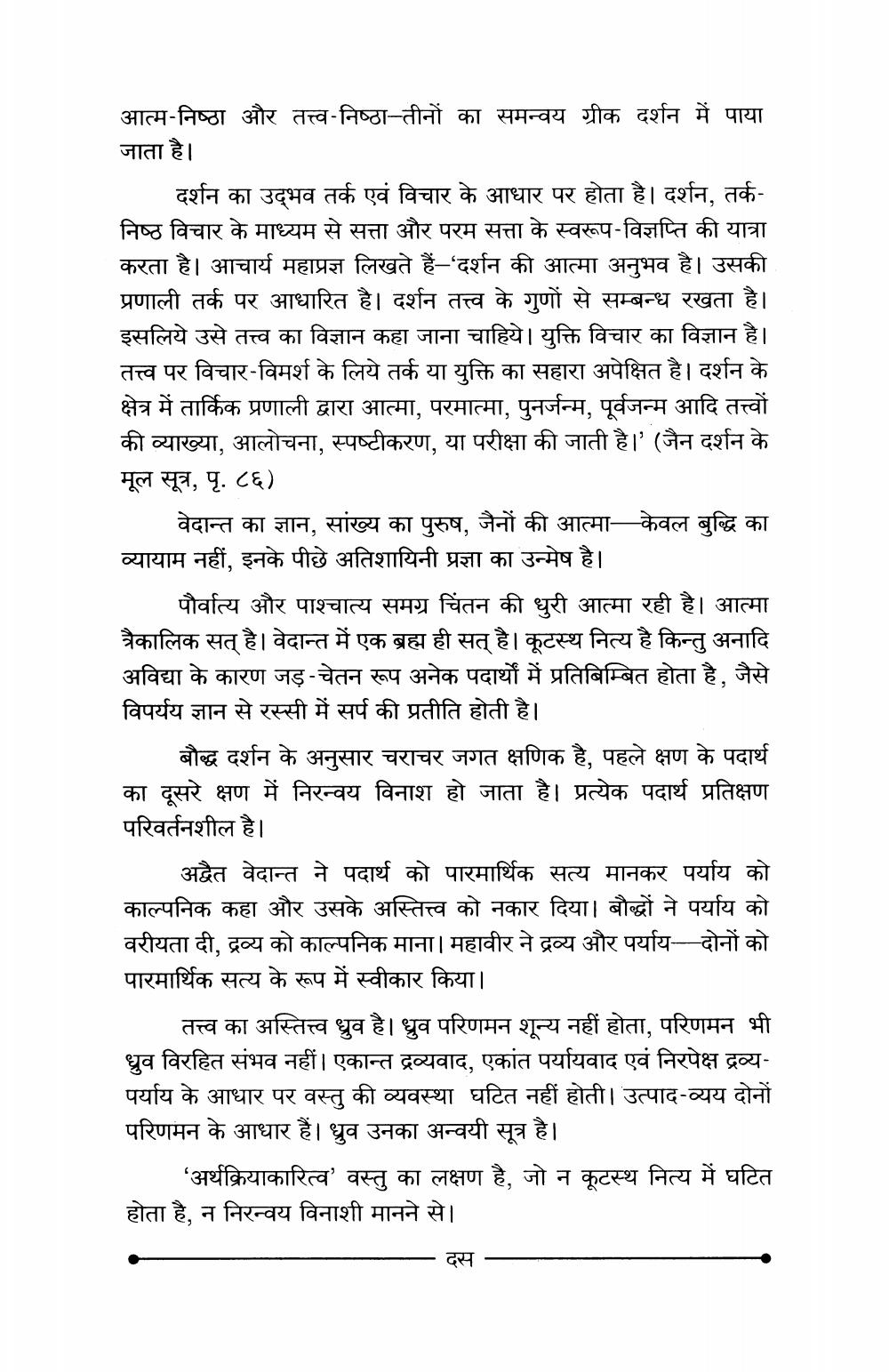________________
आत्म-निष्ठा और तत्त्व-निष्ठा - तीनों का समन्वय ग्रीक दर्शन में पाया जाता है।
दर्शन का उद्भव तर्क एवं विचार के आधार पर होता है । दर्शन, तर्कनिष्ठ विचार के माध्यम से सत्ता और परम सत्ता के स्वरूप - विज्ञप्ति की यात्रा करता है। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं- 'दर्शन की आत्मा अनुभव है । उसकी प्रणाली तर्क पर आधारित है। दर्शन तत्त्व के गुणों से सम्बन्ध रखता है। इसलिये उसे तत्त्व का विज्ञान कहा जाना चाहिये । युक्ति विचार का विज्ञान है। तत्त्व पर विचार-विमर्श के लिये तर्क या युक्ति का सहारा अपेक्षित है। दर्शन के क्षेत्र में तार्किक प्रणाली द्वारा आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म आदि तत्त्वों की व्याख्या, आलोचना, स्पष्टीकरण, या परीक्षा की जाती है।' (जैन दर्शन के मूल सूत्र, पृ. ८६)
वेदान्त का ज्ञान, सांख्य का पुरुष, जैनों की आत्मा — केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं, इनके पीछे अतिशायिनी प्रज्ञा का उन्मेष है।
पौर्वात्य और पाश्चात्य समग्र चिंतन की धुरी आत्मा रही है। आत्मा त्रैकालिक सत् है। वेदान्त में एक ब्रह्म ही सत् है । कूटस्थ नित्य है किन्तु अनादि अविद्या के कारण जड़-चेतन रूप अनेक पदार्थों में प्रतिबिम्बित होता है, जैसे विपर्यय ज्ञान से रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार चराचर जगत क्षणिक है, पहले क्षण के पदार्थ का दूसरे क्षण में निरन्वय विनाश हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।
अद्वैत वेदान्त ने पदार्थ को पारमार्थिक सत्य मानकर पर्याय को काल्पनिक कहा और उसके अस्तित्त्व को नकार दिया। बौद्धों ने पर्याय को वरीयता दी, द्रव्य को काल्पनिक माना। महावीर ने द्रव्य और पर्याय—दोनों को पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार किया।
तत्त्व का अस्तित्त्व ध्रुव है | ध्रुव परिणमन शून्य नहीं होता, परिणमन भी ध्रुव विरहित संभव नहीं । एकान्त द्रव्यवाद, एकांत पर्यायवाद एवं निरपेक्ष द्रव्यपर्याय के आधार पर वस्तु की व्यवस्था घटित नहीं होती । उत्पाद-व्यय दोनों परिणमन के आधार हैं । ध्रुव उनका अन्वयी सूत्र है ।
‘अर्थक्रियाकारित्व’ वस्तु का लक्षण है, जो न कूटस्थ नित्य में घटित होता है, न निरन्वय विनाशी मानने से ।
दस