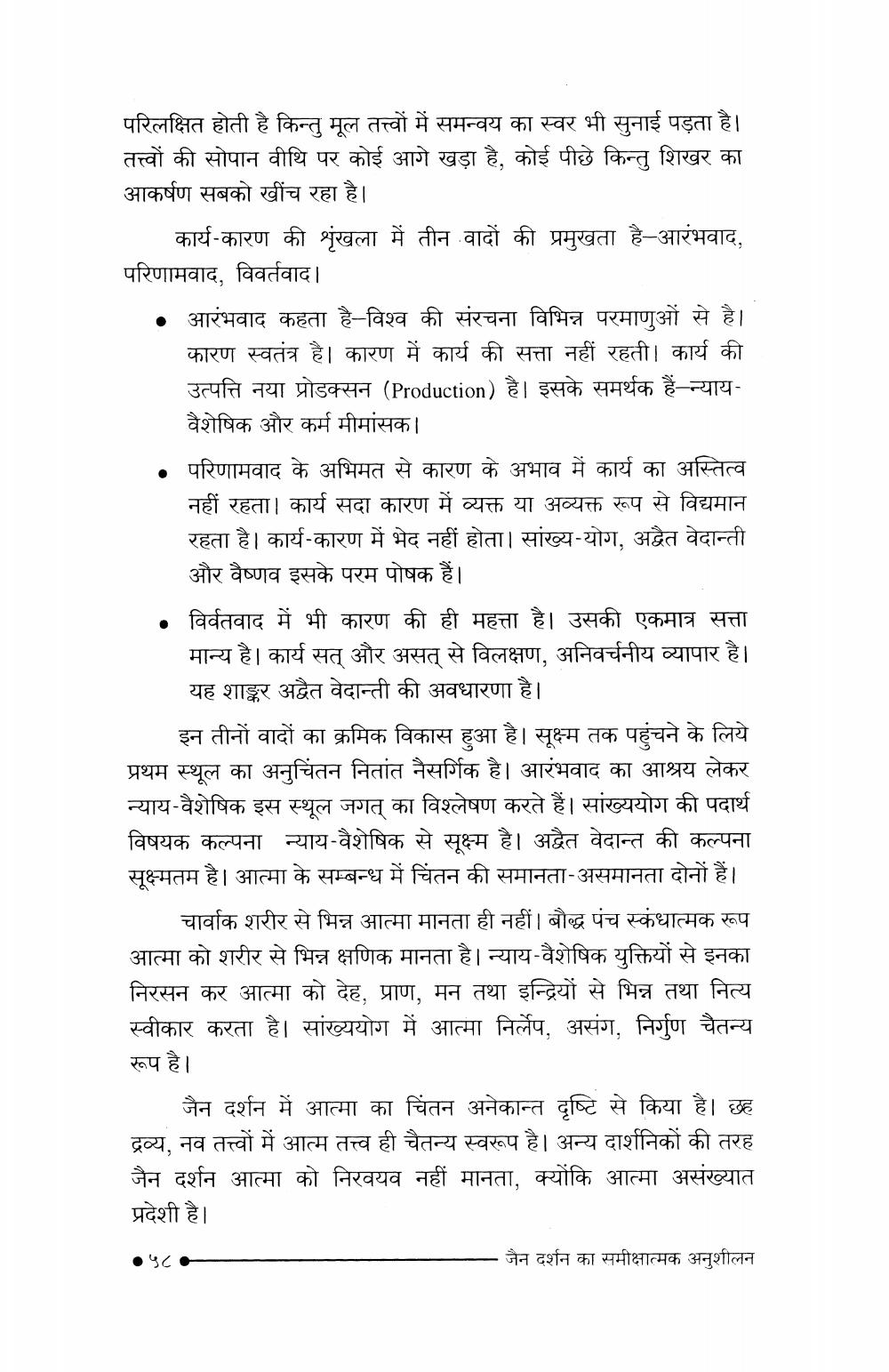________________
परिलक्षित होती है किन्तु मूल तत्त्वों में समन्वय का स्वर भी सुनाई पड़ता है। तत्त्वों की सोपान वीथि पर कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे किन्तु शिखर का आकर्षण सबको खींच रहा है।
कार्य-कारण की श्रृंखला में तीन वादों की प्रमुखता है- आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद ।
आरंभवाद कहता है-विश्व की संरचना विभिन्न परमाणुओं से है। कारण स्वतंत्र है। कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती । कार्य की उत्पत्ति नया प्रोडक्सन (Production) है। इसके समर्थक हैं-न्यायवैशेषिक और कर्म मीमांसक ।
• परिणामवाद के अभिमत से कारण के अभाव में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता। कार्य सदा कारण में व्यक्त या अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। कार्य-कारण में भेद नहीं होता । सांख्य-योग, अद्वैत वेदान्ती और वैष्णव इसके परम पोषक हैं।
• विर्वतवाद में भी कारण की ही महत्ता है। उसकी एकमात्र सत्ता मान्य है। कार्य सत् और असत् से विलक्षण, अनिवर्चनीय व्यापार है। यह शाङ्कर अद्वैत वेदान्ती की अवधारणा है ।
इन तीनों वादों का क्रमिक विकास हुआ है। सूक्ष्म तक पहुंचने के लिये प्रथम स्थूल का अनुचिंतन नितांत नैसर्गिक है। आरंभवाद का आश्रय लेकर न्याय-वैशेषिक इस स्थूल जगत् का विश्लेषण करते हैं । सांख्ययोग की पदार्थ विषयक कल्पना न्याय-वैशेषिक से सूक्ष्म है। अद्वैत वेदान्त की कल्पना सूक्ष्मतम है। आत्मा के सम्बन्ध में चिंतन की समानता - असमानता दोनों हैं।
चार्वाक शरीर से भिन्न आत्मा मानता ही नहीं । बौद्ध पंच स्कंधात्मक रूप आत्मा को शरीर से भिन्न क्षणिक मानता है । न्याय-वैशेषिक युक्तियों से इनका निरसन कर आत्मा को देह, प्राण, मन तथा इन्द्रियों से भिन्न तथा नित्य स्वीकार करता है। सांख्ययोग में आत्मा निर्लेप, असंग, निर्गुण चैतन्य रूप है।
जैन दर्शन में आत्मा का चिंतन अनेकान्त दृष्टि से किया है। छह द्रव्य, नव तत्त्वों में आत्म तत्त्व ही चैतन्य स्वरूप है। अन्य दार्शनिकों की तरह जैन दर्शन आत्मा को निरवयव नहीं मानता, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है।
०५८
जैन दर्शन का समीक्षात्मक अनुशीलन