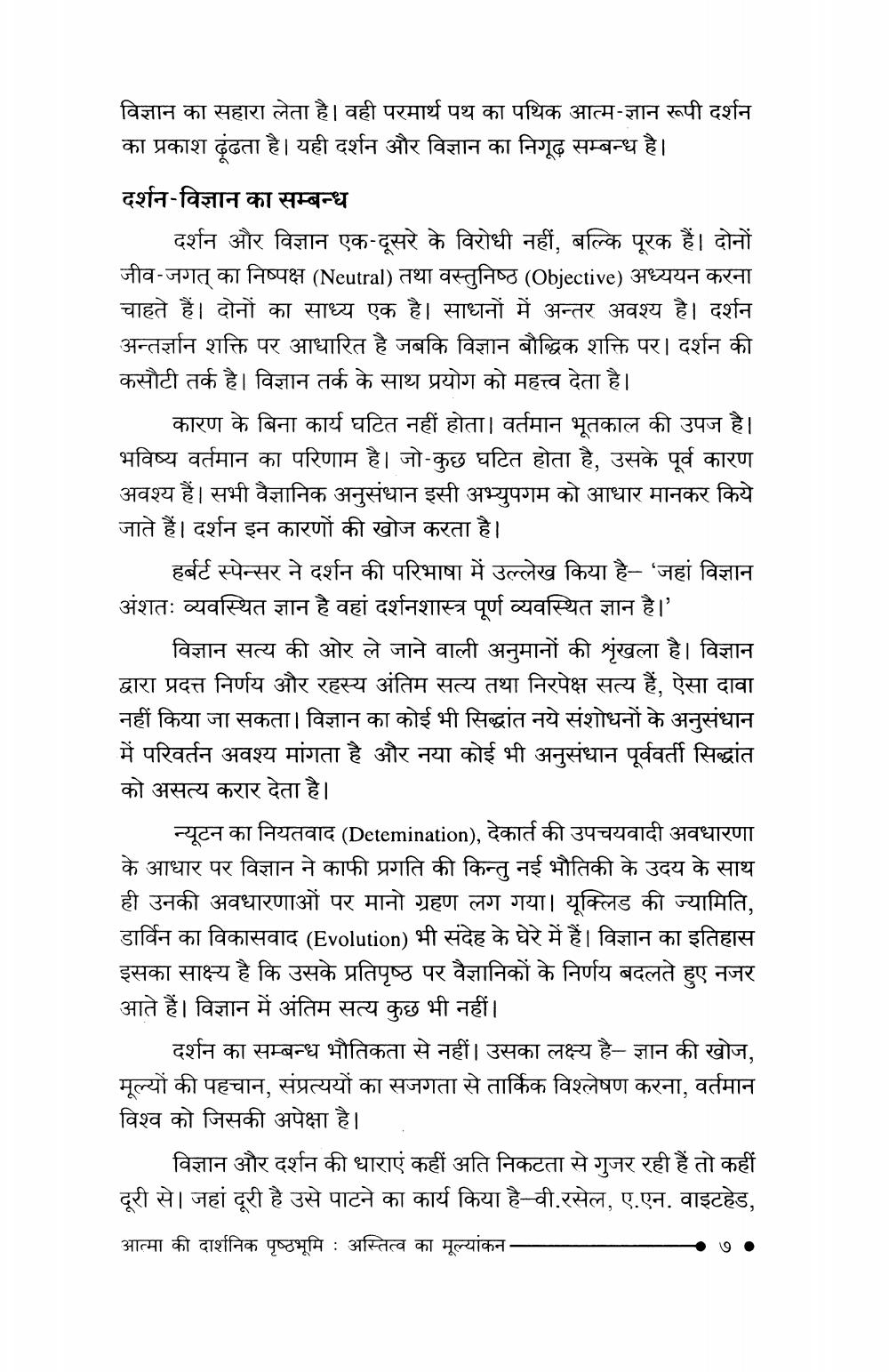________________
विज्ञान का सहारा लेता है। वही परमार्थ पथ का पथिक आत्म-ज्ञान रूपी दर्शन का प्रकाश ढूंढता है। यही दर्शन और विज्ञान का निगूढ़ सम्बन्ध है। दर्शन-विज्ञान का सम्बन्ध
दर्शन और विज्ञान एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। दोनों जीव-जगत् का निष्पक्ष (Neutral) तथा वस्तुनिष्ठ (Objective) अध्ययन करना चाहते हैं। दोनों का साध्य एक है। साधनों में अन्तर अवश्य है। दर्शन अन्तर्ज्ञान शक्ति पर आधारित है जबकि विज्ञान बौद्धिक शक्ति पर। दर्शन की कसौटी तर्क है। विज्ञान तर्क के साथ प्रयोग को महत्त्व देता है।
कारण के बिना कार्य घटित नहीं होता। वर्तमान भूतकाल की उपज है। भविष्य वर्तमान का परिणाम है। जो-कुछ घटित होता है, उसके पूर्व कारण अवश्य हैं। सभी वैज्ञानिक अनुसंधान इसी अभ्युपगम को आधार मानकर किये जाते हैं। दर्शन इन कारणों की खोज करता है।
हर्बर्ट स्पेन्सर ने दर्शन की परिभाषा में उल्लेख किया है- 'जहां विज्ञान अंशतः व्यवस्थित ज्ञान है वहां दर्शनशास्त्र पूर्ण व्यवस्थित ज्ञान है।'
विज्ञान सत्य की ओर ले जाने वाली अनुमानों की श्रृंखला है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त निर्णय और रहस्य अंतिम सत्य तथा निरपेक्ष सत्य हैं, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत नये संशोधनों के अनुसंधान में परिवर्तन अवश्य मांगता है और नया कोई भी अनुसंधान पूर्ववर्ती सिद्धांत को असत्य करार देता है।
न्यूटन का नियतवाद (Determination), देकार्त की उपचयवादी अवधारणा के आधार पर विज्ञान ने काफी प्रगति की किन्तु नई भौतिकी के उदय के साथ ही उनकी अवधारणाओं पर मानो ग्रहण लग गया। यूक्लिड की ज्यामिति, डार्विन का विकासवाद (Evolution) भी संदेह के घेरे में हैं। विज्ञान का इतिहास इसका साक्ष्य है कि उसके प्रतिपृष्ठ पर वैज्ञानिकों के निर्णय बदलते हुए नजर आते हैं। विज्ञान में अंतिम सत्य कुछ भी नहीं।
दर्शन का सम्बन्ध भौतिकता से नहीं। उसका लक्ष्य है- ज्ञान की खोज, मूल्यों की पहचान, संप्रत्ययों का सजगता से तार्किक विश्लेषण करना, वर्तमान विश्व को जिसकी अपेक्षा है।
विज्ञान और दर्शन की धाराएं कहीं अति निकटता से गुजर रही हैं तो कहीं दूरी से। जहां दूरी है उसे पाटने का कार्य किया है-वी.रसेल, ए.एन. वाइटहेड, आत्मा की दार्शनिक पृष्ठभूमि : अस्तित्व का मूल्यांकन