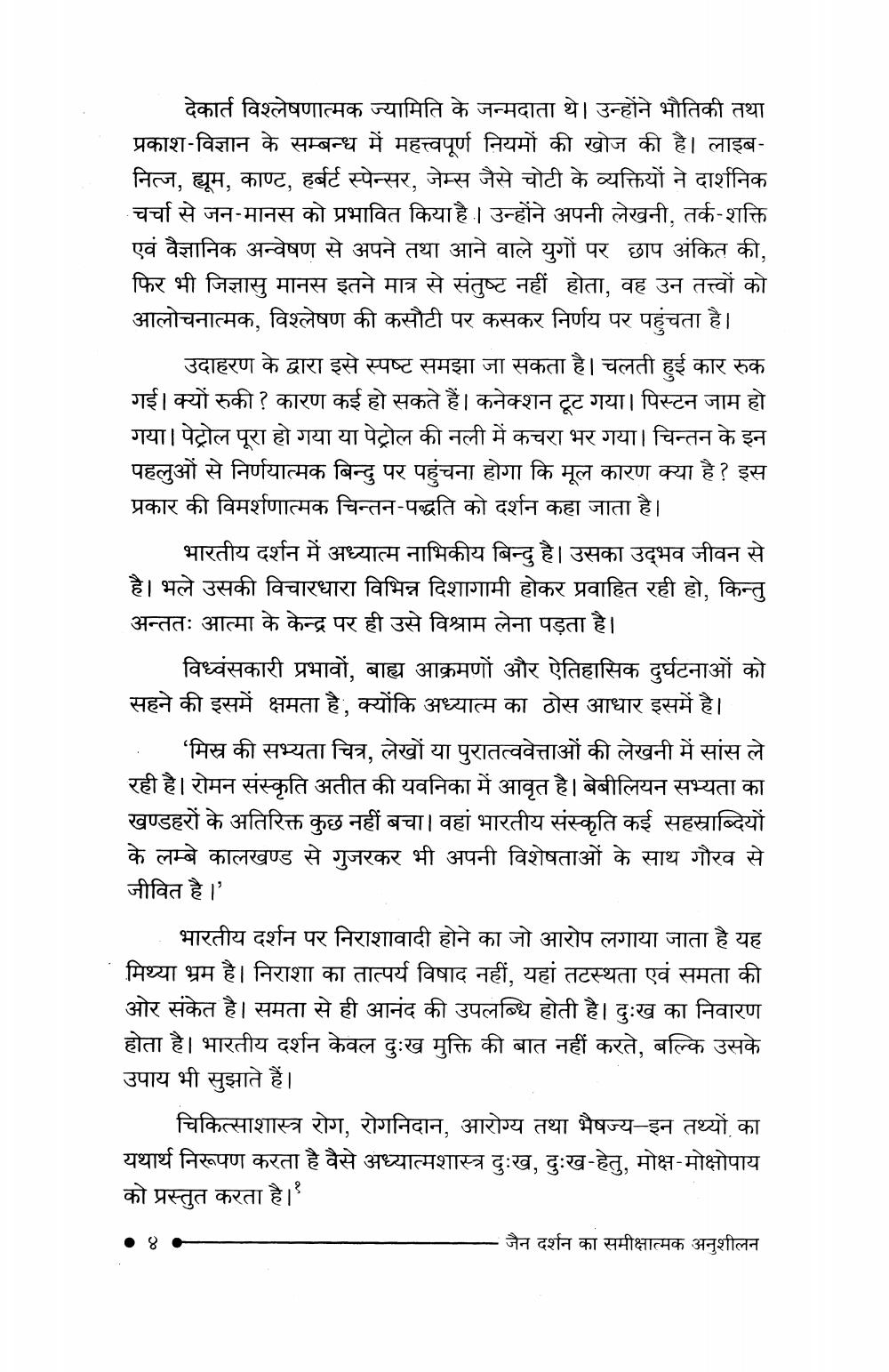________________
देकार्त विश्लेषणात्मक ज्यामिति के जन्मदाता थे। उन्होंने भौतिकी तथा प्रकाश-विज्ञान के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियमों की खोज की है। लाइबनित्ज, ह्यूम, काण्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, जेम्स जैसे चोटी के व्यक्तियों ने दार्शनिक चर्चा से जन-मानस को प्रभावित किया है । उन्होंने अपनी लेखनी, तर्क-शक्ति एवं वैज्ञानिक अन्वेषण से अपने तथा आने वाले युगों पर छाप अंकित की, फिर भी जिज्ञासु मानस इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता, वह उन तत्त्वों को आलोचनात्मक, विश्लेषण की कसौटी पर कसकर निर्णय पर पहुंचता है।
उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। चलती हुई कार रुक गई। क्यों रुकी ? कारण कई हो सकते हैं। कनेक्शन टूट गया। पिस्टन जाम हो गया। पेट्रोल पूरा हो गया या पेट्रोल की नली में कचरा भर गया। चिन्तन के इन पहलुओं से निर्णयात्मक बिन्दु पर पहुंचना होगा कि मूल कारण क्या है ? इस प्रकार की विमर्शणात्मक चिन्तन-पद्धति को दर्शन कहा जाता है।
भारतीय दर्शन में अध्यात्म नाभिकीय बिन्दु है। उसका उद्भव जीवन से है। भले उसकी विचारधारा विभिन्न दिशागामी होकर प्रवाहित रही हो, किन्तु अन्ततः आत्मा के केन्द्र पर ही उसे विश्राम लेना पड़ता है।
विध्वंसकारी प्रभावों, बाह्य आक्रमणों और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं को सहने की इसमें क्षमता है, क्योंकि अध्यात्म का ठोस आधार इसमें है।
'मिस्र की सभ्यता चित्र, लेखों या पुरातत्ववेत्ताओं की लेखनी में सांस ले रही है। रोमन संस्कृति अतीत की यवनिका में आवृत है। बेबीलियन सभ्यता का खण्डहरों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। वहां भारतीय संस्कृति कई सहस्राब्दियों के लम्बे कालखण्ड से गुजरकर भी अपनी विशेषताओं के साथ गौरव से जीवित है।'
भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का जो आरोप लगाया जाता है यह मिथ्या भ्रम है। निराशा का तात्पर्य विषाद नहीं, यहां तटस्थता एवं समता की
ओर संकेत है। समता से ही आनंद की उपलब्धि होती है। दुःख का निवारण होता है। भारतीय दर्शन केवल दुःख मुक्ति की बात नहीं करते, बल्कि उसके उपाय भी सुझाते हैं।
चिकित्साशास्त्र रोग, रोगनिदान, आरोग्य तथा भैषज्य-इन तथ्यों का यथार्थ निरूपण करता है वैसे अध्यात्मशास्त्र दुःख, दुःख-हेतु, मोक्ष-मोक्षोपाय को प्रस्तुत करता है।
- जैन दर्शन का समीक्षात्मक अनुशीलन