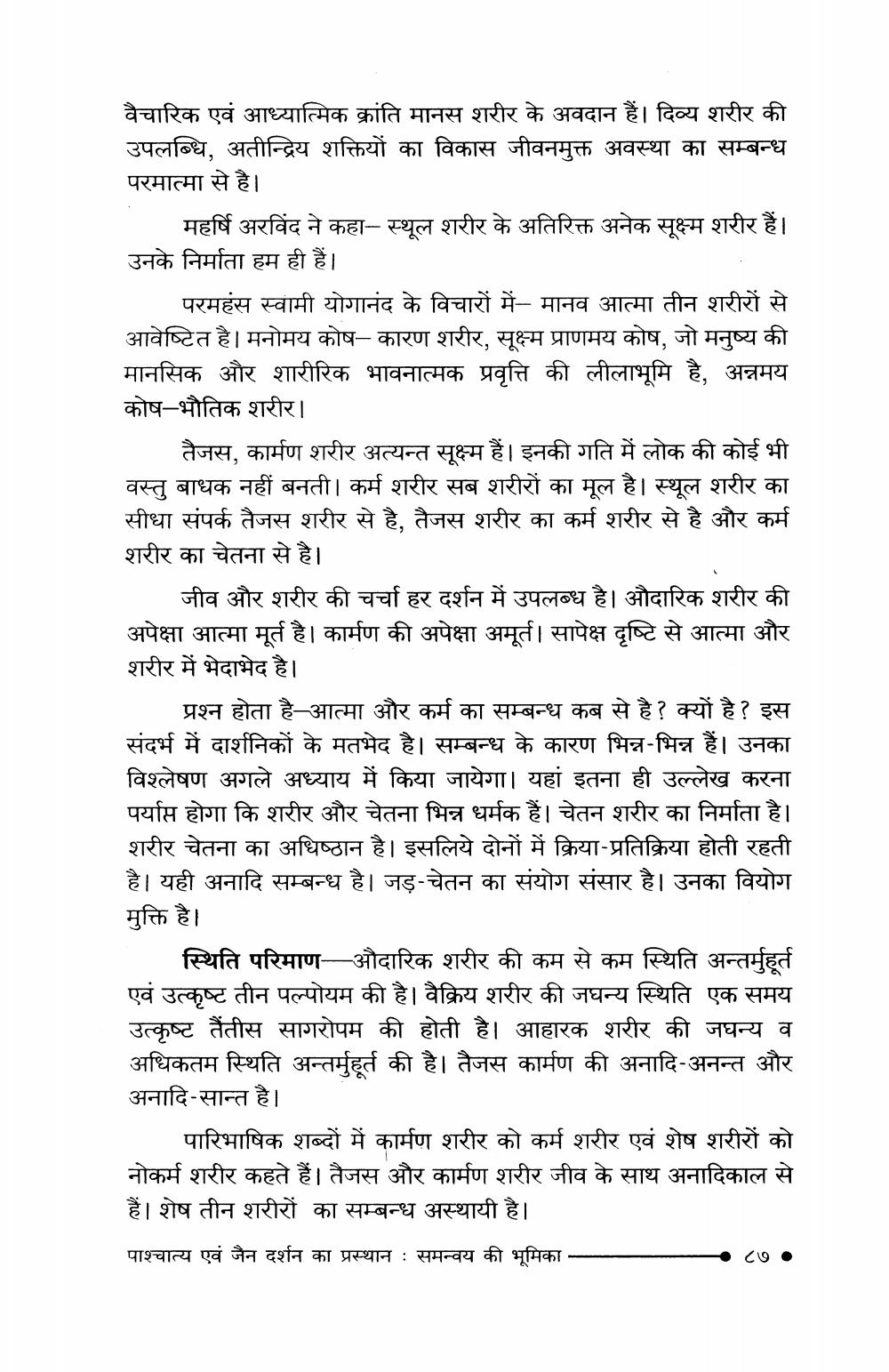________________
वैचारिक एवं आध्यात्मिक क्रांति मानस शरीर के अवदान हैं। दिव्य शरीर की उपलब्धि, अतीन्द्रिय शक्तियों का विकास जीवनमुक्त अवस्था का सम्बन्ध परमात्मा से है।
महर्षि अरविंद ने कहा- स्थूल शरीर के अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म शरीर हैं। उनके निर्माता हम ही हैं ।
परमहंस स्वामी योगानंद के विचारों में- मानव आत्मा तीन शरीरों से आवेष्टित है। मनोमय कोष – कारण शरीर, सूक्ष्म प्राणमय कोष, जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक भावनात्मक प्रवृत्ति की लीलाभूमि है, अन्नमय कोष - भौतिक शरीर ।
तैजस, कार्मण शरीर अत्यन्त सूक्ष्म हैं। इनकी गति में लोक की कोई भी वस्तु बाधक नहीं बनती। कर्म शरीर सब शरीरों का मूल है। स्थूल शरीर का सीधा संपर्क तैजस शरीर से है, तैजस शरीर का कर्म शरीर से है और कर्म शरीर का चेतना से है।
जीव और शरीर की चर्चा हर दर्शन में उपलब्ध है। औदारिक शरीर की अपेक्षा आत्मा मूर्त है । कार्मण की अपेक्षा अमूर्त । सापेक्ष दृष्टि से आत्मा और शरीर में भेदाभेद है ।
प्रश्न होता है- आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कब से है ? क्यों है ? इस संदर्भ में दार्शनिकों के मतभेद है । सम्बन्ध के कारण भिन्न-भिन्न हैं। उनका विश्लेषण अगले अध्याय में किया जायेगा। यहां इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि शरीर और चेतना भिन्न धर्मक हैं। चेतन शरीर का निर्माता है । शरीर चेतना का अधिष्ठान है। इसलिये दोनों में क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है । यही अनादि सम्बन्ध है। जड़-चेतन का संयोग संसार है। उनका वियोग मुक्ति है।
स्थिति परिमाण—औदारिक शरीर की कम से कम स्थिति अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट तीन पल्पोयम की है। वैक्रिय शरीर की जघन्य स्थिति एक समय उत्कृष्ट तैंतीस सागरोपम की होती है। आहारक शरीर की जघन्य व अधिकतम स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है । तैजस कार्मण की अनादि - अनन्त और अनादि- सान्त है।
पारिभाषिक शब्दों में कार्मण शरीर को कर्म शरीर एवं शेष शरीरों को कर्म शरीर कहते हैं । तैजस और कार्मण शरीर जीव के साथ अनादिकाल से हैं। शेष तीन शरीरों का सम्बन्ध अस्थायी है।
पाश्चात्य एवं जैन दर्शन का प्रस्थान समन्वय की भूमिका
८७.