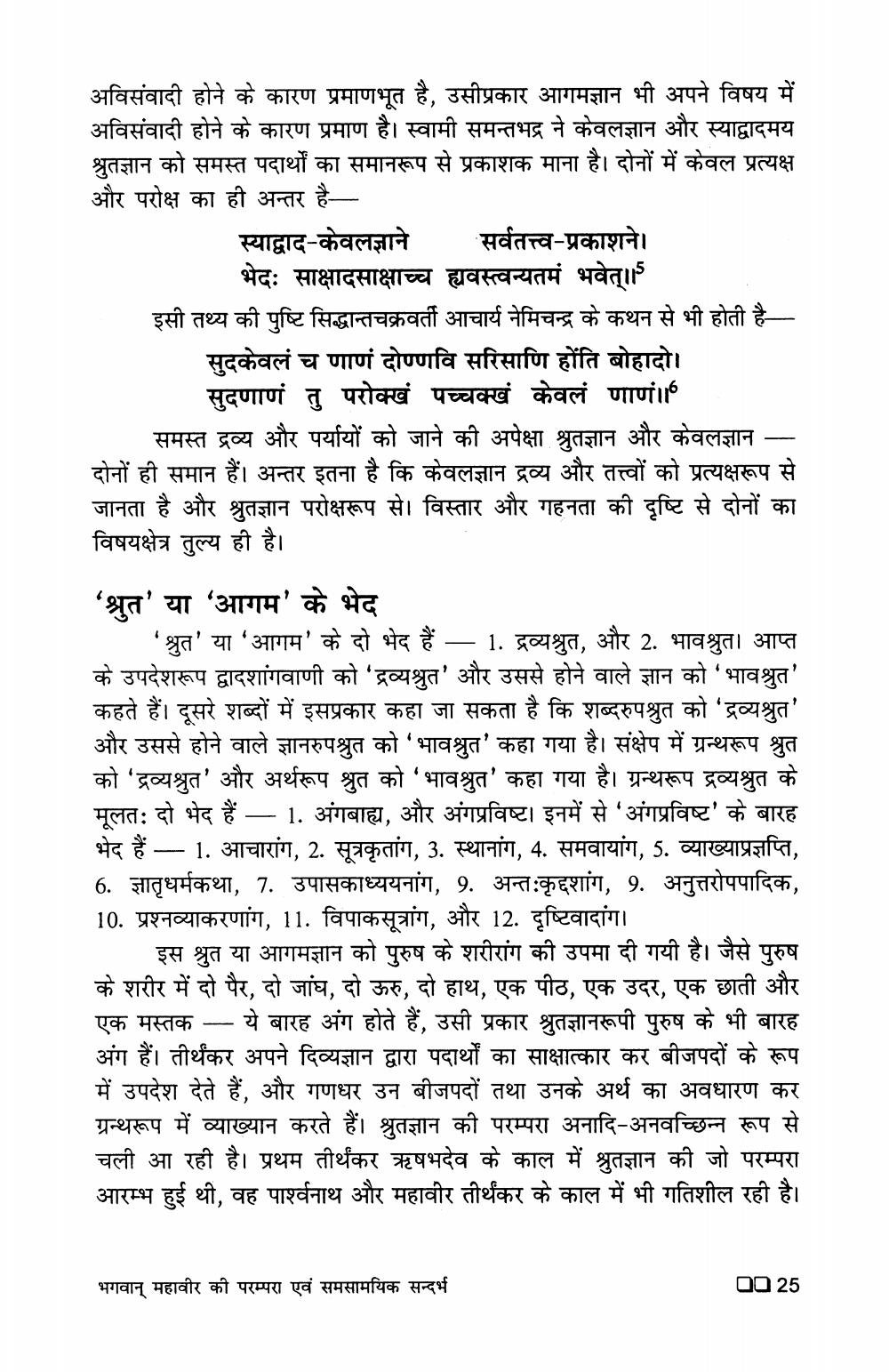________________
अविसंवादी होने के कारण प्रमाणभूत है, उसीप्रकार आगमज्ञान भी अपने विषय में अविसंवादी होने के कारण प्रमाण है। स्वामी समन्तभद्र ने केवलज्ञान और स्याद्वादमय श्रुतज्ञान को समस्त पदार्थों का समानरूप से प्रकाशक माना है। दोनों में केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अन्तर है—
स्याद्वाद - केवलज्ञाने सर्वतत्त्व - प्रकाशने। भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥
इसी तथ्य की पुष्टि सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र के कथन से भी होती है—
सुदकेवलं च णाणं दोण्णवि सरिसाणि होंति बोहादो । सुदणाणं तु परोक्खं पच्चक्खं केवलं गाणं ॥
समस्त द्रव्य और पर्यायों को जाने की अपेक्षा श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही समान हैं। अन्तर इतना है कि केवलज्ञान द्रव्य और तत्त्वों को प्रत्यक्षरूप से जानता है और श्रुतज्ञान परोक्षरूप से । विस्तार और गहनता की दृष्टि से दोनों का विषयक्षेत्र तुल्य ही है।
'श्रुत' या 'आगम' के भेद
4
'श्रुत' या 'आगम' के दो भेद हैं 1. द्रव्यश्रुत, और 2. भावश्रुत। आप्त के उपदेशरूप द्वादशांगवाणी को 'द्रव्यश्रुत' और उससे होने वाले ज्ञान को ' भावश्रुत' कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसप्रकार कहा जा सकता है कि शब्दरुपश्रुत को 'द्रव्यश्रुत' और उससे होने वाले ज्ञानरुपश्रुत को 'भावश्रुत' कहा गया है। संक्षेप में ग्रन्थरूप श्रुत को 'द्रव्यश्रुत' और अर्थरूप श्रुत को 'भावश्रुत' कहा गया है। ग्रन्थरूप द्रव्यश्रुत के मूलत: दो भेद हैं 1. अंगबाह्य, और अंगप्रविष्ट । इनमें से 'अंगप्रविष्ट' के बारह भेद हैं 1. आचारांग, 2. सूत्रकृतांग, 3. स्थानांग, 4. समवायांग, 5. व्याख्याप्रज्ञप्ति, 6. ज्ञातृधर्मकथा, 7. उपासकाध्ययनांग, 9. अन्तःकृद्दशांग, 9. अनुत्तरोपपादिक, 10. प्रश्नव्याकरणांग, 11. विपाकसूत्रांग, और 12. दृष्टिवादांग।
इस श्रुत या आगमज्ञान को पुरुष के शरीरांग की उपमा दी गयी है। जैसे पुरुष के शरीर में दो पैर, दो जांघ, दो ऊरु, दो हाथ, एक पीठ, एक उदर, एक छाती और एक मस्तक ये बारह अंग होते हैं, उसी प्रकार श्रुतज्ञानरूपी पुरुष के भी बारह अंग हैं। तीर्थंकर अपने दिव्यज्ञान द्वारा पदार्थों का साक्षात्कार कर बीजपदों के रूप में उपदेश देते हैं, और गणधर उन बीजपदों तथा उनके अर्थ का अवधारण कर ग्रन्थरूप में व्याख्यान करते हैं। श्रुतज्ञान की परम्परा अनादि - अनवच्छिन्न रूप से चली आ रही है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के काल में श्रुतज्ञान की जो परम्परा आरम्भ हुई थी, वह पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकर के काल में भी गतिशील रही है।
-
भगवान् महावीर की परम्परा एवं समसामयिक सन्दर्भ
00 25