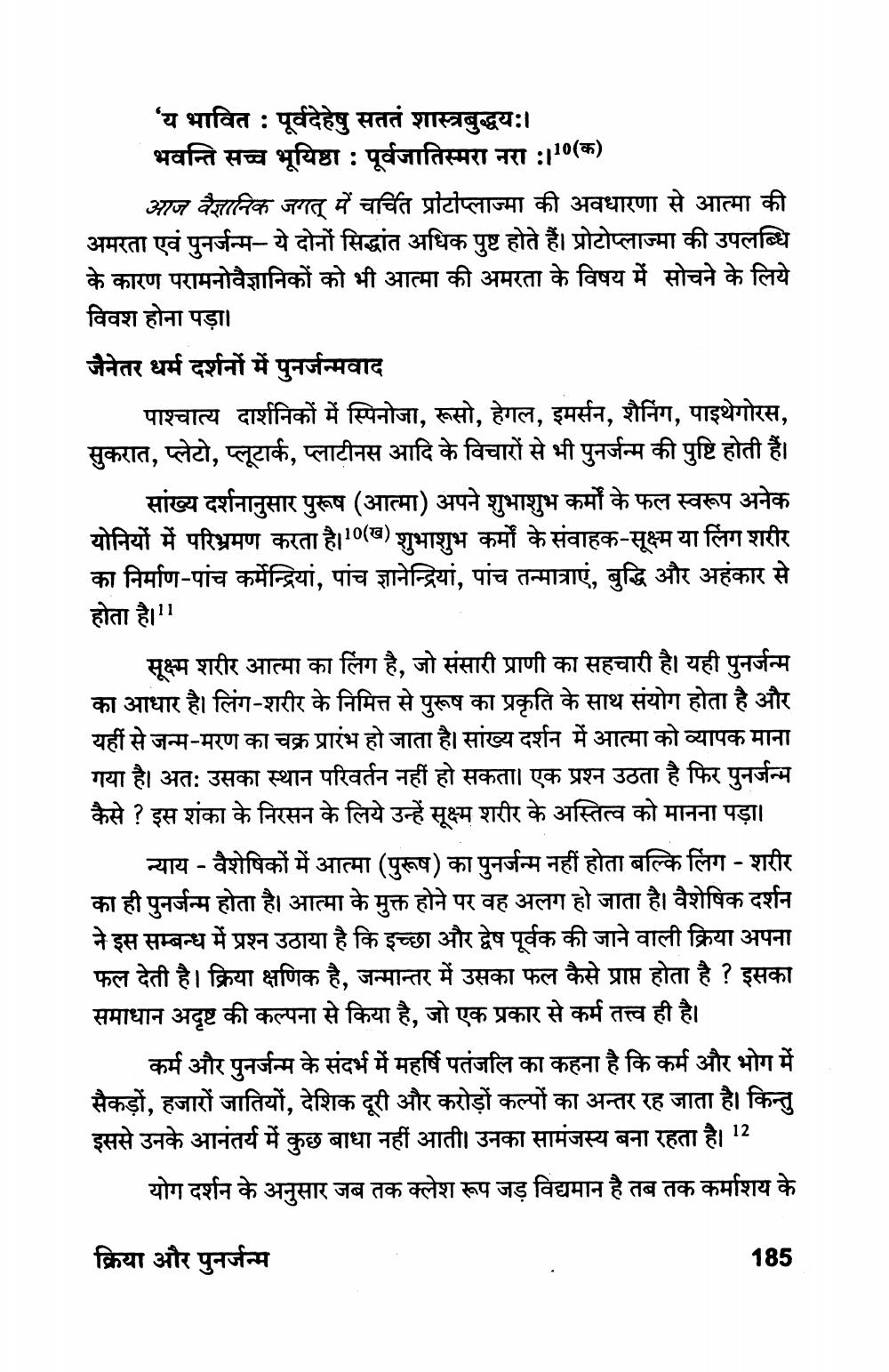________________
'य भावित : पूर्वदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः।
भवन्ति सच्च भूयिष्ठा : पूर्वजातिस्मरा नरा : 1 10 (क)
आज वैज्ञानिक जगत् में चर्चित प्रोटोप्लाज्मा की अवधारणा से आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म - ये दोनों सिद्धांत अधिक पुष्ट होते हैं। प्रोटोप्लाज्मा की उपलब्धि के कारण परामनोवैज्ञानिकों को भी आत्मा की अमरता के विषय में सोचने के लिये विवश होना पड़ा।
जैनेतर धर्म दर्शनों में पुनर्जन्मवाद
पाश्चात्य दार्शनिकों में स्पिनोजा, रूसो, हेगल, इमर्सन, शैनिंग, पाइथेगोरस, सुकरात, प्लेटो, प्लूटार्क, प्लाटीनस आदि के विचारों से भी पुनर्जन्म की पुष्टि होती हैं। सांख्य दर्शनानुसार पुरूष (आत्मा) अपने शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है। 10(ख). शुभाशुभ कर्मों के संवाहक-सूक्ष्म या लिंग शरीर का निर्माण - पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच तन्मात्राएं, बुद्धि और अहंकार से होता है। 11
सूक्ष्म शरीर आत्मा का लिंग है, जो संसारी प्राणी का सहचारी है। यही पुनर्जन्म का आधार है। लिंग- शरीर के निमित्त से पुरूष का प्रकृति के साथ संयोग होता है और यहीं से जन्म-मरण का चक्र प्रारंभ हो जाता है। सांख्य दर्शन में आत्मा को व्यापक माना गया है। अत: उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता। एक प्रश्न उठता है फिर पुनर्जन्म कैसे ? इस शंका के निरसन के लिये उन्हें सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को मानना पड़ा।
न्याय - वैशेषिकों में आत्मा (पुरूष) का पुनर्जन्म नहीं होता बल्कि लिंग - शरीर काही पुनर्जन्म होता है। आत्मा के मुक्त होने पर वह अलग हो जाता है। वैशेषिक दर्शन ने इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है कि इच्छा और द्वेष पूर्वक की जाने वाली क्रिया अपना फल देती है। क्रिया क्षणिक है, जन्मान्तर में उसका फल कैसे प्राप्त होता है ? इसका समाधान अदृष्ट की कल्पना से किया है, जो एक प्रकार से कर्म तत्त्व ही है।
कर्म और पुनर्जन्म के संदर्भ में महर्षि पतंजलि का कहना है कि कर्म और भोग में सैकड़ों, हजारों जातियों, देशिक दूरी और करोड़ों कल्पों का अन्तर रह जाता है। किन्तु इससे उनके आनंतर्य में कुछ बाधा नहीं आती। उनका सामंजस्य बना रहता है। 12
योग दर्शन के अनुसार जब तक क्लेश रूप जड़ विद्यमान है तब तक कर्माशय के क्रिया और पुनर्जन्म
185