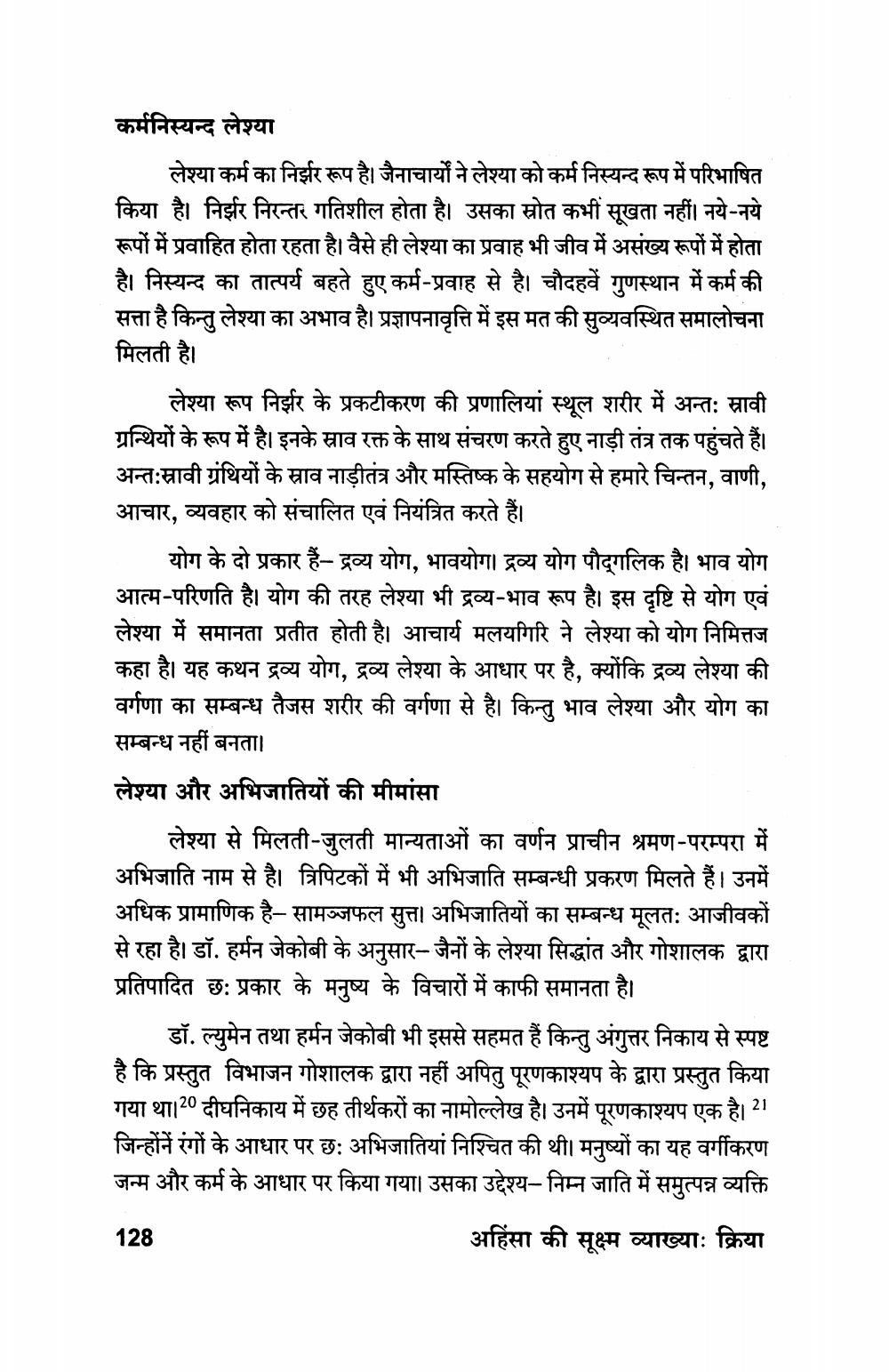________________
कर्मनिस्यन्द लेश्या __लेश्या कर्म का निर्झर रूप है। जैनाचार्यों ने लेश्या को कर्म निस्यन्द रूप में परिभाषित किया है। निर्झर निरन्तर गतिशील होता है। उसका स्रोत कभी सूखता नहीं। नये-नये रूपों में प्रवाहित होता रहता है। वैसे ही लेश्या का प्रवाह भी जीव में असंख्य रूपों में होता है। निस्यन्द का तात्पर्य बहते हुए कर्म-प्रवाह से है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म की सत्ता है किन्तु लेश्या का अभाव है। प्रज्ञापनावृत्ति में इस मत की सुव्यवस्थित समालोचना मिलती है।
लेश्या रूप निर्झर के प्रकटीकरण की प्रणालियां स्थूल शरीर में अन्त: स्रावी ग्रन्थियों के रूप में है। इनके स्राव रक्त के साथ संचरण करते हुए नाड़ी तंत्र तक पहुंचते हैं। अन्तःस्रावी ग्रंथियों के स्राव नाड़ीतंत्र और मस्तिष्क के सहयोग से हमारे चिन्तन, वाणी, आचार, व्यवहार को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं।
योग के दो प्रकार हैं- द्रव्य योग, भावयोग। द्रव्य योग पौद्गलिक है। भाव योग आत्म-परिणति है। योग की तरह लेश्या भी द्रव्य-भाव रूप है। इस दृष्टि से योग एवं लेश्या में समानता प्रतीत होती है। आचार्य मलयगिरि ने लेश्या को योग निमित्तज कहा है। यह कथन द्रव्य योग, द्रव्य लेश्या के आधार पर है, क्योंकि द्रव्य लेश्या की वर्गणा का सम्बन्ध तैजस शरीर की वर्गणा से है। किन्तु भाव लेश्या और योग का सम्बन्ध नहीं बनता। लेश्या और अभिजातियों की मीमांसा
लेश्या से मिलती-जुलती मान्यताओं का वर्णन प्राचीन श्रमण-परम्परा में अभिजाति नाम से है। त्रिपिटकों में भी अभिजाति सम्बन्धी प्रकरण मिलते हैं। उनमें अधिक प्रामाणिक है- सामञ्जफल सुत्त। अभिजातियों का सम्बन्ध मूलतः आजीवकों से रहा है। डॉ. हर्मन जेकोबी के अनुसार-जैनों के लेश्या सिद्धांत और गोशालक द्वारा प्रतिपादित छ: प्रकार के मनुष्य के विचारों में काफी समानता है।
डॉ. ल्युमेन तथा हर्मन जेकोबी भी इससे सहमत हैं किन्तु अंगुत्तर निकाय से स्पष्ट है कि प्रस्तुत विभाजन गोशालक द्वारा नहीं अपितु पूरणकाश्यप के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।20 दीघनिकाय में छह तीर्थकरों का नामोल्लेख है। उनमें पूरणकाश्यप एक है। 21 जिन्होंने रंगों के आधार पर छ: अभिजातियां निश्चित की थी। मनुष्यों का यह वर्गीकरण जन्म और कर्म के आधार पर किया गया। उसका उद्देश्य-निम्न जाति में समुत्पन्न व्यक्ति 128
अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्याः क्रिया