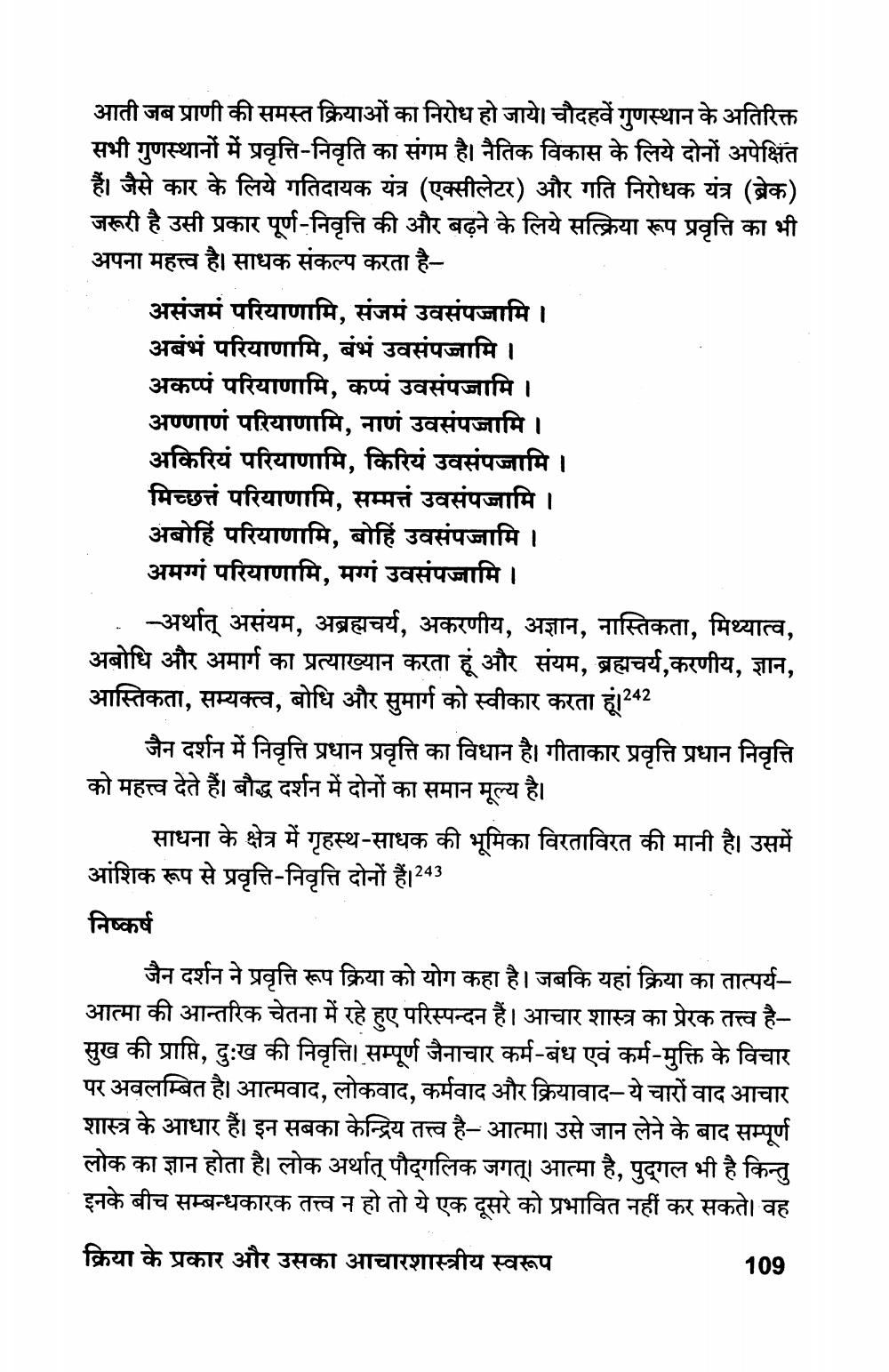________________
आती जब प्राणी की समस्त क्रियाओं का निरोध हो जाये। चौदहवें गुणस्थान के अतिरिक्त सभी गुणस्थानों में प्रवृत्ति-निवृति का संगम है। नैतिक विकास के लिये दोनों अपेक्षित हैं। जैसे कार के लिये गतिदायक यंत्र (एक्सीलेटर) और गति निरोधक यंत्र (ब्रेक) जरूरी है उसी प्रकार पूर्ण-निवृत्ति की और बढ़ने के लिये सत्क्रिया रूप प्रवृत्ति का भी अपना महत्त्व है। साधक संकल्प करता है
असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपजामि । अबंभं परियाणामि, बंभं उवसंपजामि । अकप्पं परियाणामि, कप्पं उवसंपज्जामि । अण्णाणं परियाणामि, नाणं उवसंपजामि । अकिरियं परियाणामि, किरियं उवसंपज्जामि । मिच्छत्तं परियाणामि, सम्मत्तं उवसंपज्जामि । अबोहिं परियाणामि, बोहिं उवसंपज्जामि । अमग्गं परियाणामि, मग्गं उवसंपजामि ।
-अर्थात् असंयम, अब्रह्मचर्य, अकरणीय, अज्ञान, नास्तिकता, मिथ्यात्व, अबोधि और अमार्ग का प्रत्याख्यान करता हूं और संयम, ब्रह्मचर्य,करणीय, ज्ञान, आस्तिकता, सम्यक्त्व, बोधि और सुमार्ग को स्वीकार करता हूं।242
जैन दर्शन में निवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति का विधान है। गीताकार प्रवृत्ति प्रधान निवृत्ति को महत्त्व देते हैं। बौद्ध दर्शन में दोनों का समान मूल्य है।
साधना के क्षेत्र में गृहस्थ-साधक की भूमिका विरताविरत की मानी है। उसमें आंशिक रूप से प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों हैं।243 निष्कर्ष
जैन दर्शन ने प्रवृत्ति रूप क्रिया को योग कहा है। जबकि यहां क्रिया का तात्पर्यआत्मा की आन्तरिक चेतना में रहे हुए परिस्पन्दन हैं। आचार शास्त्र का प्रेरक तत्त्व हैसुख की प्राप्ति, दुःख की निवृत्ति। सम्पूर्ण जैनाचार कर्म-बंध एवं कर्म-मुक्ति के विचार पर अवलम्बित है। आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद-ये चारों वाद आचार शास्त्र के आधार हैं। इन सबका केन्द्रिय तत्त्व है- आत्मा। उसे जान लेने के बाद सम्पूर्ण लोक का ज्ञान होता है। लोक अर्थात् पौद्गलिक जगत्। आत्मा है, पुद्गल भी है किन्तु इनके बीच सम्बन्धकारक तत्त्व न हो तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। वह
क्रिया के प्रकार और उसका आचारशास्त्रीय स्वरूप
109