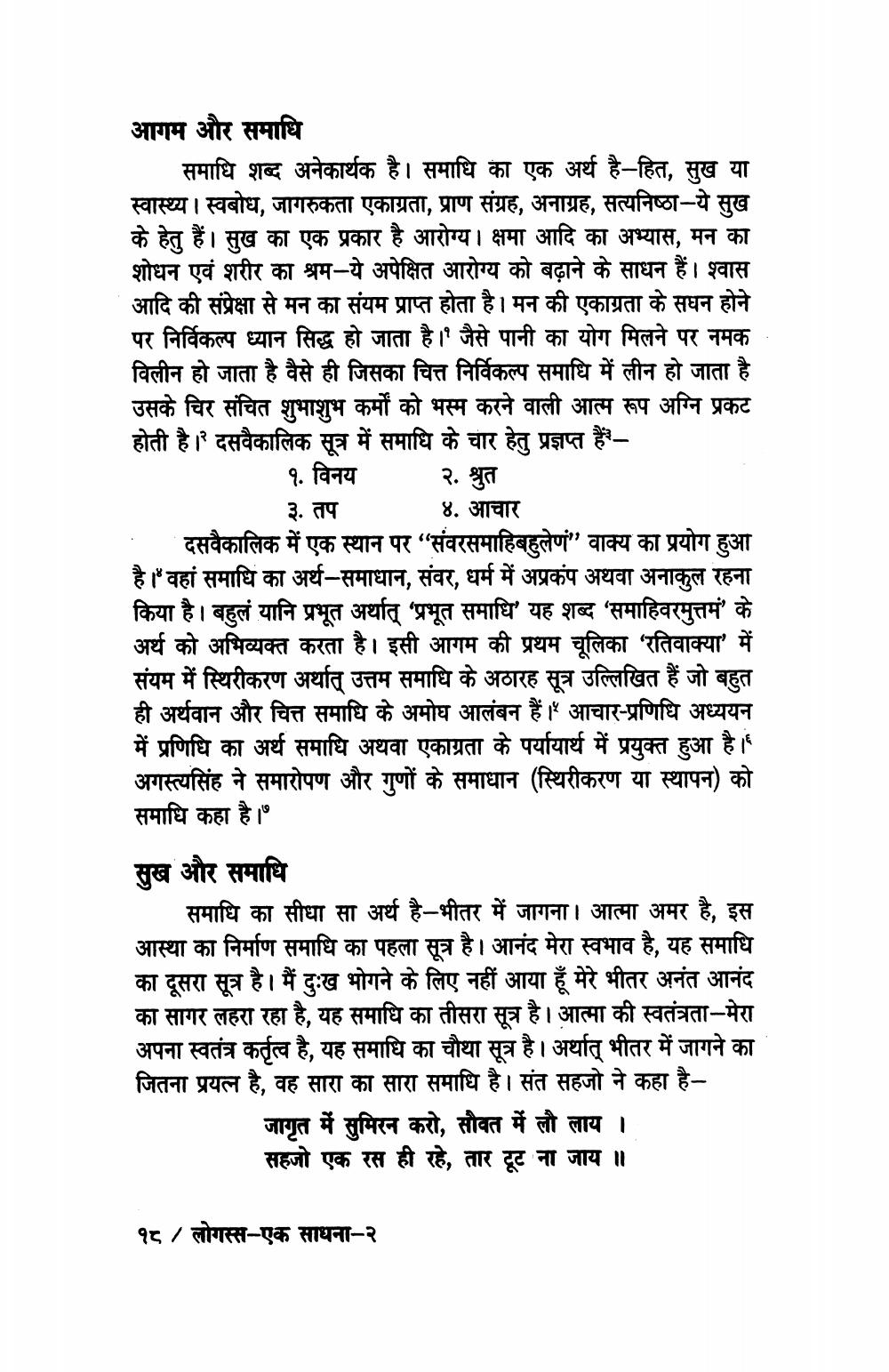________________
आगम और समाधि
समाधि शब्द अनेकार्थक है। समाधि का एक अर्थ है-हित, सुख या स्वास्थ्य। स्वबोध, जागरुकता एकाग्रता, प्राण संग्रह, अनाग्रह, सत्यनिष्ठा-ये सुख के हेतु हैं। सुख का एक प्रकार है आरोग्य। क्षमा आदि का अभ्यास, मन का शोधन एवं शरीर का श्रम-ये अपेक्षित आरोग्य को बढ़ाने के साधन हैं। श्वास आदि की संप्रेक्षा से मन का संयम प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता के सघन होने पर निर्विकल्प ध्यान सिद्ध हो जाता है। जैसे पानी का योग मिलने पर नमक विलीन हो जाता है वैसे ही जिसका चित्त निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है उसके चिर संचित शुभाशुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्म रूप अग्नि प्रकट होती है। दसवैकालिक सूत्र में समाधि के चार हेतु प्रज्ञप्त हैं
१. विनय २. श्रुत
३. तप ४. आचार - दसवैकालिक में एक स्थान पर “संवरसमाहिबहुलेणं" वाक्य का प्रयोग हुआ है। वहां समाधि का अर्थ-समाधान, संवर, धर्म में अप्रकंप अथवा अनाकुल रहना किया है। बहुलं यानि प्रभूत अर्थात् 'प्रभूत समाधि' यह शब्द 'समाहिवरमुत्तम' के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसी आगम की प्रथम चूलिका ‘रतिवाक्या' में संयम में स्थिरीकरण अर्थात् उत्तम समाधि के अठारह सूत्र उल्लिखित हैं जो बहुत ही अर्थवान और चित्त समाधि के अमोघ आलंबन हैं। आचार-प्रणिधि अध्ययन में प्रणिधि का अर्थ समाधि अथवा एकाग्रता के पर्यायार्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगस्त्यसिंह ने समारोपण और गुणों के समाधान (स्थिरीकरण या स्थापन) को समाधि कहा है।
सुख और समाधि
समाधि का सीधा सा अर्थ है-भीतर में जागना। आत्मा अमर है, इस आस्था का निर्माण समाधि का पहला सूत्र है। आनंद मेरा स्वभाव है, यह समाधि का दूसरा सूत्र है। मैं दुःख भोगने के लिए नहीं आया हूँ मेरे भीतर अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है, यह समाधि का तीसरा सूत्र है। आत्मा की स्वतंत्रता-मेरा अपना स्वतंत्र कर्तृत्व है, यह समाधि का चौथा सूत्र है। अर्थात् भीतर में जागने का जितना प्रयत्न है, वह सारा का सारा समाधि है। संत सहजो ने कहा है
जागृत में सुमिरन करो, सौवत में लौ लाय । सहजो एक रस ही रहे, तार टूट ना जाय ॥
१८ / लोगस्स-एक साधना-२