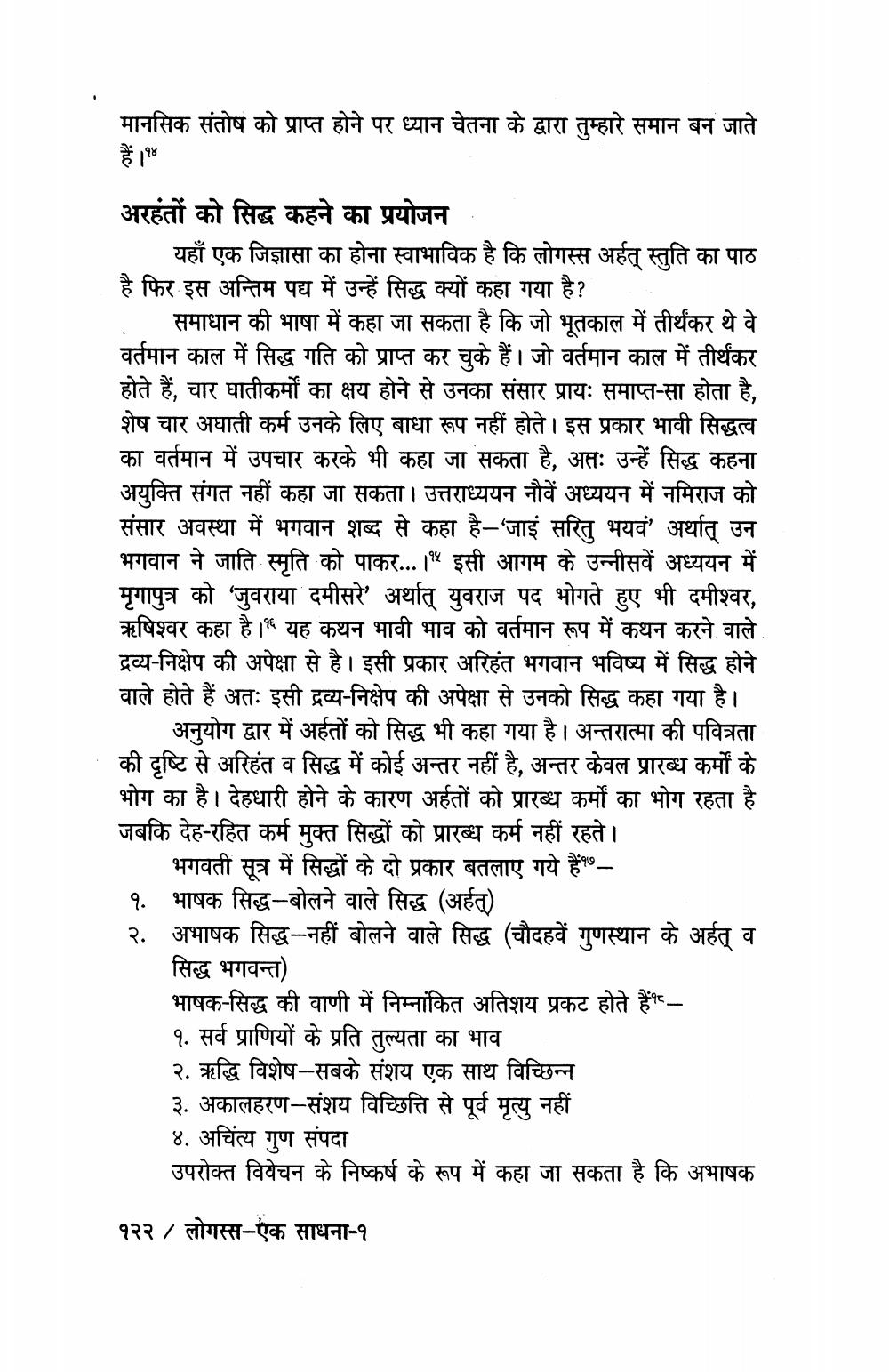________________
मानसिक संतोष को प्राप्त होने पर ध्यान चेतना के द्वारा तुम्हारे समान बन जाते
अरहंतों को सिद्ध कहने का प्रयोजन .
यहाँ एक जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है कि लोगस्स अर्हत् स्तुति का पाठ है फिर इस अन्तिम पद्य में उन्हें सिद्ध क्यों कहा गया है?
समाधान की भाषा में कहा जा सकता है कि जो भूतकाल में तीर्थंकर थे वे वर्तमान काल में सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके हैं। जो वर्तमान काल में तीर्थंकर होते हैं, चार घातीकर्मों का क्षय होने से उनका संसार प्रायः समाप्त-सा होता है, शेष चार अघाती कर्म उनके लिए बाधा रूप नहीं होते। इस प्रकार भावी सिद्धत्व का वर्तमान में उपचार करके भी कहा जा सकता है, अतः उन्हें सिद्ध कहना अयुक्ति संगत नहीं कहा जा सकता। उत्तराध्ययन नौवें अध्ययन में नमिराज को संसार अवस्था में भगवान शब्द से कहा है-'जाइं सरितु भयवं' अर्थात् उन भगवान ने जाति स्मृति को पाकर...।१५ इसी आगम के उन्नीसवें अध्ययन में मृगापुत्र को 'जुवराया दमीसरे' अर्थात् युवराज पद भोगते हुए भी दमीश्वर, ऋषिश्वर कहा है।१६ यह कथन भावी भाव को वर्तमान रूप में कथन करने वाले द्रव्य-निक्षेप की अपेक्षा से है। इसी प्रकार अरिहंत भगवान भविष्य में सिद्ध होने वाले होते हैं अतः इसी द्रव्य-निक्षेप की अपेक्षा से उनको सिद्ध कहा गया है।
अनुयोग द्वार में अर्हतों को सिद्ध भी कहा गया है। अन्तरात्मा की पवित्रता की दृष्टि से अरिहंत व सिद्ध में कोई अन्तर नहीं है, अन्तर केवल प्रारब्ध कर्मों के भोग का है। देहधारी होने के कारण अर्हतों को प्रारब्ध कर्मों का भोग रहता है जबकि देह-रहित कर्म मुक्त सिद्धों को प्रारब्ध कर्म नहीं रहते।
भगवती सूत्र में सिद्धों के दो प्रकार बतलाए गये हैं१. भाषक सिद्ध-बोलने वाले सिद्ध (अर्हत्) __ अभाषक सिद्ध-नहीं बोलने वाले सिद्ध (चौदहवें गुणस्थान के अर्हत् व सिद्ध भगवन्त) भाषक-सिद्ध की वाणी में निम्नांकित अतिशय प्रकट होते हैं। १. सर्व प्राणियों के प्रति तुल्यता का भाव २. ऋद्धि विशेष-सबके संशय एक साथ विच्छिन्न ३. अकालहरण-संशय विच्छित्ति से पूर्व मृत्यु नहीं ४. अचिंत्य गुण संपदा उपरोक्त विवेचन के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अभाषक
१२२ / लोगस्स-एक साधना-१