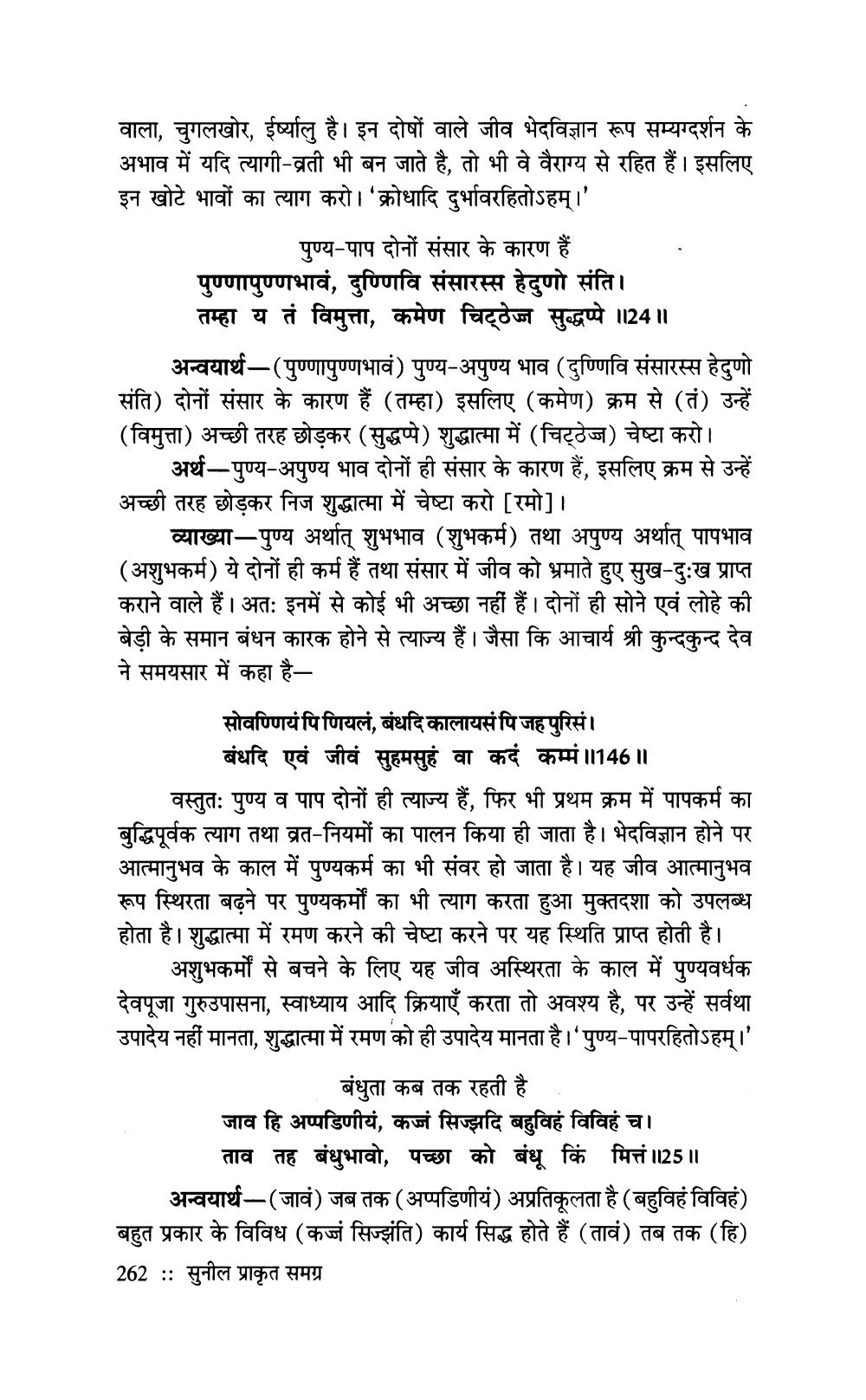________________
वाला, चुगलखोर, ईर्ष्यालु है। इन दोषों वाले जीव भेदविज्ञान रूप सम्यग्दर्शन के अभाव में यदि त्यागी-व्रती भी बन जाते है, तो भी वे वैराग्य से रहित हैं। इसलिए इन खोटे भावों का त्याग करो। 'क्रोधादि दुर्भावरहितोऽहम्।'
__पुण्य-पाप दोनों संसार के कारण हैं पुण्णापुण्णभावं, दुण्णिवि संसारस्स हेदुणो संति। तम्हा य तं विमुत्ता, कमेण चिट्ठेज सुद्धप्पे ॥24॥
अन्वयार्थ-(पुण्णापुण्णभावं) पुण्य-अपुण्य भाव (दुण्णिवि संसारस्स हेदुणो संति) दोनों संसार के कारण हैं (तम्हा) इसलिए (कमेण) क्रम से (तं) उन्हें (विमुत्ता) अच्छी तरह छोड़कर (सुद्धप्पे) शुद्धात्मा में (चिट्टेज) चेष्टा करो।
___ अर्थ-पुण्य-अपुण्य भाव दोनों ही संसार के कारण हैं, इसलिए क्रम से उन्हें अच्छी तरह छोड़कर निज शुद्धात्मा में चेष्टा करो [रमो]।
व्याख्या-पुण्य अर्थात् शुभभाव (शुभकर्म) तथा अपुण्य अर्थात् पापभाव (अशुभकर्म) ये दोनों ही कर्म हैं तथा संसार में जीव को भ्रमाते हुए सुख-दुःख प्राप्त कराने वाले हैं। अतः इनमें से कोई भी अच्छा नहीं हैं। दोनों ही सोने एवं लोहे की बेड़ी के समान बंधन कारक होने से त्याज्य हैं। जैसा कि आचार्य श्री कुन्दकुन्द देव ने समयसार में कहा है
सोवणियं पिणियलं, बंधदि कालायसंपिजहपुरिसं।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं 146॥ वस्तुतः पुण्य व पाप दोनों ही त्याज्य हैं, फिर भी प्रथम क्रम में पापकर्म का बुद्धिपूर्वक त्याग तथा व्रत-नियमों का पालन किया ही जाता है। भेदविज्ञान होने पर आत्मानुभव के काल में पुण्यकर्म का भी संवर हो जाता है। यह जीव आत्मानुभव रूप स्थिरता बढ़ने पर पुण्यकर्मों का भी त्याग करता हुआ मुक्तदशा को उपलब्ध होता है। शुद्धात्मा में रमण करने की चेष्टा करने पर यह स्थिति प्राप्त होती है।
अशुभकर्मों से बचने के लिए यह जीव अस्थिरता के काल में पुण्यवर्धक देवपूजा गुरुउपासना, स्वाध्याय आदि क्रियाएँ करता तो अवश्य है, पर उन्हें सर्वथा उपादेय नहीं मानता, शुद्धात्मा में रमण को ही उपादेय मानता है। 'पुण्य-पापरहितोऽहम्।'
बंधुता कब तक रहती है जाव हि अप्पडिणीयं, कजं सिज्झदि बहुविहं विविहं च।
ताव तह बंधुभावो, पच्छा को बंधू किं मित्तं ॥25॥ अन्वयार्थ-(जावं) जब तक (अप्पडिणीयं) अप्रतिकूलता है (बहुविहं विविहं) बहुत प्रकार के विविध (कजं सिझंति) कार्य सिद्ध होते हैं (तावं) तब तक (हि) 262 :: सुनील प्राकृत समग्र