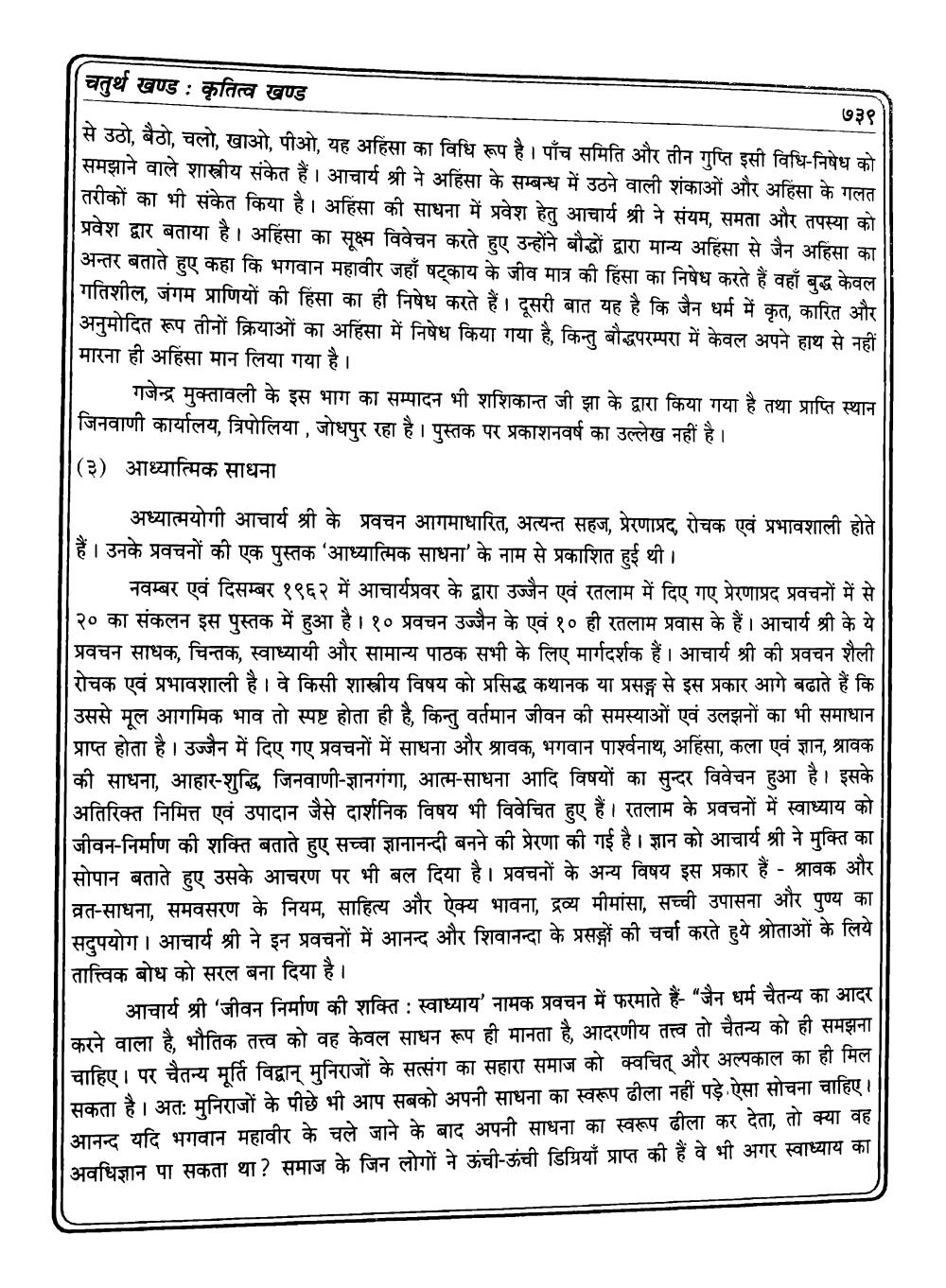________________
(चतुर्थ खण्ड : कृतित्व खण्ड
७३९ से उठो, बैठो, चलो, खाओ, पीओ, यह अहिंसा का विधि रूप है। पाँच समिति और तीन गुप्ति इसी विधि-निषेध को समझाने वाले शास्त्रीय संकेत हैं। आचार्य श्री ने अहिंसा के सम्बन्ध में उठने वाली शंकाओं और अहिंसा के गलत तरीकों का भी संकेत किया है। अहिंसा की साधना में प्रवेश हेतु आचार्य श्री ने संयम, समता और तपस्या को प्रवेश द्वार बताया है। अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन करते हुए उन्होंने बौद्धों द्वारा मान्य अहिंसा से जैन अहिंसा का अन्तर बताते हुए कहा कि भगवान महावीर जहाँ षट्काय के जीव मात्र की हिंसा का निषेध करते हैं वहाँ बुद्ध केवल गतिशील, जंगम प्राणियों की हिंसा का ही निषेध करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में कृत, कारित और अनुमोदित रूप तीनों क्रियाओं का अहिंसा में निषेध किया गया है, किन्तु बौद्धपरम्परा में केवल अपने हाथ से नहीं | मारना ही अहिंसा मान लिया गया है।
गजेन्द्र मुक्तावली के इस भाग का सम्पादन भी शशिकान्त जी झा के द्वारा किया गया है तथा प्राप्ति स्थान | | जिनवाणी कार्यालय, त्रिपोलिया , जोधपुर रहा है। पुस्तक पर प्रकाशनवर्ष का उल्लेख नहीं है। (३) आध्यात्मिक साधना
अध्यात्मयोगी आचार्य श्री के प्रवचन आगमाधारित, अत्यन्त सहज, प्रेरणाप्रद, रोचक एवं प्रभावशाली होते | | हैं। उनके प्रवचनों की एक पुस्तक 'आध्यात्मिक साधना' के नाम से प्रकाशित हुई थी।
नवम्बर एवं दिसम्बर १९६२ में आचार्यप्रवर के द्वारा उज्जैन एवं रतलाम में दिए गए प्रेरणाप्रद प्रवचनों में से | २० का संकलन इस पुस्तक में हुआ है। १० प्रवचन उज्जैन के एवं १० ही रतलाम प्रवास के हैं। आचार्य श्री के ये | प्रवचन साधक, चिन्तक, स्वाध्यायी और सामान्य पाठक सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। आचार्य श्री की प्रवचन शैली रोचक एवं प्रभावशाली है। वे किसी शास्त्रीय विषय को प्रसिद्ध कथानक या प्रसङ्ग से इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि उससे मूल आगमिक भाव तो स्पष्ट होता ही है, किन्तु वर्तमान जीवन की समस्याओं एवं उलझनों का भी समाधान प्राप्त होता है। उज्जैन में दिए गए प्रवचनों में साधना और श्रावक, भगवान पार्श्वनाथ, अहिंसा, कला एवं ज्ञान, श्रावक की साधना, आहार-शुद्धि, जिनवाणी-ज्ञानगंगा, आत्म-साधना आदि विषयों का सुन्दर विवेचन हुआ है। इसके अतिरिक्त निमित्त एवं उपादान जैसे दार्शनिक विषय भी विवेचित हुए हैं। रतलाम के प्रवचनों में स्वाध्याय को जीवन-निर्माण की शक्ति बताते हुए सच्चा ज्ञानानन्दी बनने की प्रेरणा की गई है। ज्ञान को आचार्य श्री ने मुक्ति का सोपान बताते हुए उसके आचरण पर भी बल दिया है। प्रवचनों के अन्य विषय इस प्रकार हैं - श्रावक और व्रत-साधना, समवसरण के नियम, साहित्य और ऐक्य भावना, द्रव्य मीमांसा, सच्ची उपासना और पुण्य का सदुपयोग। आचार्य श्री ने इन प्रवचनों में आनन्द और शिवानन्दा के प्रसङ्गों की चर्चा करते हुये श्रोताओं के लिये तात्त्विक बोध को सरल बना दिया है।
आचार्य श्री 'जीवन निर्माण की शक्ति : स्वाध्याय' नामक प्रवचन में फरमाते हैं- “जैन धर्म चैतन्य का आदर करने वाला है, भौतिक तत्त्व को वह केवल साधन रूप ही मानता है, आदरणीय तत्त्व तो चैतन्य को ही समझना चाहिए। पर चैतन्य मूर्ति विद्वान् मुनिराजों के सत्संग का सहारा समाज को क्वचित् और अल्पकाल का ही मिल सकता है। अत: मुनिराजों के पीछे भी आप सबको अपनी साधना का स्वरूप ढीला नहीं पड़े ऐसा सोचना चाहिए। आनन्द यदि भगवान महावीर के चले जाने के बाद अपनी साधना का स्वरूप ढीला कर देता, तो क्या वह अवधिज्ञान पा सकता था? समाज के जिन लोगों ने ऊंची-ऊंची डिग्रियाँ प्राप्त की हैं वे भी अगर स्वाध्याय का