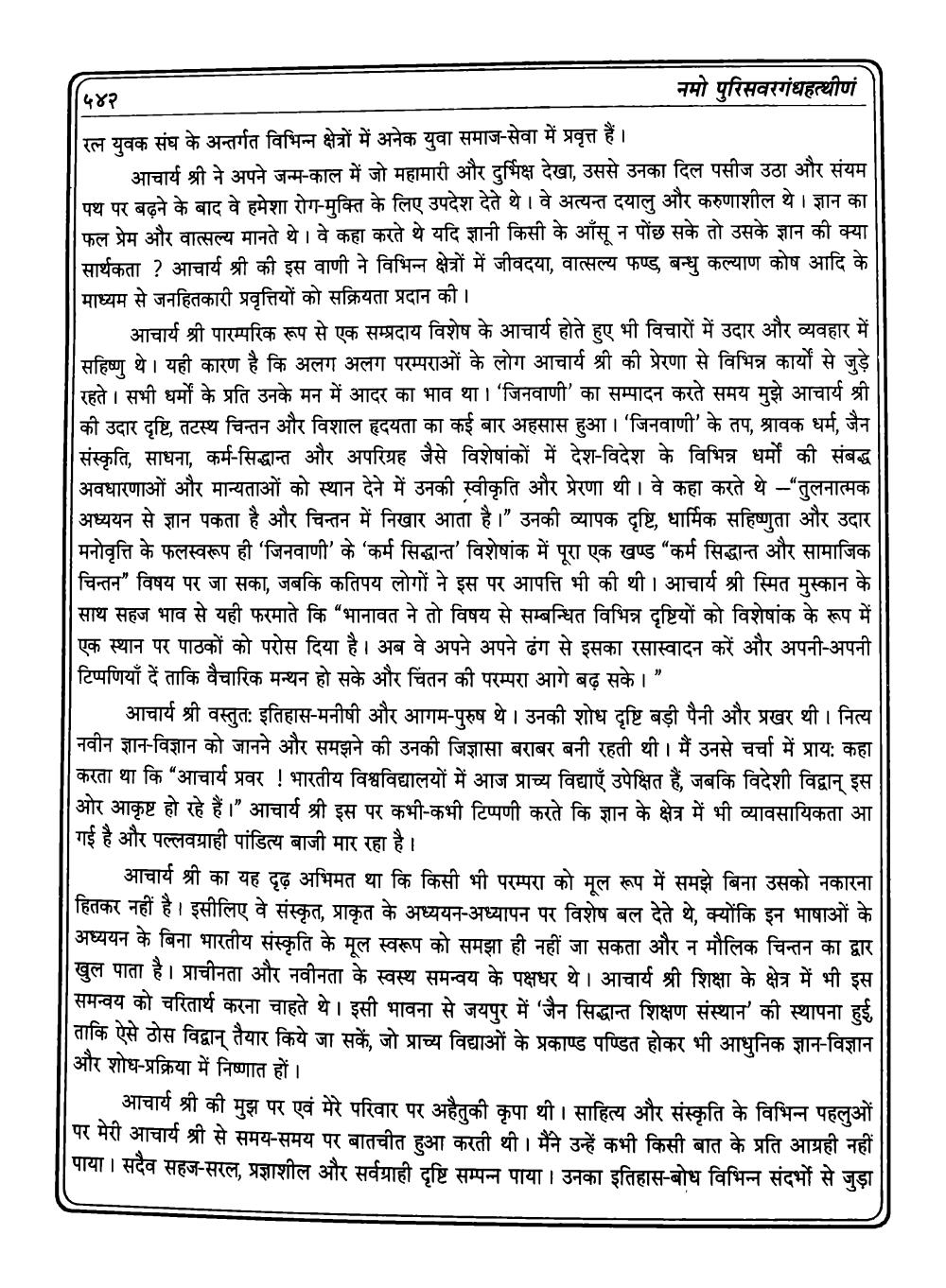________________
(६४२
नमो पुरिसवरगंधहत्थीणं
रत्न युवक संघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक युवा समाज-सेवा में प्रवृत्त हैं।
आचार्य श्री ने अपने जन्म-काल में जो महामारी और दुर्भिक्ष देखा, उससे उनका दिल पसीज उठा और संयम पथ पर बढ़ने के बाद वे हमेशा रोग-मुक्ति के लिए उपदेश देते थे। वे अत्यन्त दयालु और करुणाशील थे। ज्ञान का फल प्रेम और वात्सल्य मानते थे। वे कहा करते थे यदि ज्ञानी किसी के आँसू न पोंछ सके तो उसके ज्ञान की क्या सार्थकता ? आचार्य श्री की इस वाणी ने विभिन्न क्षेत्रों में जीवदया, वात्सल्य फण्ड, बन्धु कल्याण कोष आदि के माध्यम से जनहितकारी प्रवृत्तियों को सक्रियता प्रदान की। ___आचार्य श्री पारम्परिक रूप से एक सम्प्रदाय विशेष के आचार्य होते हुए भी विचारों में उदार और व्यवहार में सहिष्णु थे। यही कारण है कि अलग अलग परम्पराओं के लोग आचार्य श्री की प्रेरणा से विभिन्न कार्यों से जुड़े रहते। सभी धर्मों के प्रति उनके मन में आदर का भाव था। 'जिनवाणी' का सम्पादन करते समय मुझे आचार्य श्री की उदार दृष्टि, तटस्थ चिन्तन और विशाल हृदयता का कई बार अहसास हुआ। 'जिनवाणी' के तप, श्रावक धर्म, जैन संस्कृति, साधना, कर्म-सिद्धान्त और अपरिग्रह जैसे विशेषांकों में देश-विदेश के विभिन्न धर्मों की संबद्ध अवधारणाओं और मान्यताओं को स्थान देने में उनकी स्वीकृति और प्रेरणा थी। वे कहा करते थे –“तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञान पकता है और चिन्तन में निखार आता है।" उनकी व्यापक दृष्टि, धार्मिक सहिष्णुता और उदार मनोवृत्ति के फलस्वरूप ही 'जिनवाणी' के 'कर्म सिद्धान्त' विशेषांक में पूरा एक खण्ड “कर्म सिद्धान्त और सामाजिक चिन्तन” विषय पर जा सका, जबकि कतिपय लोगों ने इस पर आपत्ति भी की थी। आचार्य श्री स्मित मुस्कान के साथ सहज भाव से यही फरमाते कि “भानावत ने तो विषय से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टियों को विशेषांक के रूप में एक स्थान पर पाठकों को परोस दिया है। अब वे अपने अपने ढंग से इसका रसास्वादन करें और अपनी-अपनी टिप्पणियाँ दें ताकि वैचारिक मन्थन हो सके और चिंतन की परम्परा आगे बढ़ सके।”
आचार्य श्री वस्तुत: इतिहास-मनीषी और आगम-पुरुष थे। उनकी शोध दृष्टि बड़ी पैनी और प्रखर थी। नित्य नवीन ज्ञान-विज्ञान को जानने और समझने की उनकी जिज्ञासा बराबर बनी रहती थी। मैं उनसे चर्चा में प्राय: कहा करता था कि “आचार्य प्रवर ! भारतीय विश्वविद्यालयों में आज प्राच्य विद्याएँ उपेक्षित हैं, जबकि विदेशी विद्वान् इस
ओर आकृष्ट हो रहे हैं।” आचार्य श्री इस पर कभी-कभी टिप्पणी करते कि ज्ञान के क्षेत्र में भी व्यावसायिकता आ गई है और पल्लवग्राही पांडित्य बाजी मार रहा है।
आचार्य श्री का यह दृढ़ अभिमत था कि किसी भी परम्परा को मूल रूप में समझे बिना उसको नकारना | हितकर नहीं है। इसीलिए वे संस्कृत, प्राकृत के अध्ययन-अध्यापन पर विशेष बल देते थे, क्योंकि इन भाषाओं के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझा ही नहीं जा सकता और न मौलिक चिन्तन का द्वार खुल पाता है। प्राचीनता और नवीनता के स्वस्थ समन्वय के पक्षधर थे। आचार्य श्री शिक्षा के क्षेत्र में भी इस समन्वय को चरितार्थ करना चाहते थे। इसी भावना से जयपुर में 'जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान' की स्थापना हुई, ताकि ऐसे ठोस विद्वान् तैयार किये जा सकें, जो प्राच्य विद्याओं के प्रकाण्ड पण्डित होकर भी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और शोध-प्रक्रिया में निष्णात हों।
आचार्य श्री की मुझ पर एवं मेरे परिवार पर अहैतुकी कृपा थी। साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर मेरी आचार्य श्री से समय-समय पर बातचीत हुआ करती थी। मैंने उन्हें कभी किसी बात के प्रति आग्रही नहीं पाया। सदैव सहज-सरल, प्रज्ञाशील और सर्वग्राही दृष्टि सम्पन्न पाया। उनका इतिहास-बोध विभिन्न संदर्भो से जुड़ा