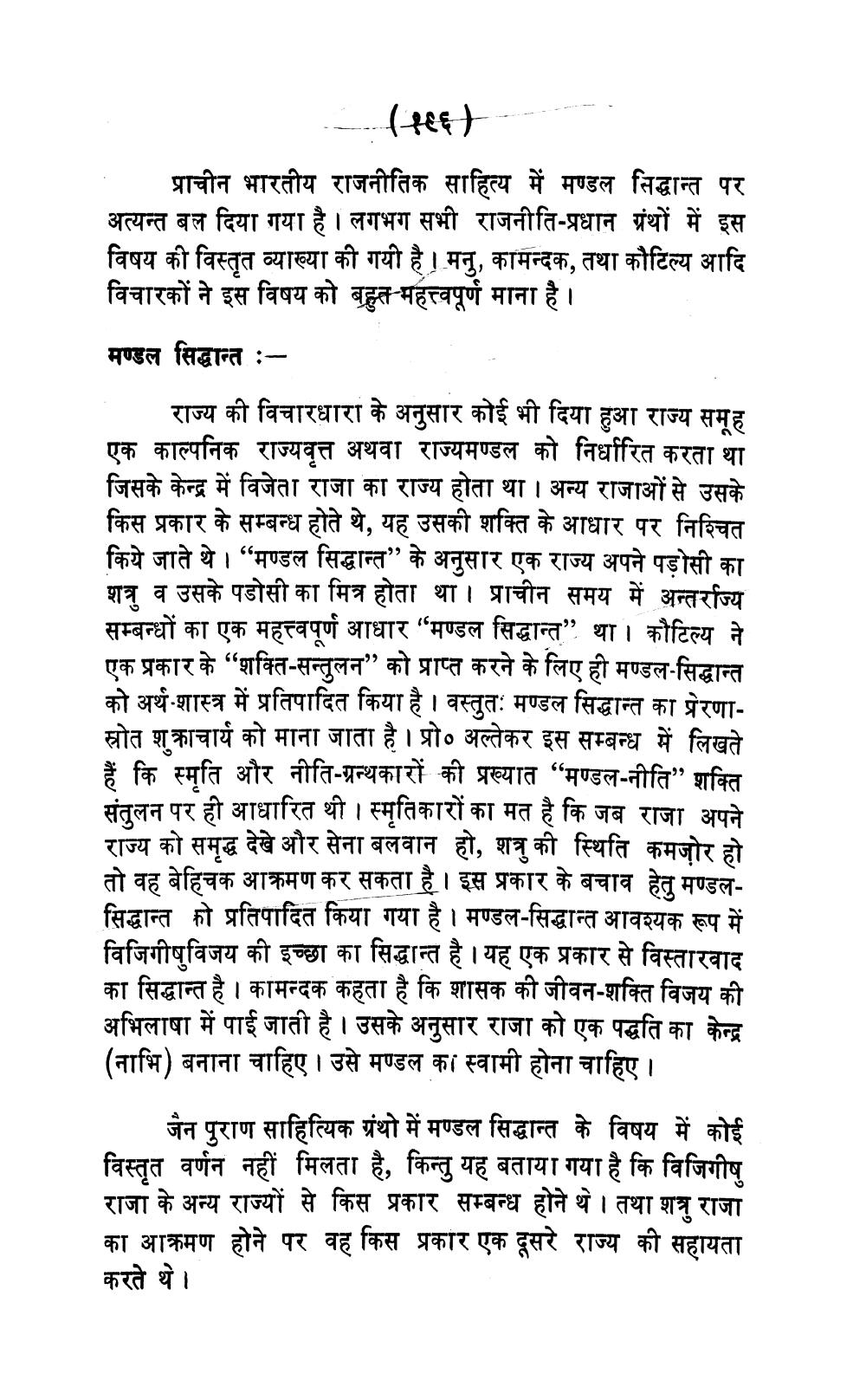________________
. (१९६) प्राचीन भारतीय राजनीतिक साहित्य में मण्डल सिद्धान्त पर अत्यन्त बल दिया गया है । लगभग सभी राजनीति-प्रधान ग्रंथों में इस विषय की विस्तृत व्याख्या की गयी है । मनु, कामन्दक, तथा कौटिल्य आदि विचारकों ने इस विषय को बहुत महत्त्वपूर्ण माना है । मण्डल सिद्धान्त :
राज्य की विचारधारा के अनुसार कोई भी दिया हुआ राज्य समूह एक काल्पनिक राज्यवृत्त अथवा राज्यमण्डल को निर्धारित करता था जिसके केन्द्र में विजेता राजा का राज्य होता था। अन्य राजाओं से उसके किस प्रकार के सम्बन्ध होते थे, यह उसकी शक्ति के आधार पर निश्चित किये जाते थे। "मण्डल सिद्धान्त" के अनुसार एक राज्य अपने पडोसी का शत्र व उसके पडोसी का मित्र होता था। प्राचीन समय में अन्तर्राज्य सम्बन्धों का एक महत्त्वपूर्ण आधार “मण्डल सिद्धान्त" था। कौटिल्य ने एक प्रकार के "शक्ति-सन्तुलन” को प्राप्त करने के लिए ही मण्डल-सिद्धान्त को अर्थ-शास्त्र में प्रतिपादित किया है । वस्तुतः मण्डल सिद्धान्त का प्रेरणास्रोत शुक्राचार्य को माना जाता है। प्रो० अल्तेकर इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि स्मति और नीति-ग्रन्थकारों की प्रख्यात "मण्डल-नीति" शक्ति संतुलन पर ही आधारित थी। स्मतिकारों का मत है कि जब राजा अपने राज्य को समृद्ध देखे और सेना बलवान हो, शत्रु की स्थिति कमजोर हो तो वह बेहिचक आक्रमण कर सकता है । इस प्रकार के बचाव हेतु मण्डलसिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है । मण्डल-सिद्धान्त आवश्यक रूप में विजिगीषुविजय की इच्छा का सिद्धान्त है । यह एक प्रकार से विस्तारवाद का सिद्धान्त है । कामन्दक कहता है कि शासक की जीवन-शक्ति विजय की अभिलाषा में पाई जाती है । उसके अनुसार राजा को एक पद्धति का केन्द्र (नाभि) बनाना चाहिए। उसे मण्डल का स्वामी होना चाहिए।
जैन पुराण साहित्यिक ग्रंथो में मण्डल सिद्धान्त के विषय में कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, किन्तु यह बताया गया है कि विजिगीषु राजा के अन्य राज्यों से किस प्रकार सम्बन्ध होने थे। तथा शत्रु राजा का आक्रमण होने पर वह किस प्रकार एक दूसरे राज्य की सहायता करते थे।