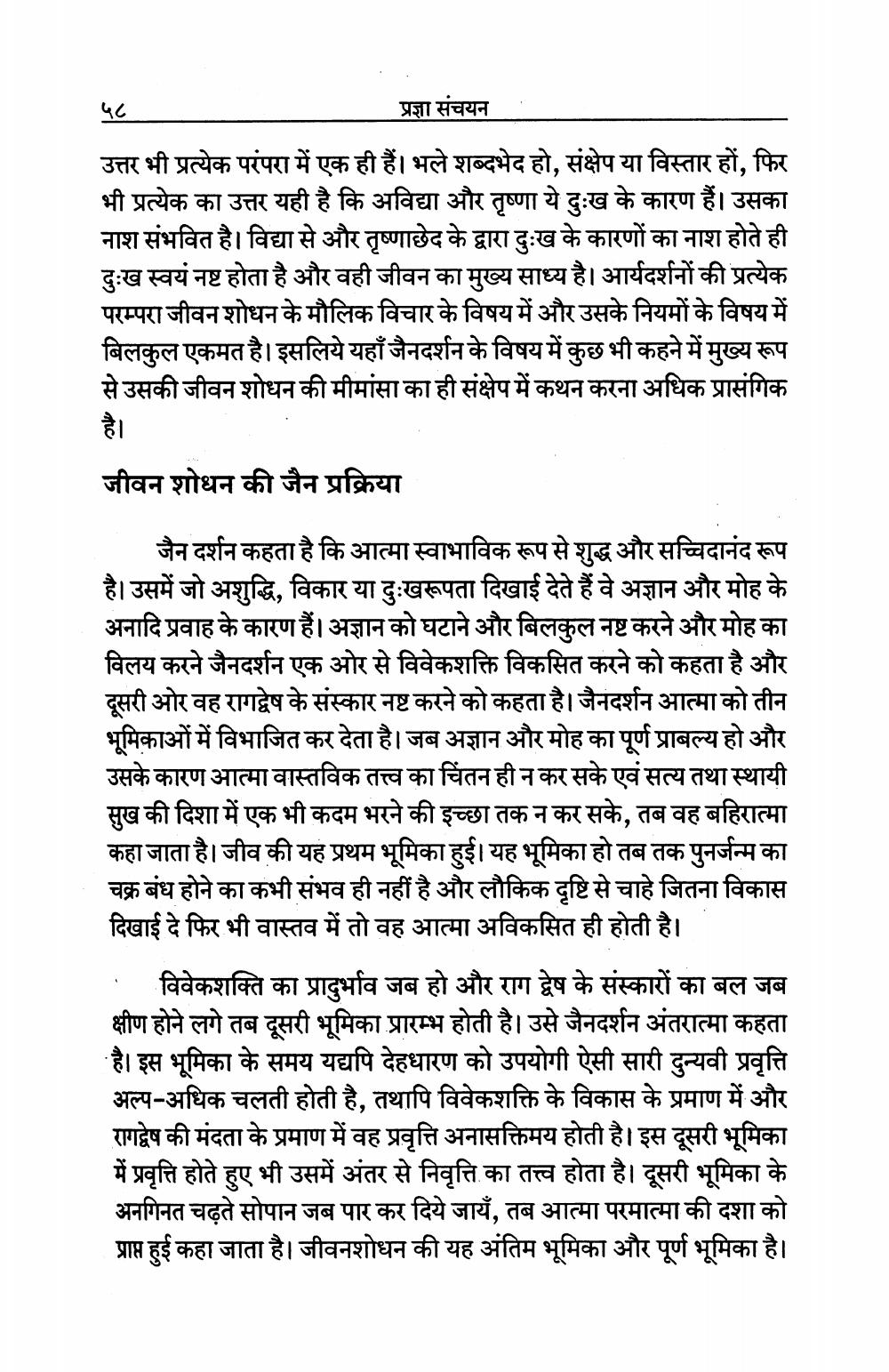________________
प्रज्ञा संचयन उत्तर भी प्रत्येक परंपरा में एक ही हैं। भले शब्दभेद हो, संक्षेप या विस्तार हों, फिर भी प्रत्येक का उत्तर यही है कि अविद्या और तृष्णा ये दुःख के कारण हैं। उसका नाश संभवित है। विद्या से और तृष्णाछेद के द्वारा दुःख के कारणों का नाश होते ही दुःख स्वयं नष्ट होता है और वही जीवन का मुख्य साध्य है। आर्यदर्शनों की प्रत्येक परम्परा जीवन शोधन के मौलिक विचार के विषय में और उसके नियमों के विषय में बिलकुल एकमत है। इसलिये यहाँ जैनदर्शन के विषय में कुछ भी कहने में मुख्य रूप से उसकी जीवन शोधन की मीमांसा का ही संक्षेप में कथन करना अधिक प्रासंगिक
जीवन शोधन की जैन प्रक्रिया
जैन दर्शन कहता है कि आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध और सच्चिदानंद रूप है। उसमें जो अशुद्धि, विकार या दुःखरूपता दिखाई देते हैं वे अज्ञान और मोह के अनादि प्रवाह के कारण हैं। अज्ञान को घटाने और बिलकुल नष्ट करने और मोह का विलय करने जैनदर्शन एक ओर से विवेकशक्ति विकसित करने को कहता है और दूसरी ओर वह रागद्वेष के संस्कार नष्ट करने को कहता है। जैनदर्शन आत्मा को तीन भूमिकाओं में विभाजित कर देता है। जब अज्ञान और मोह का पूर्ण प्राबल्य हो और उसके कारण आत्मा वास्तविक तत्त्व का चिंतन ही न कर सके एवं सत्य तथा स्थायी सुख की दिशा में एक भी कदम भरने की इच्छा तक न कर सके, तब वह बहिरात्मा कहा जाता है। जीव की यह प्रथम भूमिका हुई। यह भूमिका हो तब तक पुनर्जन्म का चक्र बंध होने का कभी संभव ही नहीं है और लौकिक दृष्टि से चाहे जितना विकास दिखाई दे फिर भी वास्तव में तो वह आत्मा अविकसित ही होती है। - विवेकशक्ति का प्रादुर्भाव जब हो और राग द्वेष के संस्कारों का बल जब क्षीण होने लगे तब दूसरी भूमिका प्रारम्भ होती है। उसे जैनदर्शन अंतरात्मा कहता है। इस भूमिका के समय यद्यपि देहधारण को उपयोगी ऐसी सारी दुन्यवी प्रवृत्ति अल्प-अधिक चलती होती है, तथापि विवेकशक्ति के विकास के प्रमाण में और रागद्वेष की मंदता के प्रमाण में वह प्रवृत्ति अनासक्तिमय होती है। इस दूसरी भूमिका में प्रवृत्ति होते हुए भी उसमें अंतर से निवृत्ति का तत्त्व होता है। दूसरी भूमिका के अनगिनत चढ़ते सोपान जब पार कर दिये जायँ, तब आत्मा परमात्मा की दशा को प्राप्त हुई कहा जाता है। जीवनशोधन की यह अंतिम भूमिका और पूर्ण भूमिका है।