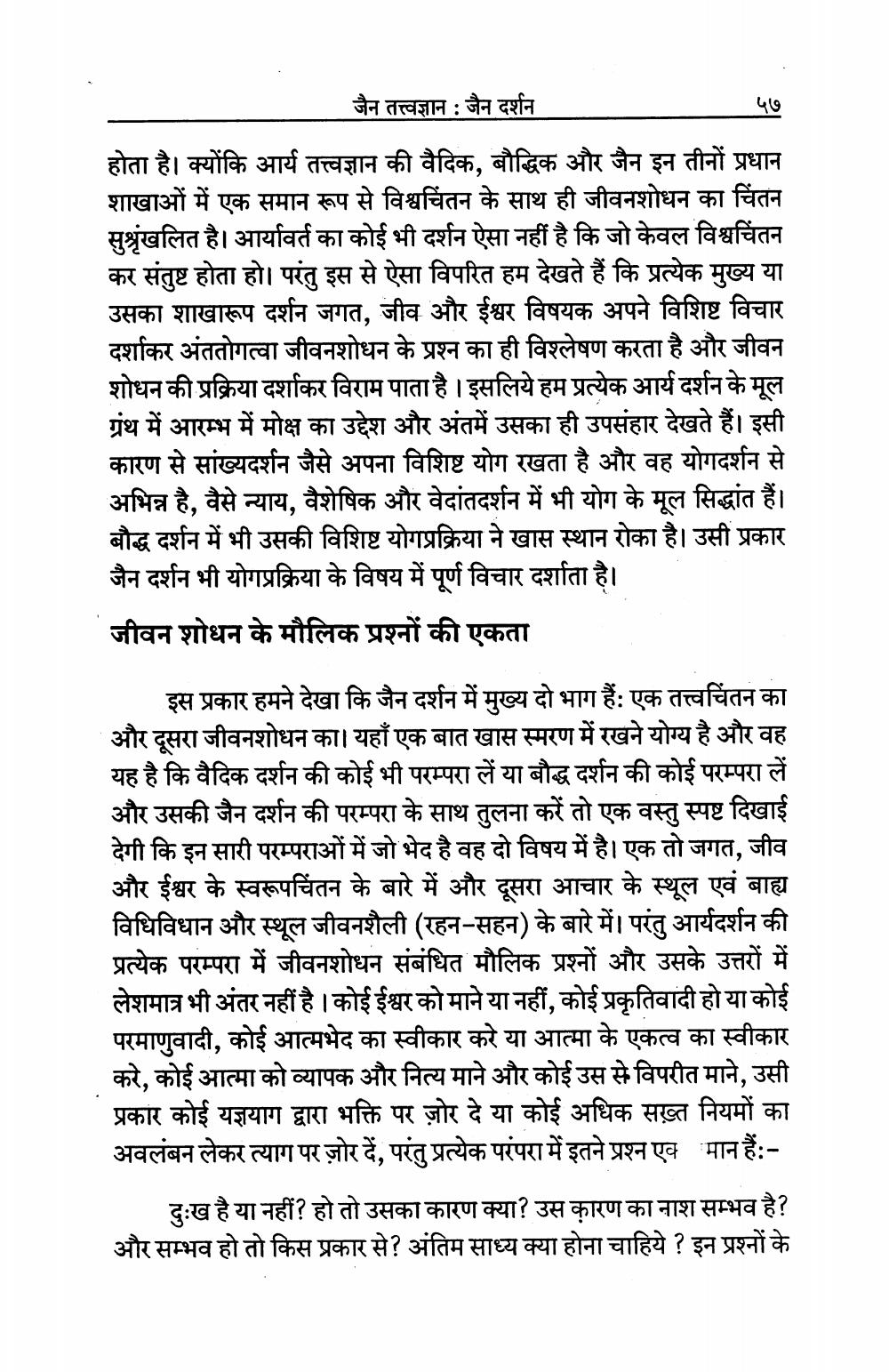________________
जैन तत्त्वज्ञान : जैन दर्शन
होता है। क्योंकि आर्य तत्त्वज्ञान की वैदिक, बौद्धिक और जैन इन तीनों प्रधान शाखाओं में एक समान रूप से विश्वचिंतन के साथ ही जीवनशोधन का चिंतन सुश्रृंखलित है। आर्यावर्त का कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है कि जो केवल विश्वचिंतन कर संतुष्ट होता हो। परंतु इस से ऐसा विपरित हम देखते हैं कि प्रत्येक मुख्य या उसका शाखारूप दर्शन जगत, जीव और ईश्वर विषयक अपने विशिष्ट विचार दर्शाकर अंततोगत्वा जीवनशोधन के प्रश्न का ही विश्लेषण करता है और जीवन शोधन की प्रक्रिया दर्शाकर विराम पाता है । इसलिये हम प्रत्येक आर्य दर्शन के मूल ग्रंथ में आरम्भ में मोक्ष का उद्देश और अंतमें उसका ही उपसंहार देखते हैं। इसी कारण से सांख्यदर्शन जैसे अपना विशिष्ट योग रखता है और वह योगदर्शन से अभिन्न है, वैसे न्याय, वैशेषिक और वेदांतदर्शन में भी योग के मूल सिद्धांत हैं। बौद्ध दर्शन में भी उसकी विशिष्ट योगप्रक्रिया ने खास स्थान रोका है। उसी प्रकार जैन दर्शन भी योगप्रक्रिया के विषय में पूर्ण विचार दर्शाता है। जीवन शोधन के मौलिक प्रश्नों की एकता
इस प्रकार हमने देखा कि जैन दर्शन में मख्य दो भाग हैं: एक तत्त्वचिंतन का और दूसरा जीवनशोधन का। यहाँ एक बात खास स्मरण में रखने योग्य है और वह यह है कि वैदिक दर्शन की कोई भी परम्परा लें या बौद्ध दर्शन की कोई परम्परा लें
और उसकी जैन दर्शन की परम्परा के साथ तुलना करें तो एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी कि इन सारी परम्पराओं में जो भेद है वह दो विषय में है। एक तो जगत, जीव
और ईश्वर के स्वरूपचिंतन के बारे में और दूसरा आचार के स्थूल एवं बाह्य विधिविधान और स्थूल जीवनशैली (रहन-सहन) के बारे में। परंतु आर्यदर्शन की प्रत्येक परम्परा में जीवनशोधन संबंधित मौलिक प्रश्नों और उसके उत्तरों में लेशमात्र भी अंतर नहीं है । कोई ईश्वर को माने या नहीं, कोई प्रकृतिवादी हो या कोई परमाणुवादी, कोई आत्मभेद का स्वीकार करे या आत्मा के एकत्व का स्वीकार करे, कोई आत्मा को व्यापक और नित्य माने और कोई उस से विपरीत माने, उसी प्रकार कोई यज्ञयाग द्वारा भक्ति पर ज़ोर दे या कोई अधिक सख़्त नियमों का अवलंबन लेकर त्याग पर ज़ोर दें, परंतु प्रत्येक परंपरा में इतने प्रश्न एव मान हैं:
दुःख है या नहीं? हो तो उसका कारण क्या? उस कारण का नाश सम्भव है? और सम्भव हो तो किस प्रकार से? अंतिम साध्य क्या होना चाहिये ? इन प्रश्नों के