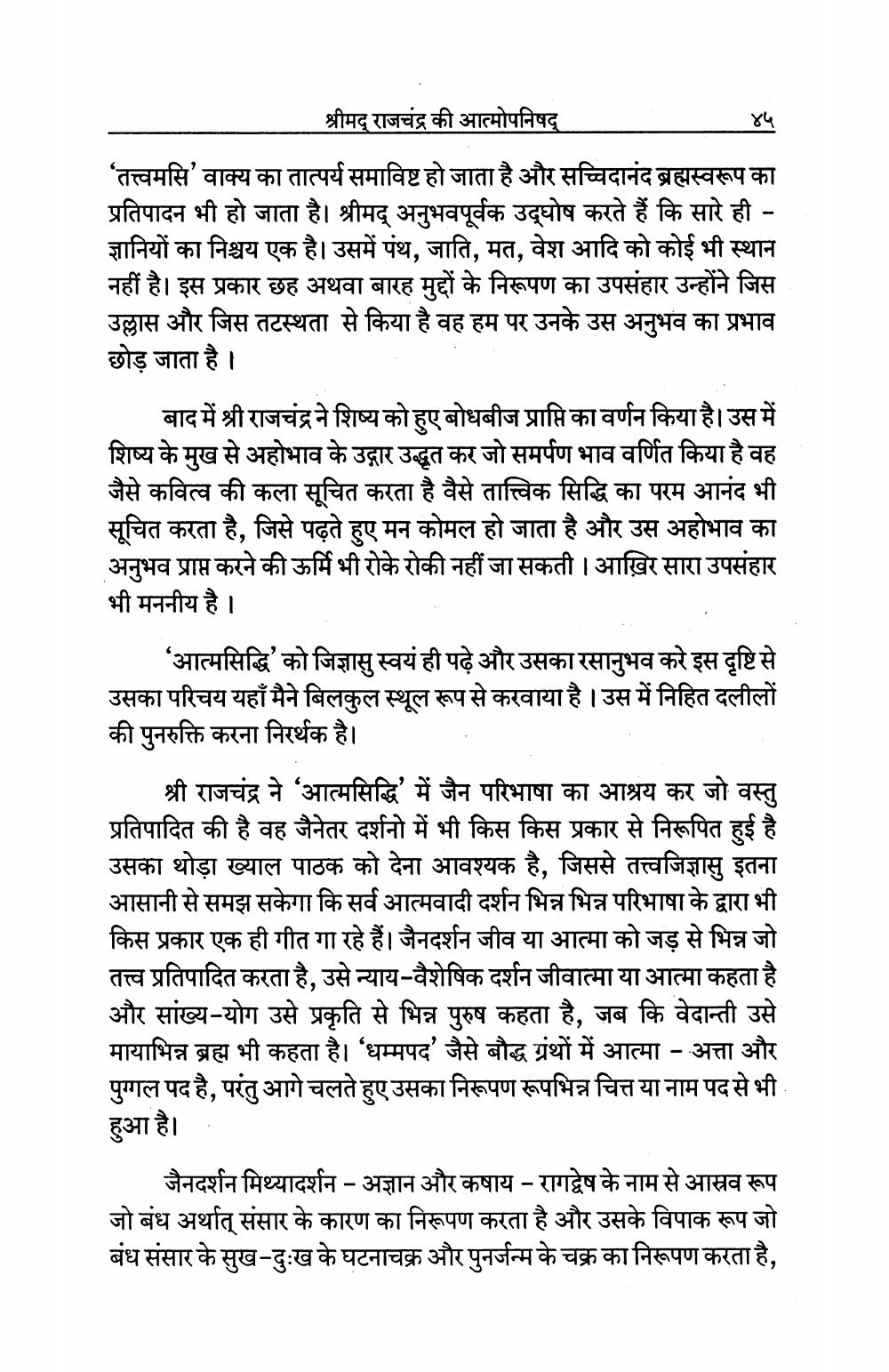________________
श्रीमद् राजचंद्र की आत्मोपनिषद्
'तत्त्वमसि' वाक्य का तात्पर्य समाविष्ट हो जाता है और सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन भी हो जाता है। श्रीमद् अनुभवपूर्वक उद्घोष करते हैं कि सारे ही - ज्ञानियों का निश्चय एक है। उसमें पंथ, जाति, मत, वेश आदि को कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार छह अथवा बारह मुद्दों के निरूपण का उपसंहार उन्होंने जिस उल्लास और जिस तटस्थता से किया है वह हम पर उनके उस अनुभव का प्रभाव छोड़ जाता है।
बाद में श्री राजचंद्र ने शिष्य को हुए बोधबीज प्राप्ति का वर्णन किया है। उस में शिष्य के मुख से अहोभाव के उद्गार उद्धृत कर जो समर्पण भाव वर्णित किया है वह जैसे कवित्व की कला सूचित करता है वैसे तात्त्विक सिद्धि का परम आनंद भी सूचित करता है, जिसे पढ़ते हुए मन कोमल हो जाता है और उस अहोभाव का अनुभव प्राप्त करने की ऊर्मि भी रोके रोकी नहीं जा सकती। आख़िर सारा उपसंहार भी मननीय है।
‘आत्मसिद्धि' को जिज्ञासु स्वयं ही पढ़े और उसका रसानुभव करे इस दृष्टि से उसका परिचय यहाँ मैने बिलकुल स्थूल रूप से करवाया है। उस में निहित दलीलों की पुनरुक्ति करना निरर्थक है।
श्री राजचंद्र ने 'आत्मसिद्धि' में जैन परिभाषा का आश्रय कर जो वस्तु प्रतिपादित की है वह जैनेतर दर्शनो में भी किस किस प्रकार से निरूपित हुई है उसका थोड़ा ख्याल पाठक को देना आवश्यक है, जिससे तत्त्वजिज्ञासु इतना आसानी से समझ सकेगा कि सर्व आत्मवादी दर्शन भिन्न भिन्न परिभाषा के द्वारा भी किस प्रकार एक ही गीत गा रहे हैं। जैनदर्शन जीव या आत्मा को जड़ से भिन्न जो तत्त्व प्रतिपादित करता है, उसे न्याय-वैशेषिक दर्शन जीवात्मा या आत्मा कहता है
और सांख्य-योग उसे प्रकृति से भिन्न पुरुष कहता है, जब कि वेदान्ती उसे मायाभिन्न ब्रह्म भी कहता है। 'धम्मपद' जैसे बौद्ध ग्रंथों में आत्मा - अत्ता और पुग्गल पद है, परंतु आगे चलते हुए उसका निरूपण रूपभिन्न चित्त या नाम पद से भी हुआ है।
जैनदर्शन मिथ्यादर्शन - अज्ञान और कषाय - रागद्वेष के नाम से आस्रव रूप जो बंध अर्थात् संसार के कारण का निरूपण करता है और उसके विपाक रूप जो बंध संसार के सुख-दुःख के घटनाचक्र और पुनर्जन्म के चक्र का निरूपण करता है,