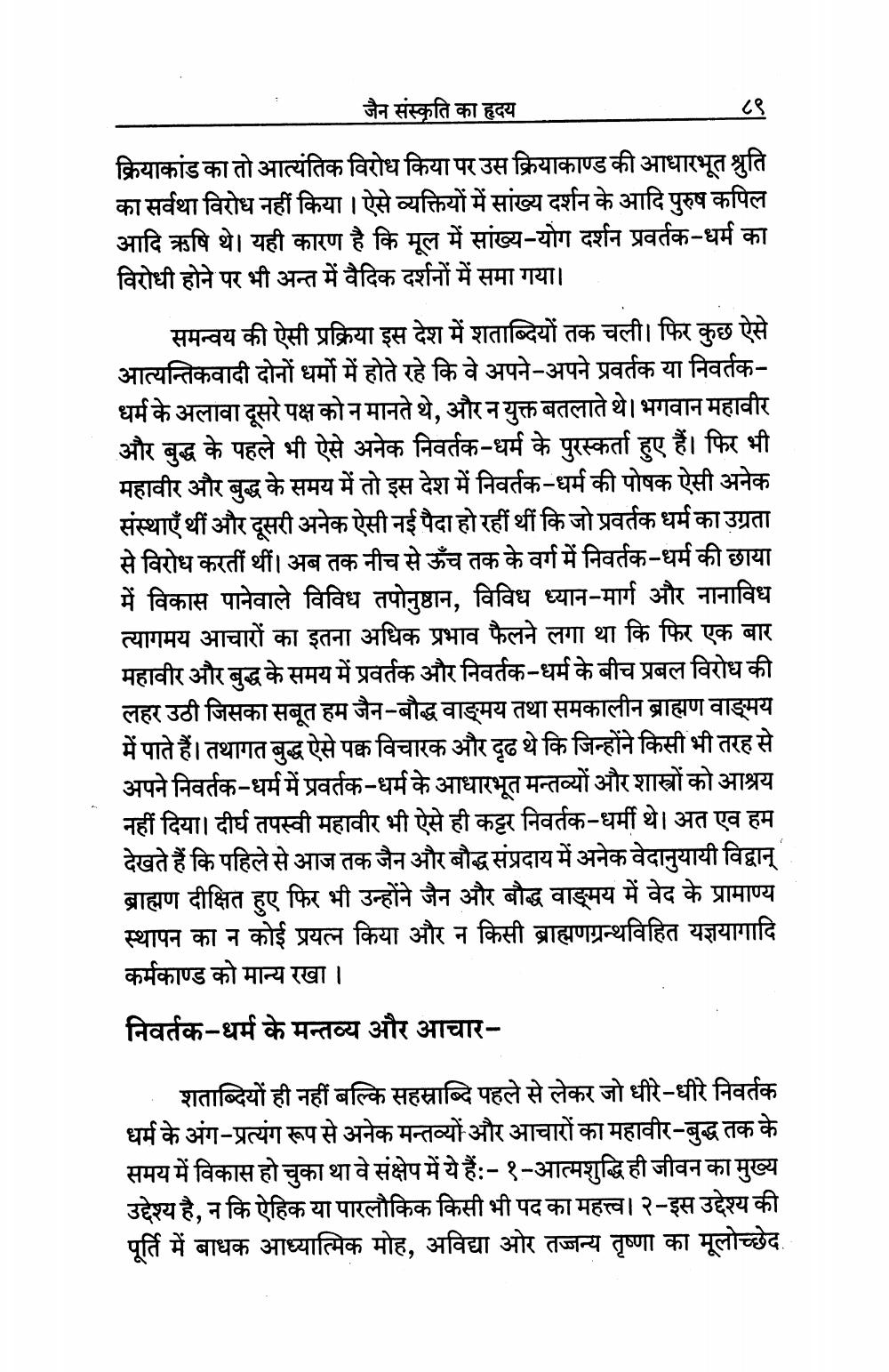________________
जैन संस्कृति का हृदय क्रियाकांड का तो आत्यंतिक विरोध किया पर उस क्रियाकाण्ड की आधारभूत श्रुति का सर्वथा विरोध नहीं किया । ऐसे व्यक्तियों में सांख्य दर्शन के आदि पुरुष कपिल आदि ऋषि थे। यही कारण है कि मूल में सांख्य-योग दर्शन प्रवर्तक-धर्म का विरोधी होने पर भी अन्त में वैदिक दर्शनों में समा गया।
समन्वय की ऐसी प्रक्रिया इस देश में शताब्दियों तक चली। फिर कुछ ऐसे आत्यन्तिकवादी दोनों धर्मो में होते रहे कि वे अपने-अपने प्रवर्तक या निवर्तकधर्म के अलावा दूसरे पक्ष को न मानते थे, और न युक्त बतलाते थे। भगवान महावीर
और बुद्ध के पहले भी ऐसे अनेक निवर्तक-धर्म के पुरस्कर्ता हुए हैं। फिर भी महावीर और बुद्ध के समय में तो इस देश में निवर्तक-धर्म की पोषक ऐसी अनेक संस्थाएँ थीं और दूसरी अनेक ऐसी नई पैदा हो रहीं थीं कि जो प्रवर्तक धर्म का उग्रता से विरोध करतीं थीं। अब तक नीच से ऊँच तक के वर्ग में निवर्तक-धर्म की छाया में विकास पानेवाले विविध तपोनुष्ठान, विविध ध्यान-मार्ग और नानाविध त्यागमय आचारों का इतना अधिक प्रभाव फैलने लगा था कि फिर एक बार महावीर और बुद्ध के समय में प्रवर्तक और निवर्तक-धर्म के बीच प्रबल विरोध की लहर उठी जिसका सबूत हम जैन-बौद्ध वाङ्मय तथा समकालीन ब्राह्मण वाङ्मय में पाते हैं। तथागत बुद्ध ऐसे पक्क विचारक और दृढ थे कि जिन्होंने किसी भी तरह से अपने निवर्तक-धर्म में प्रवर्तक-धर्म के आधारभूत मन्तव्यों और शास्त्रों को आश्रय नहीं दिया। दीर्घ तपस्वी महावीर भी ऐसे ही कट्टर निवर्तक-धर्मी थे। अत एव हम देखते हैं कि पहिले से आज तक जैन और बौद्ध संप्रदाय में अनेक वेदानुयायी विद्वान् ब्राह्मण दीक्षित हुए फिर भी उन्होंने जैन और बौद्ध वाङ्मय में वेद के प्रामाण्य स्थापन का न कोई प्रयत्न किया और न किसी ब्राह्मणग्रन्थविहित यज्ञयागादि कर्मकाण्ड को मान्य रखा। निवर्तक-धर्म के मन्तव्य और आचार
- शताब्दियों ही नहीं बल्कि सहस्राब्दि पहले से लेकर जो धीरे-धीरे निवर्तक धर्म के अंग-प्रत्यंग रूप से अनेक मन्तव्यों और आचारों का महावीर-बुद्ध तक के समय में विकास हो चुका था वे संक्षेप में ये हैं:-१-आत्मशुद्धि ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, न कि ऐहिक या पारलौकिक किसी भी पद का महत्त्व। २-इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आध्यात्मिक मोह, अविद्या ओर तजन्य तृष्णा का मूलोच्छेद