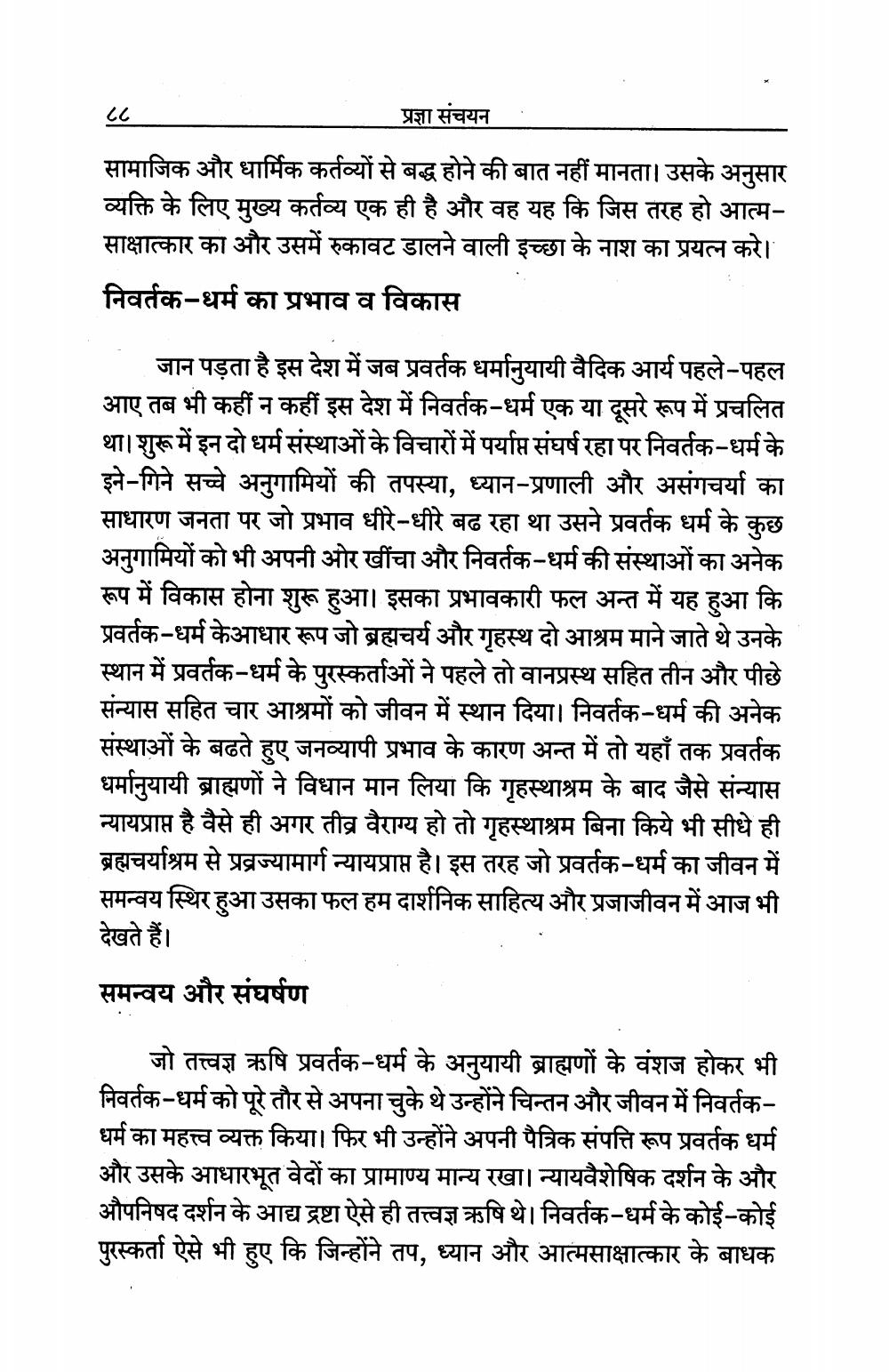________________
८८ -
प्रज्ञा संचयन
सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से बद्ध होने की बात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए मुख्य कर्तव्य एक ही है और वह यह कि जिस तरह हो आत्मसाक्षात्कार का और उसमें रुकावट डालने वाली इच्छा के नाश का प्रयत्न करे। निवर्तक-धर्म का प्रभाव व विकास
___जान पड़ता है इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी वैदिक आर्य पहले-पहल आए तब भी कहीं न कहीं इस देश में निवर्तक-धर्म एक या दूसरे रूप में प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म संस्थाओं के विचारों में पर्याप्त संघर्ष रहा पर निवर्तक-धर्म के इने-गिने सच्चे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रणाली और असंगचर्या का साधारण जनता पर जो प्रभाव धीरे-धीरे बढ रहा था उसने प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को भी अपनी ओर खींचा और निवर्तक-धर्म की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ। इसका प्रभावकारी फल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक-धर्म केआधार रूप जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो आश्रम माने जाते थे उनके स्थान में प्रवर्तक-धर्म के पुरस्कर्ताओं ने पहले तो वानप्रस्थ सहित तीन और पीछे संन्यास सहित चार आश्रमों को जीवन में स्थान दिया। निवर्तक-धर्म की अनेक संस्थाओं के बढ़ते हुए जनव्यापी प्रभाव के कारण अन्त में तो यहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने विधान मान लिया कि गृहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्यायप्राप्त है वैसे ही अगर तीव्र वैराग्य हो तो गृहस्थाश्रम बिना किये भी सीधे ही ब्रह्मचर्याश्रम से प्रव्रज्यामार्ग न्यायप्राप्त है। इस तरह जो प्रवर्तक-धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ उसका फल हम दार्शनिक साहित्य और प्रजाजीवन में आज भी देखते हैं। समन्वय और संघर्षण
जो तत्त्वज्ञ ऋषि प्रवर्तक-धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों के वंशज होकर भी निवर्तक-धर्म को पूरे तौर से अपना चुके थे उन्होंने चिन्तन और जीवन में निवर्तकधर्म का महत्त्व व्यक्त किया। फिर भी उन्होंने अपनी पैत्रिक संपत्ति रूप प्रवर्तक धर्म और उसके आधारभूत वेदों का प्रामाण्य मान्य रखा। न्यायवैशेषिक दर्शन के और औपनिषद दर्शन के आद्य द्रष्टा ऐसे ही तत्त्वज्ञ ऋषि थे। निवर्तक-धर्म के कोई-कोई पुरस्कर्ता ऐसे भी हुए कि जिन्होंने तप, ध्यान और आत्मसाक्षात्कार के बाधक